रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए ॥ रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएँ लिखिए ॥ Raghuvir Sahay Ki Kavyagat Visheshta Likhiye ॥ रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए
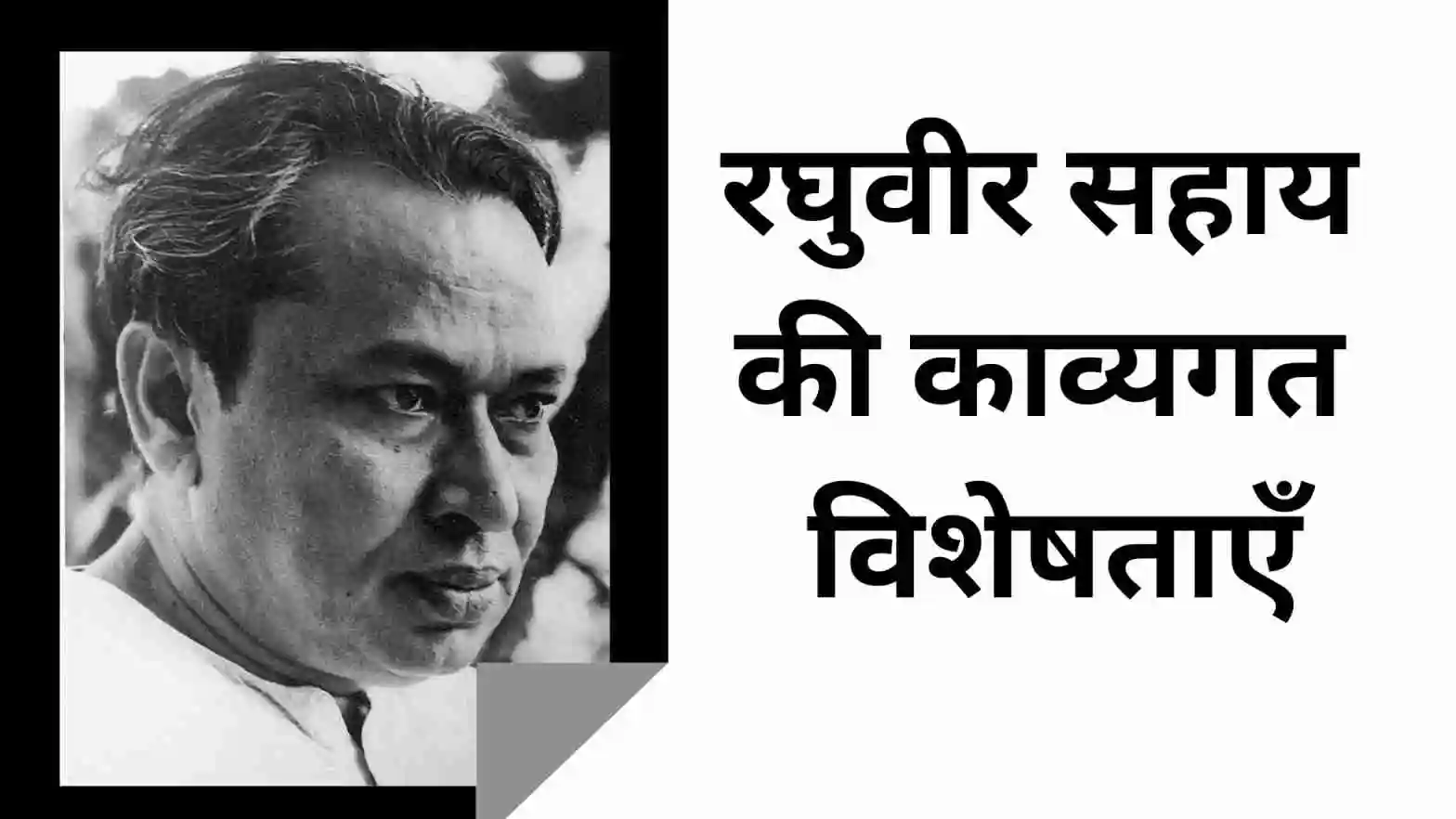
उत्तर —
लगभग 45 वर्षों तक कविता लिखने वाले रघुवीर सहाय एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उनकी कविताओं की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं:
(1) आम लोगों को महत्व देना
रघुवीर सहाय की कविताओं में आम आदमी सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी कविता का असली हीरो कोई राजा, नेता या ताकतवर इंसान नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान होता है। उन्होंने आम आदमी की समस्याओं, डर, संघर्ष और समाज में उसकी स्थिति को बहुत ही सच्चे और गहरे ढंग से दिखाया है।
जैसे प्रसिद्ध आलोचक नन्दकिशोर नवल कहते हैं —
“रघुवीर सहाय की वे कविताएँ जो राजनीतिक विषयों पर हैं, उनमें भी आम आदमी ही मुख्य रूप से मौजूद है। कवि ने हर राजनीतिक घटना को आम आदमी की नजर से देखा है।”
उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ इस बात को और अच्छे से समझाती हैं —
हँसो तुम पर निगाह रखी जा रही है
हँसो अपने पर न हँसना
क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी
और तुम मारे जाओगे।ऐसा हँसो कि बहुत खुश न मालूम हो
वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं
और मारे जाओगे।
इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि आज का आम इंसान डर के साए में जी रहा है। उसे यहाँ तक सोचना पड़ता है कि कैसे हँसे, कितना हँसे — क्योंकि कहीं उसकी हँसी को भी खतरे के रूप में न देखा जाए। यह बताता है कि समाज में डर और असुरक्षा का माहौल कितना गहरा हो गया है।
इस प्रकार रघुवीर सहाय की कविताएँ आम लोगों की आवाज़ बनती हैं और उनके जीवन की सच्चाई को सामने लाती हैं।
(2) यथार्थ का चित्रण —
रघुवीर सहाय की कविताओं की एक खास बात यह है कि वे हमारे आसपास की सच्ची घटनाओं और हालात को साफ-साफ दिखाती हैं। उन्होंने समाज में जो कुछ हो रहा था, उसी को अपनी कविता का विषय बनाया। इसलिए उनकी कविताएँ बहुत ही सजीव और सच्ची लगती हैं।
कभी-कभी आलोचक (समालोचक) यह कहते हैं कि उनकी कविताएँ बहुत साधारण या सतही लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कवि ने जानबूझकर एक डरे हुए और असुरक्षित समाज की तस्वीर दिखाई है। जब हम उस डर और सच्चाई को कविता में पढ़ते हैं, तो वह साधारण नहीं बल्कि दिल को छू जाने वाली लगती है।
उनकी एक कविता की पंक्तियाँ इस बात को साफ़ करती हैं —
“एक दिन इसी तरह आएगा – रमेश
कि किसी की कोई राय न रह जाएगी – रमेश
क्रोध होगा पर विरोध न होगा
अर्जियों के सिवाय – रमेश
खतरा होगा, खतरे की घंटी बजेगी
पर उसे बादशाह बजाएगा – रमेश”
इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि भविष्य में एक ऐसा समय भी आ सकता है, जब लोग गुस्सा तो करेंगे, लेकिन डर के कारण आवाज़ नहीं उठाएँगे। विरोध सिर्फ चुपचाप अर्जी (दरख़ास्त) देकर ही होगा। और जो खतरे की घंटी बजेगी, वह भी सरकार या ताकतवर लोग ही बजायेंगे — यानी खतरे को भी वही लोग तय करेंगे।
इस तरह रघुवीर सहाय की कविता सच्चाई को बिना डर के दिखाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है।
(3) व्यंग्यात्मकता —
रघुवीर सहाय की कविताओं की एक और बड़ी खासियत यह है कि उनमें तीखा और चुभता हुआ व्यंग्य होता है। वे अपनी कविताओं के माध्यम से समाज, राजनीति और नेताओं की कमजोरियों पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन यह कटाक्ष बहुत ही बुद्धिमानी और सूझबूझ के साथ किया जाता है।
उनकी कविता ‘राष्ट्रीय प्रतिज्ञा’ में ऐसा व्यंग्य साफ दिखाई देता है। इसमें कवि नेताओं की बातों और वादों पर तीखा व्यंग्य करता है। कविता की पंक्तियाँ देखें —
“हमने बहुत किया है
जनता ने नहीं किया है
हमने बहुत किया है
हम फिर से बहुत करेंगे
हमने बहुत किया है
पर अब हम नहीं कहेंगे
कि हम अब क्या और करेंगे
और हमसे लोग अगर कहेंगे
कुछ करने को
तो वह तो कभी नहीं करेंगे।”
इन पंक्तियों में कवि यह दिखाते हैं कि कुछ नेता खुद को महान बताकर बार-बार कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, जबकि असल में वे जनता की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अब वे यह नहीं बताएँगे कि आगे क्या करेंगे, और अगर जनता कुछ कहेगी भी, तो वे उसकी बात नहीं मानेंगे।
आलोचक नंदकिशोर नवल कहते हैं कि रघुवीर सहाय का व्यंग्य एक “बहुउपयोगी चाकू” की तरह है, जिसमें कई धारें होती हैं। कविता की हर दो-तीन पंक्तियों में एक नया व्यंग्य छिपा होता है, और आखिरी में यह व्यंग्य अपने सबसे तेज़ रूप में सामने आता है।
इस तरह रघुवीर सहाय की कविता केवल पढ़ने के लिए नहीं, समझने और सोचने के लिए भी होती है। उनका व्यंग्य हमारे समाज की सच्चाई को बहुत प्रभावशाली ढंग से सामने लाता है।
(4) श्रृंगार की संयमित अभिव्यक्ति —
रघुवीर सहाय ने अपनी कविताओं में प्रेम और भावना (श्रृंगार) को बहुत शांत, गहरे और मर्यादित ढंग से प्रस्तुत किया है। जहाँ उस समय के कई कवि प्रेम को बहुत खुलकर या अत्यधिक रूप से (अशोभनीय तरीके से) दिखाते थे, वहीं रघुवीर सहाय ने इसे बहुत संयमित और भावुक तरीके से दिखाया।
उन्होंने प्रेम की पीड़ा, यादें और विरह (जुदाई) को भी बहुत शालीन और शांत स्वर में प्रस्तुत किया। इसका एक सुंदर उदाहरण उनकी निम्नलिखित कविता की पंक्तियों में देखने को मिलता है —
“मैं कभी-कभी कमरे के कोने में जाकर
एकान्त जहाँ पर होता है,
चुपके से एक पुराना कागज पढ़ता हूँ
मेरे जीवन का विवरण उसमें लिखा हुआ
यह एक पुराना प्रेम पत्र है
जो लिखकर भेजा ही नहीं गया,
जिसको पाने वाला, काफी दिन बीते गुजर चुका।”
इन पंक्तियों में कवि यह बता रहे हैं कि कैसे वे अकेले में चुपचाप बैठकर एक पुराना प्रेम पत्र पढ़ते हैं, जिसे उन्होंने कभी भेजा ही नहीं। उस पत्र में उनका बीता हुआ प्रेम और जीवन की यादें छिपी हैं। जिसे यह पत्र भेजना था, वह अब इस दुनिया में नहीं है।
इस तरह रघुवीर सहाय ने प्रेम की भावना को बिना दिखावे के, बहुत गहराई और सादगी से व्यक्त किया है।
(5) प्रयोगवादी शैली —
रघुवीर सहाय की कविता-शैली को प्रयोगवादी कहा जाता है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी कविताओं में नई-नई तकनीकों और शैलियों का प्रयोग किया, ताकि कविता में कुछ अलग और असरदार किया जा सके।
शुरुआत में रघुवीर सहाय ने छंदों (कविता की लय और तुक) में कविताएँ लिखीं, लेकिन बाद में उन्होंने गद्य (सीधी-सादी भाषा) जैसी शैली अपनाई। उनकी कई कविताएँ पढ़ने में ऐसे लगती हैं जैसे कोई आम इंसान अपनी बात कह रहा हो, लेकिन उनमें गहरी बातें और भाव छिपे होते हैं।
उन्होंने भाषा, ध्वनि और शब्दों से भी नए प्रयोग किए हैं। जैसे उनकी एक कविता की पंक्तियाँ देखें —
“अगर कहीं मैं तोता होता
तोता होता तो क्या होता?
तोता होता।
होता तो फिर ?
होता ‘फिर’ क्या ?
होता क्या?
मैं तोता होता तो
तो वो तो ता ता ता ता
बोल पट्ठे सीताराम”
(कविता – सीढ़ियों पर धूप में)
इस कविता में उन्होंने जानबूझकर शब्दों को बार-बार दोहराया है — जैसे “तोता होता”, “होता क्या?” आदि। ऐसा करके उन्होंने एक खेल जैसी भाषा बनाई है, जो पढ़ने में रोचक लगती है और साथ ही कविता को एक नया रूप देती है।
इस तरह रघुवीर सहाय ने कविता को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बनाया, बल्कि रचना और भाषा के स्तर पर भी प्रयोग करके उसे और खास बनाया।
(6) पारदर्शी एवं नई भाषा का प्रयोग —
रघुवीर सहाय ने अपनी कविताओं में सीधी, स्पष्ट और नई तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कविता को क्लासरूम जैसी भारी-भरकम भाषा से अलग करके आम बोलचाल की भाषा के करीब लाने का काम किया।
डॉ. सुरेश शर्मा का कहना है कि —
“रघुवीर सहाय हिन्दी कविता में नई विषयवस्तु लाने वाले सबसे बड़े कवियों में से एक हैं। वे कविता में जिस विषय को चुनते हैं, उसकी भाषा भी उसी विषय से जुड़ी होती है।”
इसलिए कई लोगों को उनकी भाषा अखबार जैसी लगती है, लेकिन असल में वह भाषा स्पष्ट और सच्ची बात कहने वाली पारदर्शी भाषा होती है।
श्री नंदकिशोर नवल का कहना है कि —
“रघुवीर सहाय का भरोसा पुराने ढाँचों को तोड़ने में था। उन्होंने आम और स्वीकृत भाषा को तोड़कर नई भाषा बनाई।”
उन्होंने यह काम केवल शब्दों के प्रयोग से ही नहीं किया, बल्कि वाक्यों की रचना (वाक्य-विन्यास) को भी अलग ढंग से बनाया।
इसका मतलब यह है कि उन्होंने कविता की भाषा को न केवल नया रूप दिया, बल्कि उसे और भी जीवंत, सच्चा और समझने लायक बना दिया।
उनकी यह शैली छात्रों के लिए यह सिखाने में मदद करती है कि कविता केवल तुक और भावनाओं का खेल नहीं होती, बल्कि विषय के अनुसार सही भाषा का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है।
(7) नारी जाति के प्रति सहानुभूति —
रघुवीर सहाय की कविताओं में स्त्री (नारी) एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय रही है। वे स्त्रियों को केवल एक पात्र नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और शोषित वर्ग का प्रतीक मानते हैं।
उनकी नजर में नारी उस आम इंसान की तरह है, जो सहनशील, असहाय और दमन का शिकार है। उन्होंने अपनी कविताओं में नारी की दर्द भरी स्थिति, उसकी चुप्पी और समाज द्वारा उसके साथ किए जा रहे अन्याय को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाया है।
उनकी प्रसिद्ध कविता ‘बड़ी हो रही है लड़की’ में वे लिखते हैं —
“जब वह कुछ कहती है
उसकी आवाज में
एक कोई चीज।
मुझे एकाएक औरत की आवाज लगती है
जो
अपमान बड़े होने पर सहेगी।”
इन पंक्तियों में कवि यह महसूस करते हैं कि जब एक लड़की बोलती है, तो उसकी आवाज में पहले से ही भविष्य के अपमानों का डर सुनाई देता है — जैसे वह जानती है कि जैसे-जैसे वह बड़ी होगी, उसे समाज में अपमान सहना पड़ेगा।
इसी प्रकार, ‘नारी’ नामक कविता में वे लिखते हैं —
“नारी विचारी / पुरुष की मारी।
तन से सुधित है / मन से मुदित है।
लपदन्कर-झपककर / अन्त में चित है।”
इस कविता में कवि ने दिखाया है कि नारी समाज में पुरुषों द्वारा शोषित होती है। वह बाहर से तो मुस्कराती है, लेकिन अंदर से दर्द और अपमान सहती है। अंत में वह गिर पड़ती है, यानी टूट जाती है।
इस तरह रघुवीर सहाय की कविताएँ नारी के दर्द, संघर्ष और स्थिति के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करती हैं। वे चाहते हैं कि समाज नारी को केवल एक शरीर न समझे, बल्कि उसकी आत्मा और अस्तित्व को भी माने और सम्मान दे।
(8) अन्य काव्यगत विशेषताएँ —
ऊपर दी गई विशेषताओं के अलावा रघुवीर सहाय की कविताओं में कई और विशेषताएँ भी देखने को मिलती हैं। उनकी कविताओं में—
- प्रेम (रोमांस) की भावना,
- गहरी सोच (बौद्धिकता),
- अपने निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति (नैयैतिकता),
- और सामान्य इंसान की भावनाएँ (मानवीय संवेदना) भी बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं।
उन्होंने अपने समय के समाज की सच्चाई, उसमें फैली असमानता और विरोधाभास, तथा आम आदमी के जीवन के संघर्षों को बहुत ही सच्चे और प्रभावशाली ढंग से कविता में पेश किया है।
‘समकालीन काव्य-यात्रा’ नामक पुस्तक के लेखक का कहना है कि —
“1960 के दशक में जब लोगों का राजनीति से विश्वास उठने लगा था, उस मोहभंग (निराशा) को रघुवीर सहाय ने बहुत ही दर्दनाक और गहराई से अपनी कविताओं में दिखाया है।”
उन्होंने कविता के माध्यम से दिखाया कि एक आम नागरिक की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, वोट देने का अधिकार, और स्वतंत्र भारत में आम जनता की हालत कैसी हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे समाज में जो राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियाँ (बेमेल स्थिति), विडंबनाएँ (विरोधाभास) और निरर्थकता (बेमतलब की बातें) हैं, वे आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं।
उनकी कविताएँ पढ़कर हमें यह महसूस होता है कि कवि अपने समय का सच बोलता है, और साथ ही आम इंसान की पीड़ा और आवाज बनता है।
Also Read:
- रामदास कविता के संदेश को अपने शब्दों में लिखें ॥ Ramdas Kavita Ka Mukhya Sandesh Kya Hai
- रामदास कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। Ramdas Kavita Ka Uddeshya Kya Hai
- रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताएँ(ramdhari singh dinkar ki kavyagat visheshta)
- मीराबाई की काव्यगत विशेषताएँ
- कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं (krishna bhakti kavya ki visheshtaen)