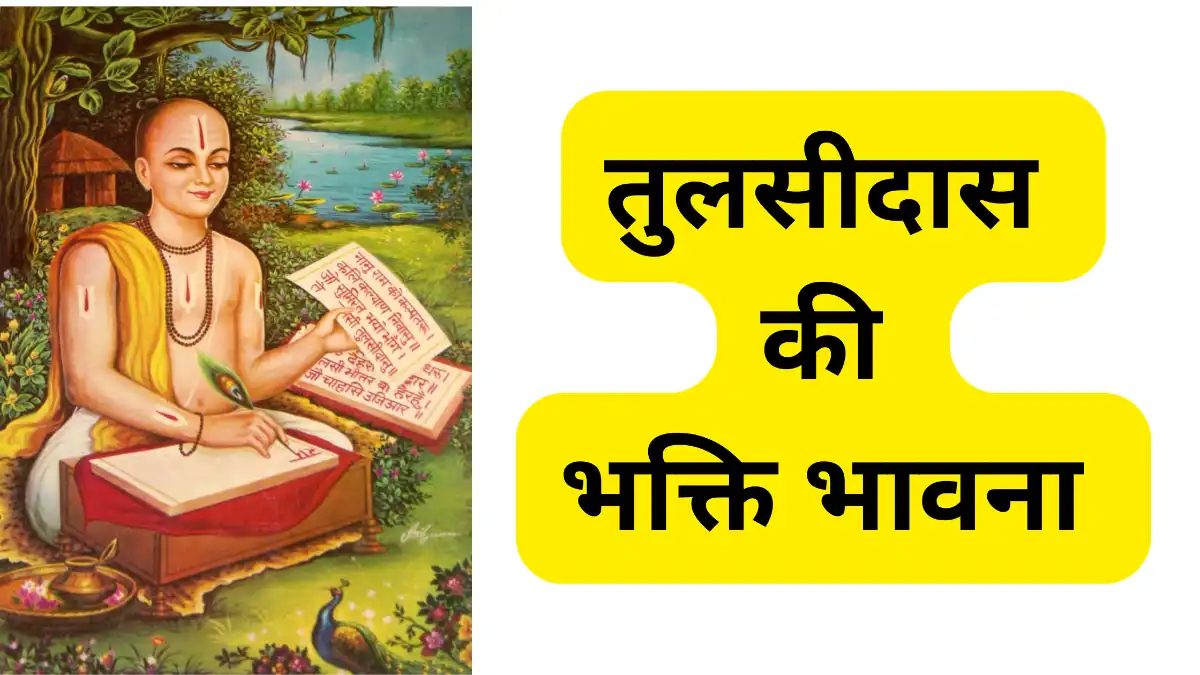तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें
गोस्वामी तुलसीदास भारतीय भक्ति-साहित्य के असीम विस्तार वाले कवि और रामकाव्य के महान प्रतिनिधि हैं। उनका सम्पूर्ण साहित्य भक्ति-भावना से परिपूर्ण है, जिसमें राम के प्रति अनन्य श्रद्धा और दास्य भाव सर्वोपरि है। तुलसीदास का जीवन और काव्य, भक्ति-काव्य की सगुण धारा का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके लिए राम केवल आदर्श देवता नहीं, बल्कि उनका स्वामी और स्वयं उनका आध्यात्मिक उद्धारकर्ता हैं।
गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:
1. तुलसी की दास्य-भक्ति
तुलसी की भक्ति का मूल आधार दास्य-भाव है। वे स्वयं को अपने प्रभु के लिए पूर्णतः समर्पित मानते हैं। उनका मानना था कि बिना सेवक-सेव्य भाव के कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने रामचरितमानस में इसे स्पष्ट रूप से कहा है:
“सेवक-सेव्य भाव विनु भव न तरिअ उरगारि।”
इस कथन से यह सिद्ध होता है कि भक्ति में आत्मसमर्पण और दास्य-भाव अत्यंत आवश्यक हैं। तुलसीदास की भक्ति में दैन्य प्रधान है। इस दैन्य के कारण वे अपने इष्टदेव राम को महान और सर्वगुण सम्पन्न तथा स्वयं को तुच्छ, छोटे और पापी मानते हैं। आत्मनिवेदन की यह प्रवृत्ति उनकी कविताओं में बार-बार दिखाई देती है:
“राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो? राम सी खरो है कौन मोसो कौन खोटो?”
यह सरल कथन तुलसी की विनयपूर्ण भक्ति का प्रतीक है, जिसमें प्रभु की महिमा के सामने आत्मा की तुच्छता और असीम श्रद्धा प्रकट होती है।
2. सगुण भक्ति –
तुलसीदास जी की भक्ति सगुण भक्ति पर आधारित है। वे भगवान राम को अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका मानना था कि प्रभु ने अपने भक्तों के कल्याण और उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। तुलसीदास जी के राम सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। वे दीनबंधु, भक्तवत्सल और दया-निधान हैं। राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय है; वे न केवल परब्रह्म हैं, बल्कि अपने भक्तों के मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा का स्रोत भी हैं।
सगुण भक्ति के दोहे:
“राम जी की भक्ति करौं, सब कष्ट मिट जाय।
जो नर राम नाम सुमिरै, सुख संसार पाय॥”
“साधु-संगत की छवि पावन, राम नाम के रति।
तुलसी कहैं जीव अब तुझ, भवसागर से छुट्टी॥”
इन दोहों से स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी की भक्ति केवल भक्ति-सिद्धांत तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जीवन को आराध्य राम के प्रति समर्पित करने का मार्ग भी बताती थी।
3. सगुण और निर्गुण का समन्वय
यद्यपि तुलसीदास जी मुख्यतः सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे, फिर भी उनकी भक्ति में सगुण और निर्गुण का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई स्थानों पर वे श्री रामचंद्र जी को विष्णु के अवतार और परब्रह्म के रूप में चित्रित करते हैं, जिससे उनकी भक्ति में निर्गुण तत्व का दर्शन भी होता है।
तुलसीदास जी स्वयं स्वीकारते हैं कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। दोनों केवल ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न साधन हैं। उनके अनुसार, भक्ति का मूल उद्देश्य वही है—ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा का उद्धार।
वे इसे स्वयं इस प्रकार स्पष्ट करते हैं:
“सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा,
गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा।”
इसका अर्थ है कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं; संत, मुनि और विद्वान सभी इसे समान रूप से मानते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति इसलिए सर्वग्राही और सार्वकालिक है, क्योंकि यह न केवल देवता की सगुण छवि को स्वीकार करती है, बल्कि निर्गुण ब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप को भी दर्शाती है।
4. ज्ञान और भक्ति का समन्वय
तुलसीदास जी अपने काव्य में ज्ञान और भक्ति का गहन समन्वय प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार, इस संसार के दुखों और मोह-माया से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य के पास दो मुख्य मार्ग हैं—ज्ञान और भक्ति। तुलसीदास जी दोनों को समान रूप से महत्व देते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि में भक्ति का मार्ग सरल और सहज है।
वे ज्ञान के मार्ग की तुलना तलवार की धार से करते हैं, जिसमें छोटी सी चूक भी घातक सिद्ध हो सकती है। इसके विपरीत, भक्ति का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम और उपलब्ध है। दोनों मार्गों का उद्देश्य—भवसागर से पार पाना—समान है, लेकिन भक्ति का मार्ग अधिक सुखद और शीघ्र फलदायी है।
तुलसीदास जी इसे स्वयं इस प्रकार व्यक्त करते हैं:
“भगतहिं ज्ञानहिं नहीं कछु भेदा,
उभय हरहिं भव सम्भव खेदा।”
इसका अर्थ है कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं, और दोनों का अंतिम गंतव्य एक ही है। फिर भी तुलसीदास जी के अनुसार, भक्ति में सरलता और सहजता के कारण यह श्रेष्ठ मार्ग है। उनके अनुसार, सच्चे मन से अपने आराध्य देव का नाम लेना ही पर्याप्त है, और इसी भक्ति के मार्ग से भक्त भवसागर को पार कर सकते हैं।
वे यह भी मानते हैं कि ज्ञान मार्ग में मनुष्य माया के मोह में फंस सकता है, जबकि भक्ति में भक्तों का हृदय भगवान से कभी नहीं भटकता। इसलिए तुलसीदास जी ने भक्ति को सहज, सुखद और सदा फलदायी मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है।
5. भक्ति वैविध्य
तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति के विविध रूपों का दर्शन होता है। मुख्यतः उनके काव्य में दास्य-भक्ति प्रधान है, जिसमें भक्त अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्म-निवेदन प्रकार की भक्ति भी मिलती है।
श्री राम के बाल-रूप का वर्णन करते हुए वात्सल्य भाव प्रकट होता है, जबकि राम को परब्रह्म रूप में दर्शाते समय निर्गुण भक्ति का दर्शन होता है। इस प्रकार, तुलसीदास जी का काव्य भक्ति के विभिन्न रूपों का समन्वय और वैविध्य प्रस्तुत करता है।
भक्ति वैविध्य का दोहा:
“राम नाम भजे दिन-रात, भवसागर कटै सब जात।
तुलसी कहैं भक्ति इस तरहे, सुख-शांति सब पावत।”
6. लोक मंगलकारी भावना
गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सर्वजनहिताय और समाज में प्रेम, सद्भावना और एकता का प्रसार करना भी है। उनके काव्य में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सच्ची भक्ति वही है जो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए प्रेरित करे। तुलसीदास मानते हैं कि केवल अपने लिए भक्ति करना अधूरी भक्ति है; लोकहितकारी भक्ति ही परम सुख और आनंद का स्रोत है।
“राम भजे सब सुख पावे, जो जन हितकारी।
दीनदयालु हित करे सब, वही है सच्चा प्यारी॥”
“सकल जगत हितकारी भक्ति, करहि तू साधक निरंतर।
जन जन में प्रेम प्रवहावे, पावे सुख संसार भर॥”
इन दोहों में तुलसीदास यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का सही स्वरूप वही है जो समाज में प्रेम, सेवा और कल्याण का संदेश फैलाए।
7. आंतरिक शुद्धता और प्रेम
तुलसीदास की भक्ति में बाहरी पूजा-पाठ या दिखावे से अधिक मन की एकाग्रता, आंतरिक शुद्धता और प्रेम को महत्व दिया गया है। उनका मानना था कि केवल रस्मों और रीति-रिवाजों का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं, बल्कि व्यक्ति का हृदय सच्चे प्रेम, करुणा और भक्ति भावना से परिपूर्ण होना आवश्यक है।
तुलसीदास की भक्ति में प्रेम का अर्थ केवल राम के प्रति निष्ठा नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति, दया और सेवा भी है। उनके अनुसार, जो व्यक्ति हृदय से निर्मल और प्रेमपूर्ण है, वही सच्ची भक्ति में रत होता है।
“मन को मनसा शुद्ध करि, प्रेम भाव रखो हियारे।
सदा सत्कर्म में लीन रहो, भजत राम सदा प्यारे॥”
यह दोहा स्पष्ट करता है कि तुलसीदास के अनुसार आंतरिक शुद्धता और प्रेम ही भक्ति की आत्मा हैं, न कि केवल बाहरी अनुष्ठान।
8. राम के प्रति पूर्ण समर्पण
गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति का केंद्र भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण था। उनके काव्य और दोहों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उनका भक्ति मार्ग सच्चा, सरल और निःस्वार्थ था। तुलसीदास ने अपने हृदय में राम के लिए जो प्रेम और भक्ति विकसित की, वह किसी प्रकार के आडंबर या दिखावे से रहित थी।
उनकी भक्ति में न केवल भक्ति की भावना का शुद्ध रूप था, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुशासन, प्रेम और निष्ठा का पर्याय भी थी। तुलसीदास का मानना था कि राम के प्रति समर्पण केवल वचन या कर्म से नहीं, बल्कि पूर्ण मन, हृदय और आत्मा से होना चाहिए।
“राम रटत हियँ लीन रहो, न कोई भेद न द्वेष।
सच्चा भक्त जो समर्पित, पावे प्रेम अनुपम भेस॥”
इस दोहे में तुलसीदास यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें पूर्ण समर्पण और प्रेम हो, न कि बाहरी आडंबर।
9. सेवक-सेव्य भाव
गोस्वामी तुलसीदास के भक्ति दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष ‘सेवक-सेव्य भाव’ है। उनके अनुसार, सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त स्वयं को सेवा करने वाला (सेवक) और परमात्मा या ईश्वर को सेवा योग्य (सेव्य) मानकर पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करे। तुलसीदास के विचार में, यह भाव जीवन में सच्चा मार्गदर्शन और मुक्ति का साधन है।
वे कहते हैं कि बिना सेवक-सेव्य भाव के संसार का सागर पार करना कठिन है, क्योंकि यह भावना व्यक्ति को अहंकार, स्वार्थ और तुच्छता से दूर रखती है। सेवक-सेव्य भाव से व्यक्ति में दया, करुणा और निःस्वार्थ प्रेम का विकास होता है, जो उसे आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से उन्नत बनाता है।
“जो सेवक-सेव्य भाव राखे, निस्वार्थ मन सदा भरे।
सागर जीवन के पार पावे, राम रूप नित्य चले चले॥”
इस दोहे में तुलसीदास स्पष्ट करते हैं कि सच्ची भक्ति और जीवन की सफलता इस भाव के बिना अधूरी है।
निष्कर्ष
निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि तुलसीदास की भक्ति-भावना का मूल स्वरूप सगुण भक्ति है। वे भगवान राम को अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं और उनकी भक्ति का केंद्र राम की सगुण रूप में आराधना करना है। तुलसीदास की भक्ति में दास्य-भाव सर्वोपरि है, अर्थात् भक्त की भक्ति का आधार ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निःस्वार्थ सेवा भाव है।
उनकी भक्ति केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोकहित, प्रेम, करुणा और सामाजिक सद्भावना का भी समावेश है। तुलसीदास का संदेश स्पष्ट है कि सच्ची भक्ति वही है जो प्रेम, समर्पण और सेवा के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण में योगदान दे।
इन्हें भी पढ़े : कृष्ण काव्याधारा की प्रमुख विशेषता।। सूरदास का वात्सल्य वर्णन।। बिहारी को गागर मे सागर भरने वाला कवि क्यों कहा जाता है।। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता।। मीरा की काव्यागत विशेषता ।। भारतेन्दु युग की विशेषता।। प्रगतिवाद की विशेषता।। भक्तिकाल की प्रमुख विशेषता ।। कबीर की काव्य भाषा शैली की विशेषता ।। कबीर के रहस्यवाद ।। कबीर दास की विद्रोही भावना ।। कबीर एक समाज सुधारक ।। राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएँ ।। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण .।। कबीर की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए (kabir ki bhakti bhavna ka vishleshan kijiye)