प्रतिवेदन लेखन क्या है: मानव सभ्यता के विकास में लेखन की प्रमुख भूमिका रही है। जब भी कोई घटना घटती है, उसका लिपिबद्ध विवरण भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनता है। प्रतिवेदन लेखन इसी परंपरा का एक संगठित रूप है, जिसमें किसी घटना अथवा स्थिति का तार्किक एवं तथ्यात्मक विवरण क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।
प्रतिवेदन केवल सूचनाओं का दस्तावेज़ भर नहीं है बल्कि यह प्रशासन, शिक्षा, शोध, पत्रकारिता और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का आधार भी है।
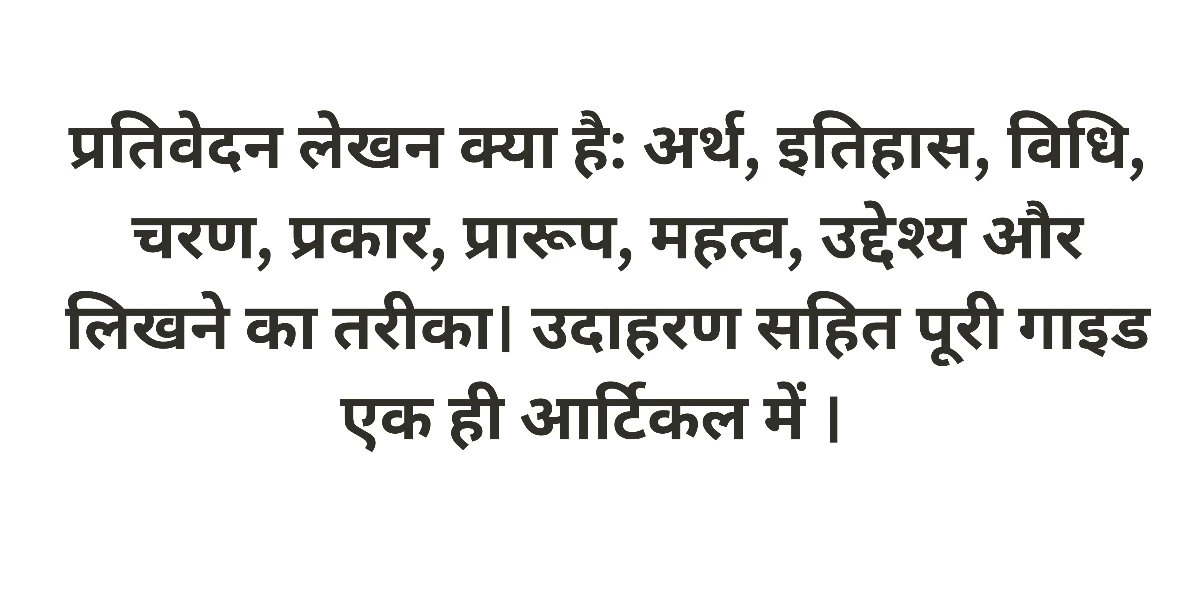
प्रतिवेदन लेखन क्या है
प्रतिवेदन लेखन का अर्थ है किसी घटना, समस्या, गतिविधि या विषय से सम्बन्धित तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं को लिखित रूप में क्रमबद्ध और यथार्थपरक रूप से प्रस्तुत करना। यह निबंध या लेख की भाँति व्यक्तिगत विचारों पर आधारित नहीं होता, बल्कि तथ्यपरक और औपचारिक शैली में लिखा जाता है।
उदाहरणस्वरूप—यदि किसी विद्यालय में “स्वच्छता अभियान” आयोजित किया गया, तो उसमें प्रयोग किए गए संसाधन, उपस्थित लोगों की संख्या, किए गए कार्य और अभियान का परिणाम, सब कुछ प्रतिवेदन में व्यवस्थित रूप से लिखा जाएगा।
प्रतिवेदन लेखन का अर्थ
‘Report’ का हिंदी पर्याय ‘प्रतिवेदन’ है। इसमें “प्रति” का अर्थ है “वापस” और “वेदन” का अर्थ है “सूचना देना”। अर्थात्, प्रतिवेदन वह लिखित दस्तावेज़ है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति, संस्था अथवा विभाग किसी घटना या कार्य की वास्तविक जानकारी किसी उच्च अधिकारी, पाठक या समाज को उपलब्ध कराता है।
इसका मूल आधार वस्तुनिष्ठता (objectivity) है, न कि कल्पना।
प्रतिवेदन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
प्राचीन काल में घटनाओं का संकलन शिलालेख, ताम्रपत्र और पांडुलिपियों में किया जाता था। अशोक के शिलालेख, अकबरनामा, राजतरंगिणी और स्मृति-साहित्य में प्रतिवेदनात्मक स्वर मिलते हैं।
आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक कार्यों और युद्ध संबंधी वृत्तांतों ने प्रतिवेदन को औपचारिक रूप दिया। स्वतंत्रता संग्राम में अनेक प्रतिवेदन तैयार किए गए जिनके आधार पर आंदोलन की दिशा तय होती थी।
आज डिजिटल युग में प्रतिवेदन केवल लिखित नहीं, बल्कि चार्ट, ग्राफ़, पावरपॉइंट और डाटा शीट के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।
प्रतिवेदन लिखने की विधि
प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है:
1. सूचना संग्रहण (Information Collection)
प्रतिवेदन तैयार करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सटीक और विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करना।
- घटना, परियोजना, या विषय से संबंधित सभी तथ्य एकत्र करें।
- स्रोतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें, जैसे सरकारी रिपोर्ट, आधिकारिक दस्तावेज़, प्रत्यक्ष साक्ष्य या विशेषज्ञों की राय।
- नोट्स बनाते समय तथ्यों को क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप में लिखें ताकि बाद में उपयोग करना आसान हो।
उदाहरण: यदि आप किसी स्कूल कार्यक्रम पर प्रतिवेदन लिख रहे हैं, तो आयोजन की तिथि, स्थान, उपस्थित लोग और मुख्य गतिविधियों को नोट करें।
2. विश्लेषण (Analysis)
संग्रहित जानकारी को वर्गीकृत और प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करना आवश्यक है।
- महत्वपूर्ण तथ्यों को मुख्य बिंदुओं के रूप में अलग करें।
- अनावश्यक या अप्रासंगिक जानकारी को हटा दें।
- डेटा और सूचना को तार्किक क्रम में रखें, ताकि प्रतिवेदन पढ़ने में आसान और समझने में स्पष्ट हो।
उदाहरण: कार्यक्रम के दौरान कौन-कौन से आयोजन हुए, किसने भाग लिया, किस गतिविधि में विशेष सफलता मिली आदि।
3. भाषा चयन (Language Selection)
प्रतिवेदन की भाषा स्पष्ट, सरल और औपचारिक होनी चाहिए।
- कठिन या साहित्यिक शब्दों का प्रयोग सीमित रखें।
- संक्षिप्त वाक्य और सरल व्याकरण का प्रयोग करें।
- भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पाठक को तुरंत तथ्य और संदेश समझ में आए।
उदाहरण: “कार्यक्रम बहुत अच्छा था” की बजाय लिखें, “कार्यक्रम में छात्रों ने सक्रिय भाग लिया और सभी गतिविधियाँ समयानुसार संपन्न हुईं।”
4. संक्षिप्तता (Brevity)
प्रतिवेदन अनावश्यक विस्तार से बचते हुए सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए।
- केवल मुख्य बिंदुओं और आवश्यक तथ्यों को शामिल करें।
- किसी भी तरह की जानकारी जो प्रतिवेदन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, उसे हटा दें।
उदाहरण: आयोजन में हुई प्रत्येक छोटी घटना का विवरण देने की बजाय, केवल मुख्य घटनाओं और उनके परिणामों का उल्लेख करें।
5. निष्पक्षता (Objectivity)
प्रतिवेदन में व्यक्तिगत राय या पक्षपात नहीं होना चाहिए।
- तथ्य आधारित लेखन पर ध्यान दें।
- किसी भी प्रकार की भावनात्मक टिप्पणी या व्यक्तिगत धारणा को शामिल न करें।
- निष्पक्षता पाठक में विश्वास पैदा करती है और प्रतिवेदन की विश्वसनीयता बढ़ाती है।
उदाहरण: “कुल कार्यक्रम संतोषजनक था” एक निष्पक्ष निष्कर्ष है, जबकि “यह सबसे बेहतरीन कार्यक्रम था” व्यक्तिगत राय है।
6. प्रारूप का अनुसरण (Following a Format)
प्रतिवेदन निर्धारित ढाँचे और स्वरूप में लिखा जाना चाहिए।
- शीर्षक, तिथि, उद्देश्य, घटनाक्रम, निष्कर्ष आदि को क्रमवार रूप में रखें।
- अलग-अलग प्रकार के प्रतिवेदन (जैसे घटनाविशेष प्रतिवेदन, परियोजना रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट) के लिए अलग- अलग प्रारूप होते हैं।
- सही प्रारूप से प्रतिवेदन पेशेवर और व्यवस्थित लगता है।
उदाहरण प्रारूप:
- शीर्षक
- तिथि और स्थान
- उद्देश्य
- मुख्य घटनाक्रम / विवरण
- निष्कर्ष / सुझाव
7. सम्पादन (Editing)
अंतिम चरण में प्रतिवेदन का भाषाई और तथ्यात्मक सुधार किया जाता है।
- वर्तनी और व्याकरण की जांच करें।
- तथ्य और आँकड़ों की पुष्टि करें।
- वाक्यों को और अधिक स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाएं।
उदाहरण: यदि किसी आयोजन की तिथि गलत लिखी है, तो उसे सही करें; किसी वाक्य को सरल और स्पष्ट बनाएं।
प्रतिवेदन लेखन के चरण
1. विषय की पहचान – यह तय करना कि किस घटना या स्थिति पर प्रतिवेदन लिखना है।
2. डेटा संग्रह – आँकड़े, दस्तावेज़, प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात्कार या सर्वेक्षण।
3. रूपरेखा बनाना – महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रमवार लिखना।
4. मसौदा लेखन – प्रारंभिक रूप से विवरण लिखकर जाँच करना।
5. अंतिम रूप – त्रुटियाँ सुधारकर परिष्कृत प्रतिवेदन तैयार करना।
प्रतिवेदन लेखन के प्रकार
प्रतिवेदन कई आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं।
प्रकृति के आधार पर
- व्यक्तिगत प्रतिवेदन – व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन आधारित।
- सामूहिक प्रतिवेदन – किसी समिति अथवा टीम द्वारा तैयार।
उद्देश्य के आधार पर
- सूचनात्मक प्रतिवेदन – केवल सूचना देने के लिए।
- विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन – कारण और समाधान प्रस्तुत करने वाला।
क्षेत्र के आधार पर
- शैक्षणिक प्रतिवेदन
- प्रशासनिक प्रतिवेदन
- पत्रकारिता/समाचार प्रतिवेदन
- वैज्ञानिक एवं शोध प्रतिवेदन
- व्यावसायिक प्रतिवेदन
- कानूनी प्रतिवेदन
- आपदा प्रतिवेदन
प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप
आमतौर पर प्रतिवेदन का प्रारूप निम्नलिखित होता है:
1. शीर्षक या विषय का उल्लेख
- प्रतिवेदन का शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट और विषय-संवेदनशील होना चाहिए।
- यह पाठक को बताता है कि प्रतिवेदन किस विषय पर आधारित है।
उदाहरण: - “विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों पर प्रतिवेदन”
- “कृषि विकास योजना 2025: प्रभाव और सुझाव”
2. तिथि और स्थान
- प्रतिवेदन लिखते समय उसकी तिथि और स्थान लिखना आवश्यक है।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्रतिवेदन कब और कहां तैयार किया गया।
उदाहरण:
तिथि: 18 सितंबर 2025
स्थान: दिल्ली
3. प्रस्तावना या पृष्ठभूमि
- इस खंड में प्रतिवेदन लिखने का कारण और उद्देश्य बताया जाता है।
- पृष्ठभूमि में समस्या, घटना या स्थिति का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।
उदाहरण:
इस प्रतिवेदन का उद्देश्य हमारे विद्यालय में आयोजित “स्वच्छता अभियान” की गतिविधियों और उनके प्रभाव का विश्लेषण करना है।
4. मुख्य विवरण (तथ्य, आँकड़े, घटनाक्रम)
- यह प्रतिवेदन का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है।
- इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य, आँकड़े, घटनाक्रम, निरीक्षण और अवलोकन क्रमबद्ध रूप में लिखे जाते हैं।
- आवश्यक हो तो इसे उपखंडों, तालिकाओं, बुलेट पॉइंट्स और चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।
उदाहरण:
- अभियान में कुल 100 छात्रों ने भाग लिया।
- विद्यालय के सभी वर्गों में 5 दिन तक सफाई गतिविधियाँ संचालित हुई।
- सफाई के दौरान पाए गए मुख्य समस्याएँ – कचरा प्रबंधन की कमी, प्रदूषण।
5. निष्कर्ष
- निष्कर्ष में मुख्य तथ्यों का सारांश दिया जाता है।
- इसमें प्रतिवेदन से मिलने वाले परिणाम, प्रभाव या स्थिति का संक्षिप्त विवरण होता है।
उदाहरण:
स्वच्छता अभियान ने छात्रों में जागरूकता बढ़ाई और विद्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने में मदद की।
6. सुझाव (यदि आवश्यक हो)
- यदि प्रतिवेदन किसी समस्या या सुधारात्मक उपाय से संबंधित है, तो सुझावों का उल्लेख किया जाता है।
- सुझाव व्यावहारिक और सरल होने चाहिए।
उदाहरण: - विद्यालय में नियमित रूप से स्वच्छता निरीक्षण किया जाए।
- कचरे के लिए अलग-अलग बिन रखे जाएँ।
7. प्रस्तुतकर्ता का नाम और पद
- अंत में प्रतिवेदन लिखने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पद और हस्ताक्षर लिखना आवश्यक है।
उदाहरण:
प्रस्तुतकर्ता: अजय कुमार
पद: सहायक शिक्षक
प्रतिवेदन लेखन का महत्व
1. प्रशासनिक कार्यवाही को सरल बनाना
प्रतिवेदन लेखन प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकारी और निजी संस्थानों में निर्णय लेने, योजनाओं को लागू करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिवेदन एक आवश्यक दस्तावेज़ होता है। यह अधिकारीयों और कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रमाणिक रूप में प्रदान करता है, जिससे समय की बचत होती है और कार्यवाही अधिक प्रभावशाली बनती है।
2. शिक्षा जगत में गतिविधियों का स्थायी दस्तावेज़ तैयार करना
शिक्षा क्षेत्र में प्रतिवेदन लेखन का महत्व अत्यधिक है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आयोजित गतिविधियों, कार्यशालाओं, परियोजनाओं और परीक्षाओं का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के माध्यम से तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज़ न केवल वर्तमान वर्ष की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है बल्कि भविष्य में छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन के लिए मार्गदर्शन और संदर्भ का काम भी करता है।
3. शोध और विज्ञान में प्रमाण और डेटा उपलब्ध कराना
प्रतिवेदन लेखन शोध और वैज्ञानिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता अपने प्रयोगों, प्रेक्षणों और परिणामों को प्रतिवेदन के रूप में संकलित करते हैं। यह वैज्ञानिक समुदाय को प्रमाणित डेटा प्रदान करता है, जिससे किसी विषय पर निष्कर्ष निकालना, नए प्रयोग करना और ज्ञान को आगे बढ़ाना संभव होता है। बिना व्यवस्थित प्रतिवेदन के शोध कार्य का मूल्यांकन और पुनःप्रयोग करना कठिन हो जाता है।
4. कंपनियों को लाभ-हानि और प्रगति का पता चलाना
व्यवसायिक क्षेत्र में प्रतिवेदन कंपनियों के लिए वित्तीय और प्रगति संबंधी जानकारी का मूल स्रोत होते हैं। इससे कंपनियों को यह पता चलता है कि कौन से प्रोजेक्ट लाभकारी हैं, कौन से क्षेत्र सुधार की आवश्यकता रखते हैं और कंपनी की कुल प्रगति कैसी रही। इन आंकड़ों के आधार पर रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, जिससे व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित होती है।
5. समाज और सरकार को किसी स्थिति की वास्तविक तस्वीर देखने का मौका देना
प्रतिवेदन समाज और सरकार के लिए किसी भी समस्या या स्थिति की वास्तविक जानकारी प्रदान करता है। चाहे वह प्राकृतिक आपदा, सामाजिक समस्या या विकास परियोजना हो, प्रतिवेदन के माध्यम से नीति निर्माता और समाज की हितधारक वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं और त्वरित तथा उचित निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी और तथ्यात्मक बनाता है।
6. मीडिया एवं पत्रकारिता में समाचार का विश्वसनीय आधार बनना
मीडिया और पत्रकारिता क्षेत्र में भी प्रतिवेदन लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार और रिपोर्टिंग के लिए विश्वसनीय तथ्यों और डेटा की आवश्यकता होती है। प्रतिवेदन पत्रकारों को घटनाओं और परिस्थितियों की सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे सटीक और प्रमाणिक समाचार तैयार कर सकते हैं। इससे समाचार की विश्वसनीयता बढ़ती है और जनता तक वास्तविक जानकारी पहुँचती है।
प्रतिवेदन लेखन के उद्देश्य
1. तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना
प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य सटीक और प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करना होता है। यह किसी घटना, कार्य, परियोजना या गतिविधि के बारे में तथ्यात्मक विवरण देता है, जिससे पाठक या संबंधित अधिकारी पूरी स्थिति को समझ सकें। तथ्यात्मक जानकारी होने से अफवाहों और अनुमान पर आधारित निर्णयों से बचा जा सकता है और कार्यवाही अधिक विश्वसनीय बनती है।
2. निर्णय प्रक्रिया में सहायता करना
प्रतिवेदन लेखन निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाता है। प्रशासन, संस्थान या व्यवसाय में किसी नीति, योजना या परियोजना को लागू करने से पहले संबंधित विवरणों, आंकड़ों और विश्लेषणों को समझना आवश्यक होता है। प्रतिवेदन इस जानकारी को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे प्रबंधक और अधिकारी सही निर्णय ले सकते हैं।
3. भविष्य के लिए दस्तावेज़ सुरक्षित रखना
प्रतिवेदन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है भविष्य में संदर्भ के लिए जानकारी सुरक्षित रखना। किसी भी गतिविधि, परियोजना या अध्ययन का विवरण प्रतिवेदन में दर्ज होने से भविष्य में उसका मूल्यांकन, पुनःअवलोकन और तुलना करना आसान हो जाता है। यह दस्तावेज़ संस्थानों और शोधकर्ताओं के लिए स्थायी रिकॉर्ड का कार्य करता है।
4. पाठकों को निष्पक्ष विवरण देना
प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं, बल्कि इसे निष्पक्ष और तटस्थ ढंग से प्रस्तुत करना भी है। लेखक अपनी व्यक्तिगत राय से प्रभावित हुए बिना घटनाओं और तथ्यों का विवरण देता है। इससे पाठक पूरी सच्चाई को समझ पाते हैं और किसी प्रकार की भ्रामक या पक्षपाती जानकारी से बचा जा सकता है।
5. सुधार और सुझाव प्रस्तुत करना
कई प्रतिवेदन सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समस्याओं का विश्लेषण कर सुधार और सुझाव भी प्रदान करते हैं। यह उद्देश्य किसी परियोजना या गतिविधि की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और भविष्य में संभावित खामियों को कम करने में मदद करता है। सुझावों के माध्यम से न केवल वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन होता है बल्कि आगे की रणनीति बनाने में भी मार्गदर्शन मिलता है।
प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है
– औपचारिक एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।
– घटना के अनुसार कालक्रमिक या तार्किक क्रम चुनें।
– सूचनाएँ संपूर्ण परंतु संक्षिप्त हों।
– शीर्षक, तिथि, समय और स्थान अवश्य हों।
– अंत में निष्कर्ष एवं आवश्यक सुझाव शामिल हों।
प्रतिवेदन लेखन के उदाहरण
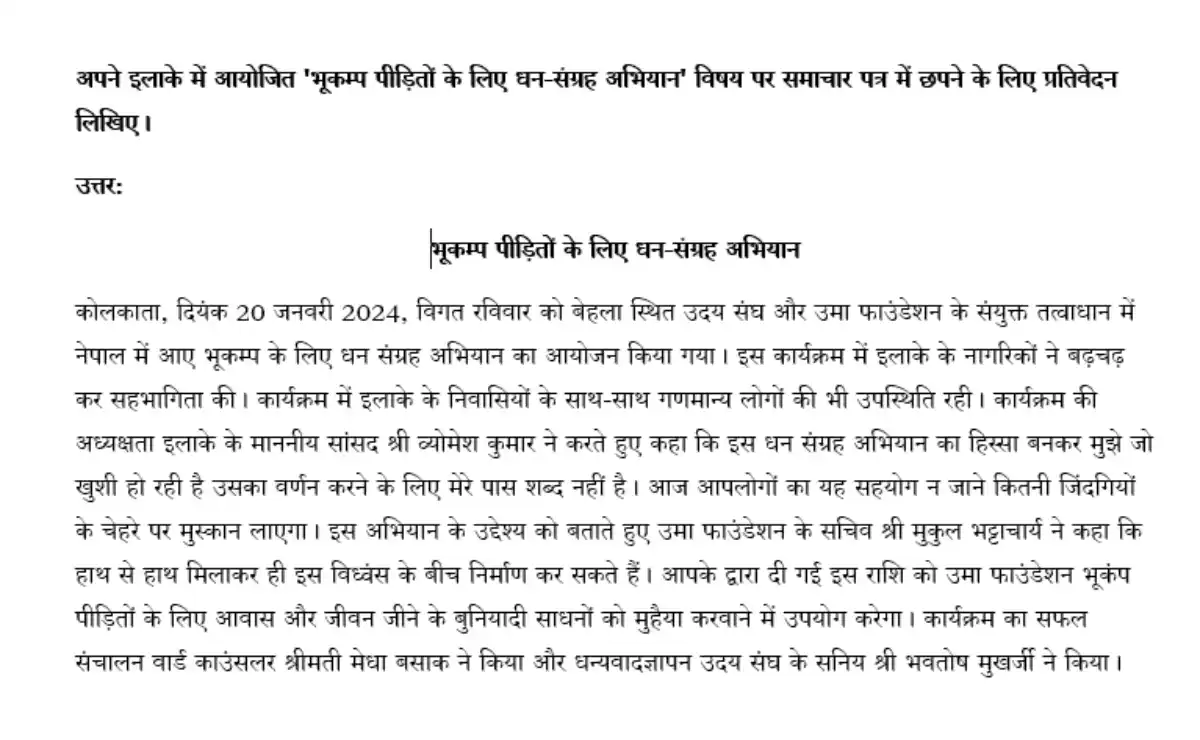
उदाहरण 1: विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का प्रतिवेदन
विज्ञान प्रदर्शनी प्रतिवेदन
सरस्वती विद्यालय, लखनऊ,12 जनवरी 2025। विद्यालय में 12 जनवरी को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डी.एस.आर. कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. वर्मा थे। छात्रों ने जल संरक्षण, सौर ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में लगभग 500 दर्शक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सर्वश्रेष्ठ मॉडल को पुरस्कृत किया गया।
प्रस्तुतकर्ता: आलोक यादव, कक्षा 12 विज्ञान
उदाहरण 2: प्राकृतिक आपदा का प्रतिवेदन
भूकंप प्रभावित क्षेत्र का प्रतिवेदन
कच्छ, गुजरात, 5 जून 2025: गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। 40 गाँव प्रभावित हुए। लगभग 200 मकान ढह गए और 50 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य सरकार ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में लगी हैं।
प्रस्तुतकर्ता: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी
उदाहरण 3: व्यावसायिक मासिक बिक्री प्रतिवेदन
बिक्री प्रतिवेदन – अगस्त 2025
एबीसी कंपनी लिमिटेड, 1 सितंबर 2025: अगस्त माह में कुल बिक्री ₹75 लाख रही। यह पिछले माह की तुलना में 15% अधिक है। उत्तर भारत में बिक्री में सर्वाधिक वृद्धि हुई। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से कंपनी को नया ग्राहक वर्ग मिला।
प्रस्तुतकर्ता: विपणन प्रबंधक
केस स्टडी : भारत में आपदा प्रतिवेदन
2018 में केरल में आई बाढ़ का विस्तृत प्रतिवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तैयार किया था। इसमें वर्षा की मात्रा, प्रभावित जिलों, मृतकों की संख्या, राहत की मात्रा, पुनर्वास कार्य और भविष्य की रणनीति का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर केंद्र ने पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी।
यह उदाहरण दर्शाता है कि प्रतिवेदन महज़ सूचनाएँ संकलित करने का कार्य नहीं करता बल्कि व्यावहारिक नीतिगत निर्णयों का भी आधार बनता है।
निष्कर्ष
प्रतिवेदन लेखन एक संगठित और औपचारिक शैली है, जो तथ्यों एवं आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है। यह न केवल शैक्षणिक जगत में उपयोगी है, बल्कि राजनीति, प्रशासन, व्यावसायिक प्रबंधन, पत्रकारिता और वैज्ञानिक शोध जैसे क्षेत्रों में भी इसका महत्व अत्यधिक है।
यदि प्रतिवेदन स्पष्ट, संक्षिप्त और निष्पक्ष हो तो यह निर्णय प्रक्रिया के लिए दिशा-दर्शक बन सकता है।
इसे भी पढ़ें :
- लेखन कौशल (Writing Skill in Hindi): अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषताएं, विधियां, उद्देश्य, उपयोगिता, प्रकार
- स्तंभ लेखन क्या है पत्रकारिता में स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य है (Stambh yojna kya hai)
- फीचर लेखन के कितने प्रकार है(feature lekhan ke prakar)- परिभाषा,स्वरूप, तत्व, उद्देश्य
- समाचार लेखन के तत्व और समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं
- अनुच्छेद लेखन