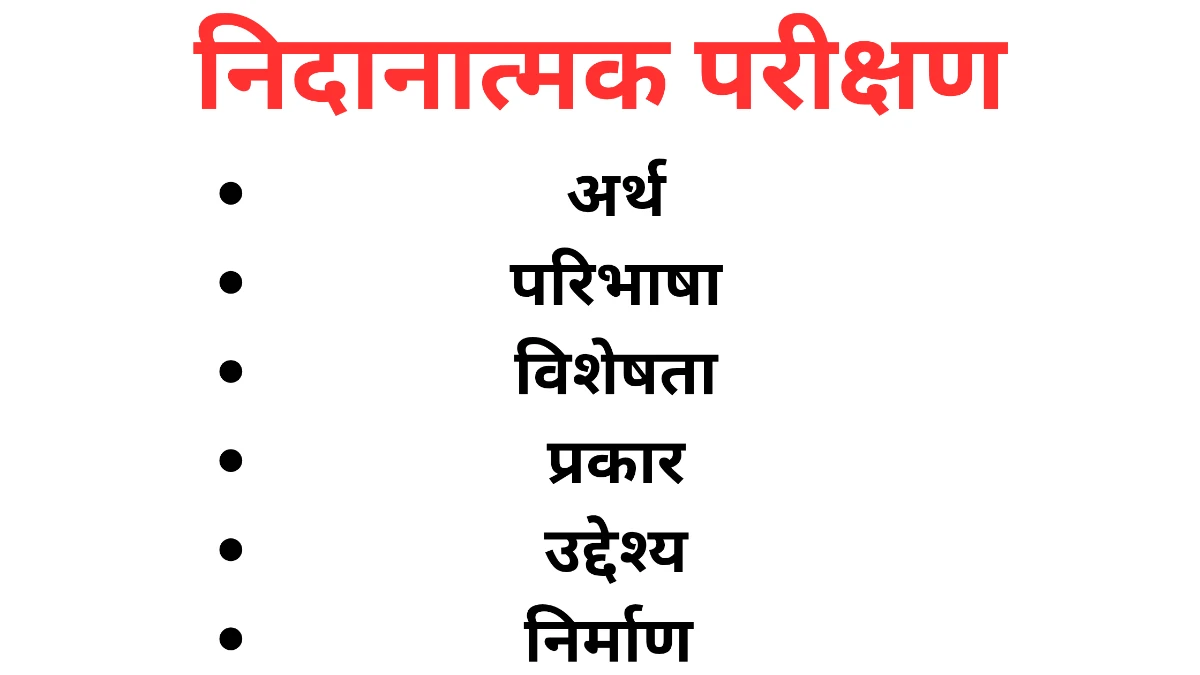निदानात्मक परीक्षण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार, उद्देश्य, निर्माण Nidanatmak Parikshan In Hindi
‘निदान’ शब्द अंग्रेज़ी के ‘Diagnosis’ का हिन्दी रूप है, जिसका अर्थ है किसी समस्या, रोग या स्थिति के मूल कारण का पता लगाना या उसका निर्णय करना। यह शब्द मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र में रोग की पहचान के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
निदानात्मक परीक्षण का अर्थ (Meaning of Diagnostic Test)
‘निदान’ शब्द अंग्रेज़ी के Diagnosis का हिन्दी रूप है, जिसका अर्थ है — किसी समस्या या रोग के मूल कारण का निर्णय करना। जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सीखने में आने वाली कठिनाइयों, मन्दता या पिछड़ेपन को पहचानकर उन समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षण करते हैं, तो उसे निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है।
निदानात्मक परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जो विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं, त्रुटियों या कमजोरियों का पता लगाने के लिए बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य केवल कमियों को पहचानना नहीं, बल्कि उनके मूल कारणों का विश्लेषण कर उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाना भी होता है। इन परीक्षणों से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यकताओं को समझ पाते हैं और उसे उसी अनुरूप सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उसकी शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा (Definition of Diagnostic Test)
निदानात्मक परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्र की अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों, कमियों या त्रुटियों की पहचान की जाती है ताकि उन्हें दूर करने के लिए उचित शिक्षण उपाय अपनाए जा सकें।
गुड (Good) के अनुसार —
“निदान का अर्थ है अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण।”
योकम एवं सिम्पसन (Yokam and Simpson) के अनुसार —
“निदान किसी कठिनाई का उसके चिह्नों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है।”
मरसेल (Mursell) के अनुसार —
“जिस शिक्षण में छात्र की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है।”
क्रोनबाख (Cronbach) के अनुसार —
“निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने तथा कमज़ोर प्रदर्शन के कारणों को खोजने के लिए किया जाता है।”
थॉर्नडाइक (Thorndike) के अनुसार —
“शिक्षा में निदान का अर्थ है सीखने की कठिनाइयों की प्रकृति और कारणों का पता लगाना ताकि प्रभावी सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।”
निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य (Objectives of Diagnostic Test)
नैदानिक या निदानात्मक परीक्षण (Diagnostic Test) शिक्षा क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने की कमजोरियों, कठिनाइयों और उनकी व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकताओं का पता लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि छात्र कहाँ, क्यों और किस कारण से पिछड़ रहा है, ताकि उसके अनुरूप शिक्षण-सहायता प्रदान की जा सके। नीचे नैदानिक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है—
1. किसी विशिष्ट विषय में छात्र की कठिनाइयों का पता लगाना
निदानात्मक परीक्षण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह जानना है कि छात्र को किसी विशेष विषय, अध्याय या अवधारणा में कहाँ कठिनाई आ रही है। उदाहरण के लिए, गणित में यदि कोई विद्यार्थी बार-बार समान प्रकार की गलती करता है, तो इस परीक्षण से यह स्पष्ट हो सकता है कि समस्या गणना में है या अवधारणा की समझ में।
2. ज्ञानार्जन में बाधक तत्वों की पहचान
हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता और गति अलग होती है। कुछ छात्रों को भाषाई अड़चन, ध्यान की कमी या पूर्व ज्ञान की कमी जैसी समस्याएँ होती हैं। नैदानिक परीक्षण इन बाधक तत्वों को पहचानता है ताकि शिक्षक उचित उपाय कर सकें और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
3. शिक्षण विधियों में सुधार के लिए सुझाव देना
यदि परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकतर विद्यार्थियों को किसी विषय में कठिनाई हो रही है, तो यह संकेत होता है कि शिक्षण विधि में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस प्रकार, नैदानिक परीक्षण शिक्षक को अपनी शिक्षण रणनीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित करता है।
4. पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों में संशोधन
निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि क्या पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों की समझ के स्तर के अनुरूप हैं या नहीं। यदि नहीं, तो शिक्षक या शिक्षा नियोजक छात्रों की आवश्यकताओं और कमजोरियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।
5. उपलब्धि परीक्षण (Achievement Test) में सहायता
निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्धि परीक्षण के प्रश्नों का चयन किया जा सकता है, जिससे छात्रों की वास्तविक उपलब्धियों का सही मूल्यांकन संभव हो सके। यह परीक्षणों की विश्वसनीयता और वैधता (Reliability and Validity) को भी बढ़ाता है।
6. मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सार्थक बनाना
निदानात्मक परीक्षण केवल अंक देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझने और सुधारने में सहायता करता है। इससे मूल्यांकन केवल परिणाम नहीं, बल्कि प्रगति और क्षमता-विकास का भी आकलन बन जाता है।
7. उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की व्यवस्था
निदानात्मक परीक्षण के परिणामों से शिक्षक यह तय कर सकते हैं कि किन विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या पुनः शिक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार, उपचारात्मक शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था करके हर छात्र की सीखने की गति में सुधार किया जा सकता है।
8. साफल्य परीक्षा (Achievement Test) के निर्माण में सहयोग
निदानात्मक परीक्षण प्रश्नों के प्रकार, कठिनाई स्तर और विषय-वस्तु की उपयुक्तता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे परीक्षा अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनती है, जो विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता को दर्शाती है।
निष्कर्ष
निदानात्मक परीक्षण केवल कमियों का पता लगाने का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षण-सीखने की पूरी प्रक्रिया को सुधारने का माध्यम है। इसके द्वारा शिक्षक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझते हैं, शिक्षण पद्धतियों को परिष्कृत करते हैं और समग्र शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। इस प्रकार, नैदानिक परीक्षण शिक्षा के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक, उपयोगी और प्रभावशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।
निदानात्मक परीक्षाओं की विशेषताएँ (Characteristics of Diagnostic Test) —
निदानात्मक परीक्षाएँ (Diagnostic Tests) विद्यार्थियों की सीखने की कमजोरियों, त्रुटियों और व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए बनाई जाती हैं। इन परीक्षाओं का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि छात्र की कठिनाइयों के मूल कारणों का विश्लेषण करना होता है ताकि उचित उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके। एक प्रभावी निदानात्मक परीक्षा में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ पाई जाती हैं—
1. पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग
निदानात्मक परीक्षाएँ शिक्षण प्रक्रिया से अलग नहीं होतीं, बल्कि यह पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होती हैं। इन्हें शिक्षण के विभिन्न चरणों में इस प्रकार सम्मिलित किया जाता है कि शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति को निरंतर जाँच सके।
2. प्रमापीकृत या गैर-प्रमापीकृत स्वरूप
सामान्यतः ये परीक्षाएँ प्रमापीकृत (Standardized) होती हैं, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता बनी रहती है। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मत है कि निदानात्मक परीक्षाएँ व्यक्तिगत स्तर पर बनाई जानी चाहिए ताकि हर छात्र की विशिष्ट कठिनाइयों को पहचाना जा सके।
3. विशिष्ट उद्देश्य आधारित
इन परीक्षाओं का उद्देश्य बहुत स्पष्ट और विशिष्ट होता है — जैसे गणितीय अवधारणाओं की समझ, भाषा की व्याकरणिक त्रुटियों की पहचान, या वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्पष्टता जाँचना। ये सामान्य मूल्यांकन की तरह नहीं, बल्कि विशेष समस्या के निदान पर केंद्रित होती हैं।
4. योग्यता का नहीं, कमजोरी का परीक्षण
निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता को मापना नहीं है, बल्कि विषय से जुड़ी उसकी कमियों और त्रुटियों का पता लगाना है, ताकि उन्हें सुधारने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाई जा सकें।
5. समय-सीमा का अभाव
इन परीक्षाओं में किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता क्योंकि उद्देश्य विद्यार्थियों पर दबाव डालना नहीं, बल्कि उनकी सीखने की प्रक्रिया को समझना है। शिक्षक आवश्यकता अनुसार समय दे सकता है ताकि छात्र आराम से प्रश्नों को हल कर सके।
6. विश्लेषणात्मक स्वरूप
निदानात्मक परीक्षाएँ अत्यंत विश्लेषणात्मक होती हैं। ये किसी भी शिक्षण प्रक्रिया या विषय-वस्तु को छोटे-छोटे घटकों में बाँटकर यह जानने का प्रयास करती हैं कि छात्र किस स्तर पर त्रुटि कर रहा है।
7. प्रयोग आधारित मानक
इन परीक्षाओं का निर्माण ठोस शैक्षणिक अनुसंधानों और प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इनके परिणाम ऐसे मानकों से तुलना करके देखे जाते हैं जिन्हें वास्तविक शिक्षण अनुभवों से सत्यापित किया गया हो।
8. अंकों का कोई विशेष महत्व नहीं
निदानात्मक परीक्षाओं में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों की बजाय उसकी प्रतिक्रिया और उत्तर देने की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि छात्र किन प्रकार के प्रश्न हल कर पाता है और कहाँ उसे कठिनाई होती है।
9. मानसिक प्रक्रिया का स्पष्ट चित्रण
इन परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे — सोचने का तरीका, समझने की गति, त्रुटियों की प्रवृत्ति आदि को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। इससे शिक्षक को विद्यार्थी की सीखने की मनोवैज्ञानिक स्थिति की सही समझ मिलती है।
10. वस्तुनिष्ठ परीक्षण
निदानात्मक परीक्षाएँ निष्पक्ष (Objective) और मापन योग्य होती हैं। इनसे प्राप्त जानकारी शिक्षक को विद्यार्थियों की प्रगति का सटीक आकलन करने में सहायता करती है। इससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनती है।
निष्कर्ष
निदानात्मक परीक्षाएँ केवल मूल्यांकन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षण-सुधार का मार्गदर्शक उपकरण हैं। ये शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि विद्यार्थी कहाँ अटका है और उसे आगे बढ़ाने के लिए कौन-से उपाय सबसे उपयुक्त होंगे। इस प्रकार, निदानात्मक परीक्षाएँ शिक्षा प्रक्रिया को अधिक उपयोगी, वैज्ञानिक और परिणामोन्मुख बनाती हैं।
निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र (Scope of Diagnostic Teaching) —
निदानात्मक शिक्षण (Diagnostic Teaching) शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने से जुड़ी कठिनाइयों की पहचान कर उनका समाधान किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल यह जानना नहीं होता कि छात्र ने क्या सीखा है, बल्कि यह समझना भी होता है कि वह क्यों नहीं सीख पा रहा है और उसे कैसे सिखाया जा सकता है।
1. निदानात्मक शिक्षण का वर्तमान क्षेत्र
वर्तमान में निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग मुख्य रूप से आधारभूत विषयों में किया जाता है, जैसे —
- अंकगणित (Arithmetic)
- लेखन (Writing)
- उच्चारण (Pronunciation)
- वाचन (Reading)
इन विषयों में विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को आसानी से विश्लेषित किया जा सकता है क्योंकि इन विषयों में सीखने की त्रुटियाँ या कठिनाइयाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए —
यदि कोई छात्र गणित में बार-बार गलती करता है, तो निदानात्मक परीक्षण से यह पता लगाया जा सकता है कि गलती गणना में है या अवधारणा में।
2. आधारभूत विषयों तक सीमित रहने का कारण
शिक्षाविद् योकस (Yocum) और सिम्पसन (Simpson) के अनुसार, निदानात्मक शिक्षण का उपयोग मुख्यतः इन आधारभूत विषयों तक ही सीमित है क्योंकि —
- इन विषयों में सीखने के विशिष्ट रूपों की पहचान करना अपेक्षाकृत सरल है।
- इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा सकता है।
- ये विषय अन्य सभी विषयों के अध्ययन और ज्ञानार्जन का आधार माने जाते हैं।
अर्थात यदि विद्यार्थी इन आधारभूत क्षेत्रों में दक्ष होगा, तो वह अन्य विषयों को भी आसानी से समझ पाएगा।
3. भविष्य में विस्तार की संभावना
योकस और सिम्पसन का मानना है कि आने वाले समय में निदानात्मक शिक्षण की विधियों में व्यापक विस्तार होगा। तकनीकी प्रगति और शिक्षण विधियों में सुधार के साथ यह संभव है कि निदानात्मक शिक्षण केवल आधारभूत विषयों तक सीमित न रहे, बल्कि —
- विज्ञान,
- सामाजिक अध्ययन (Social Studies),
- भाषा अध्ययन (Language Learning),
- तथा अन्य व्यावहारिक विषयों में भी इसका प्रयोग किया जा सके।
भविष्य में यह शिक्षण-पद्धति विद्यालयों के संपूर्ण पाठ्यक्रम (Curriculum) के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को पहचानने और दूर करने का सशक्त उपकरण बन सकती है।
वर्तमान में निदानात्मक शिक्षण का क्षेत्र भले ही कुछ आधारभूत विषयों तक सीमित हो, लेकिन इसका महत्व बहुत व्यापक है। जैसे-जैसे शिक्षण की तकनीकें विकसित होंगी, निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सुधार के लिए किया जा सकेगा। इस प्रकार, यह भविष्य की व्यक्तिकेंद्रित शिक्षा (Individualized Education) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता एवं महत्त्व (Utility and Importance of Diagnostic Tests) —
निदानात्मक परीक्षण (Diagnostic Test) शिक्षा की वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों, कमजोरियों और बाधाओं का पता लगाकर उनके समाधान हेतु उपयुक्त उपाय करते हैं। इसका उद्देश्य केवल त्रुटियों की पहचान करना नहीं, बल्कि उन त्रुटियों के मूल कारणों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करना भी है। इस प्रकार, निदानात्मक परीक्षण शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, उपयोगी और परिणामोन्मुख बनाता है। इसके प्रमुख उपयोगिता और महत्त्व निम्नलिखित हैं—
1. विद्यार्थियों की सीखने की समस्याओं की पहचान
निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से शिक्षक यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी किसी विषय या अध्याय के किस भाग में कठिनाई महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, गणित में गलती जोड़-घटाव की समझ में है या सूत्रों के प्रयोग में — यह जानकारी शिक्षक को इस परीक्षण से मिलती है।
2. पिछड़े विद्यार्थियों की पहचान और सहायता
यह परीक्षण उन छात्रों को चिन्हित करने में मदद करता है जो किसी विषय में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक विशेष शिक्षण योजनाएँ या उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) तैयार कर सकते हैं, जिससे वे अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें।
3. भाषाई एवं विषयगत कमियों का विश्लेषण
निदानात्मक परीक्षण भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषयों में विद्यार्थियों की विशिष्ट कमियों — जैसे उच्चारण, लेखन शैली, व्याकरणिक त्रुटियाँ या अवधारणात्मक भ्रम — को उजागर करता है। इससे शिक्षक विद्यार्थी के अनुसार उपयुक्त अभ्यास या रणनीतियाँ अपना सकते हैं।
4. शिक्षण प्रक्रिया में सुधार
इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धतियों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि किसी विशिष्ट पद्धति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे, तो शिक्षक उसमें संशोधन कर नई तकनीकें अपना सकते हैं। इससे शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है।
5. अध्ययन प्रक्रिया में अवरोधों की पहचान
कभी-कभी सीखने में कठिनाइयाँ केवल विषयगत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक या सामाजिक भी होती हैं। निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थियों की इन आंतरिक बाधाओं को उजागर करता है, जिससे शिक्षक उनके अनुरूप व्यक्तिगत मार्गदर्शन (Individual Guidance) दे सकते हैं।
6. पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव
निदानात्मक परीक्षण यह संकेत देता है कि पाठ्यक्रम के कौन-से भाग विद्यार्थियों के लिए कठिन या अनुपयुक्त हैं। इस आधार पर पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी, स्तरानुकूल और व्यावहारिक बनाया जा सकता है।
7. पाठ्य-पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार
यदि किसी विषय की कठिनाइयाँ मुख्यतः पाठ्य-पुस्तक की जटिलता या प्रस्तुति शैली से उत्पन्न हो रही हों, तो इन परीक्षणों से मिली जानकारी के आधार पर पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। इससे विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री अधिक सुगम और प्रभावी बनती है।
8. शैक्षिक एवं व्यावसायिक दिशा-निर्देश
निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थियों की क्षमता, रुचि और कमजोरियों का वास्तविक आकलन प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर शिक्षक या परामर्शदाता विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक (Educational) और व्यावसायिक (Vocational) दिशा-निर्देश प्रदान कर सकते हैं।
9. मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार
निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त आंकड़े मूल्यांकन पद्धति में सुधार लाने में मदद करते हैं। पारंपरिक परीक्षा केवल परिणाम देती है, जबकि निदानात्मक परीक्षण प्रक्रिया-आधारित मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, जिससे शिक्षा अधिक सार्थक (Meaningful) और समग्र (Comprehensive) बनती है।
निष्कर्ष
निदानात्मक परीक्षण शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो शिक्षक को न केवल विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने में सहायता करता है, बल्कि उनके समाधान के लिए सही दिशा भी प्रदान करता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक सटीक, प्रभावी और छात्र-केंद्रित बन जाती है। इस प्रकार, निदानात्मक परीक्षण शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक सिद्ध होता है।
निदान प्रक्रिया (Diagnostic Process) —
किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक सुसंगठित एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया का होना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों का समाधान करने हेतु निदान प्रक्रिया (Diagnostic Process) अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक न केवल विद्यार्थियों की समस्याओं की पहचान करता है, बल्कि उनके मूल कारणों का विश्लेषण कर प्रभावी उपचारात्मक कदम भी उठाता है।
निदान प्रक्रिया सामान्यतः पाँच प्रमुख चरणों में पूर्ण होती है —
1. नैदानिक विद्यार्थियों का चयन (Selection of Diagnostic Students)
निदान प्रक्रिया का प्रथम चरण नैदानिक विद्यार्थियों का चयन है। इस चरण में उन विद्यार्थियों की पहचान की जाती है जो किसी विषय में पीछे रह जाते हैं, धीरे-धीरे सीखते हैं या विद्यालय के वातावरण में सामंजस्य बैठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे विद्यार्थी अक्सर कम उपलब्धि, असामान्य व्यवहार या अध्ययन में अरुचि का प्रदर्शन करते हैं। इन विद्यार्थियों की पहचान के लिए विद्यालयी परीक्षाओं के परिणाम, बुद्धि परीक्षण (Intelligence Tests), उपलब्धि परीक्षण (Achievement Tests), शिक्षक के व्यक्तिगत अनुभव, तथा साक्षात्कार और अवलोकन (Observation and Interview) जैसे विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि किन विद्यार्थियों को विशेष ध्यान, सहायता तथा निदानात्मक शिक्षण (Diagnostic Teaching) की आवश्यकता है, ताकि उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
2. विद्यार्थियों के कठिनाई स्थलों का चयन (Identification of Problem Areas)
यह निदान प्रक्रिया का द्वितीय चरण है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी को किन विषयों, टॉपिक्स या कौशलों में कठिनाई हो रही है। इस चरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी की सीखने की समस्या का वास्तविक स्रोत क्या है — चाहे वह संकल्पना की अस्पष्टता, अभ्यास की कमी, या रुचि एवं प्रेरणा की कमी ही क्यों न हो। इसके लिए शिक्षक विभिन्न उपायों का उपयोग करता है, जैसे — विद्यार्थियों से बातचीत और साक्षात्कार, उनके कार्यों एवं व्यवहार का अवलोकन, तथा बुद्धि और उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण। साथ ही, शिक्षक के अनुभव और अनौपचारिक परीक्षण (Informal Tests) भी इस चरण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से विद्यार्थी की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति और कठिनाइयों की गहराई को समझा जा सकता है।
3. कठिनाई के कारणों का विश्लेषण (Analysis of Causes of Difficulty)
यह निदान प्रक्रिया का तीसरा चरण है, जिसमें शिक्षक विद्यार्थी की कठिनाइयों के मूल कारणों को समझने और उनका विश्लेषण करने का प्रयास करता है। केवल कठिनाई की पहचान करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह जानना आवश्यक है कि वह कठिनाई क्यों उत्पन्न हुई है। इसके लिए शिक्षक विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है, जैसे — विद्यार्थियों से व्यक्तिगत वार्तालाप, अभिभावकों और अन्य शिक्षकों से चर्चा, तथा व्यवहारिक और भावनात्मक पहलुओं का गहन अध्ययन। विद्यार्थियों की कठिनाइयों के संभावित कारणों में शारीरिक दोष (जैसे दृष्टि या श्रवण संबंधी समस्या), मानसिक या संवेगात्मक अस्थिरता, अध्ययन के प्रति अरुचि या गलत अध्ययन आदतें, तथा पारिवारिक या विद्यालयी वातावरण का दबाव प्रमुख हैं। इन कारणों की सटीक पहचान से शिक्षक को यह तय करने में सहायता मिलती है कि आगे कौन-से उपचारात्मक या सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ, ताकि विद्यार्थी की सीखने की समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सके।
4. उपचारात्मक प्रक्रिया (Remedial Process)
यह निदान प्रक्रिया का चतुर्थ और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसे सम्पूर्ण प्रक्रिया का मुख्य भाग माना जाता है। इस चरण में विद्यार्थी की कठिनाइयों की पहचान हो जाने के बाद उन्हें दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित उपचारात्मक शिक्षण योजना (Remedial Plan) तैयार की जाती है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमता और सीखने की गति के अनुरूप सहायता मिल सके। उपचारात्मक योजना में आमतौर पर निम्न उपाय शामिल होते हैं —
- विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने के लिए विशेष अभ्यास
- व्यक्तिगत या सामूहिक शिक्षण सत्र
- अतिरिक्त समय या विशेष निर्देशों की व्यवस्था
- शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्रियों में आवश्यक परिवर्तन
इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी अपनी पिछली गलतियों को सुधार सके, आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करे और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके। इस प्रकार, उपचारात्मक प्रक्रिया विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होती है।
5. रोकथाम के उपाय (Preventive Measures)
यह निदान प्रक्रिया का पंचम और अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य भविष्य में सीखने से संबंधित कठिनाइयों की पुनरावृत्ति को रोकना है। इस चरण में शिक्षक, विद्यालय और अभिभावक मिलकर विद्यार्थियों के लिए एक अनुकूल, सहयोगी और प्रेरक शिक्षण वातावरण तैयार करते हैं, ताकि वे आगे किसी प्रकार की अधिगम समस्या का सामना न करें। इसके अंतर्गत कई निवारक कदम उठाए जाते हैं, जैसे —
- विद्यालय और घर के वातावरण में सुधार, ताकि विद्यार्थी मानसिक रूप से सुरक्षित और सहज महसूस करे।
- पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में आवश्यक संशोधन, जिससे सीखना अधिक व्यावहारिक और रुचिकर बन सके।
- शिक्षण विधियों में नवीनता, ताकि हर विद्यार्थी की सीखने की शैली के अनुरूप शिक्षण प्रदान किया जा सके।
- विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के उपाय, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा बनी रहे।
इन सभी रोकथामात्मक उपायों का परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी न केवल अपनी वर्तमान कठिनाइयों से उबरते हैं, बल्कि भविष्य में भी किसी प्रकार की सीखने की समस्या से बचने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार, रोकथाम के उपाय निदान प्रक्रिया को पूर्णता और स्थायित्व प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष
निदान प्रक्रिया एक वैज्ञानिक, चरणबद्ध और छात्र-केंद्रित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य केवल त्रुटियों की पहचान करना नहीं, बल्कि उनका स्थायी समाधान खोजना है। यह प्रक्रिया शिक्षक को न केवल प्रभावी शिक्षण में सहायता करती है, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है।
इस प्रकार, निदान प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता की ओर अग्रसर करने का एक सशक्त माध्यम है।
निदानात्मक परीक्षण का निर्माण (Construction of Diagnostic Test)
निदानात्मक परीक्षण (Diagnostic Test) का निर्माण एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनके समाधान हेतु उचित उपचारात्मक उपाय निर्धारित करना होता है। यह परीक्षण न केवल विद्यार्थियों की ज्ञान की स्थिति का मूल्यांकन करता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे कहाँ और क्यों पिछड़ रहे हैं।
निदानात्मक परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जाती है —
1. उद्देश्य का निर्धारण (Determination of Objective)
सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षण का उद्देश्य क्या है —
क्या यह किसी विशेष विषय (जैसे गणित, हिंदी या विज्ञान) में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचानने के लिए बनाया जा रहा है या किसी विशिष्ट कौशल (जैसे पठन, लेखन या गणना) का मूल्यांकन करने के लिए। उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, परीक्षण उतना ही सटीक बनेगा।
2. विषय-वस्तु का चयन (Selection of Content)
इस चरण में उस विषय या इकाई की रूपरेखा तैयार की जाती है जिसके लिए परीक्षण बनाना है। उदाहरण के लिए, गणित विषय में ‘भाग’, ‘भिन्न’, या ‘मापन’ जैसी इकाइयों में विद्यार्थियों की समझ का परीक्षण किया जा सकता है। विषय-वस्तु का चयन पाठ्यक्रम और शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।
3. अधिगम उद्देश्यों का विश्लेषण (Analysis of Learning Objectives)
यहाँ प्रत्येक इकाई के अधिगम उद्देश्यों को उप-उद्देश्यों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, “भिन्न की समझ” में उप-उद्देश्य होंगे —
- भिन्नों की पहचान करना,
- समान भिन्न बनाना,
- भिन्नों का जोड़ व घटाना।
इन उप-उद्देश्यों के आधार पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि विद्यार्थी किस स्तर पर कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।
4. प्रश्नों का निर्माण (Preparation of Test Items)
यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। प्रत्येक उप-उद्देश्य के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं जैसे —
- वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)
- लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type)
- सत्य-असत्य (True/False)
- रिक्त स्थान भरें (Fill in the blanks)
- मिलान करें (Match the following)
प्रश्न सरल से कठिन क्रम में होने चाहिए ताकि विद्यार्थी की अधिगम यात्रा का क्रमिक मूल्यांकन किया जा सके।
5. परीक्षण की प्रारूप योजना (Preparation of Test Blueprint)
ब्लूप्रिंट में यह निर्धारित किया जाता है कि कौन-से अध्याय से कितने प्रश्न होंगे, उनका भारांक कितना होगा और वे किस प्रकार के होंगे। यह परीक्षण को संतुलित और व्यवस्थित बनाता है।
6. परीक्षण का प्रारूपण एवं परीक्षण (Try Out of the Test)
तैयार प्रश्न-पत्र को पहले सीमित संख्या में विद्यार्थियों पर लागू किया जाता है ताकि उसकी उपयोगिता, विश्वसनीयता (Reliability) और वैधता (Validity) की जांच की जा सके। यदि किसी प्रश्न में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है तो उसे संशोधित किया जाता है।
7. अंकन योजना एवं विश्लेषण (Scoring and Interpretation)
प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित किए जाते हैं। विद्यार्थियों के उत्तरों का मूल्यांकन करके उनकी गलतियों का विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता चले कि कठिनाई का स्तर कहाँ है — ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या विश्लेषण स्तर पर।
8. उपचारात्मक सुझाव (Remedial Suggestions)
अंत में, निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपचारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। जैसे —
- कमजोर विद्यार्थियों के लिए पुनःशिक्षण (Re-teaching),
- अतिरिक्त अभ्यास,
- व्यक्तिगत मार्गदर्शन,
- समूह चर्चा, आदि।
निष्कर्ष (Conclusion)
निदानात्मक परीक्षण का निर्माण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की कमजोरियों और अधिगम कठिनाइयों की सटीक पहचान करने में मदद करता है। इससे न केवल शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होता है, बल्कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत प्रगति भी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार, यह परीक्षण शिक्षण को अधिक प्रभावी, लक्ष्य-उन्मुख और विद्यार्थी-केंद्रित बनाता है।
निदानात्मक परीक्षण के प्रकार (Types of Diagnostic Tests)
निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनके समाधान के लिए बनाए जाते हैं। यह परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जो अध्यापक को यह समझने में सहायता करते हैं कि छात्र किस बिंदु पर कठिनाई अनुभव कर रहा है और उसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएँ। इन परीक्षणों को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है —
1. विषय के आधार पर (On the Basis of Subject Matter)
निदानात्मक परीक्षणों का सबसे सामान्य वर्गीकरण विषय-वस्तु के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक विषय की प्रकृति अलग होती है, इसलिए कठिनाइयाँ भी भिन्न होती हैं।
मुख्य प्रकार:
- (क) भाषा विषय के निदानात्मक परीक्षण:
भाषा सीखने में विद्यार्थियों को पठन, लेखन, व्याकरण, उच्चारण और शब्दार्थ संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। इन कठिनाइयों की पहचान करने के लिए भाषा विषय के निदानात्मक परीक्षण बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, गलत वाक्य संरचना, वर्तनी दोष या वाक्य रचना की समस्या का पता लगाने के लिए विशेष प्रकार के परीक्षण उपयोग किए जाते हैं। - (ख) गणित के निदानात्मक परीक्षण:
गणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, मापन, अनुपात, प्रतिशत आदि के विषयों में विद्यार्थियों को अक्सर कठिनाई होती है। ऐसे परीक्षण विद्यार्थियों की गणना संबंधी त्रुटियों और अवधारणात्मक कमियों की पहचान करते हैं। - (ग) विज्ञान के निदानात्मक परीक्षण:
विज्ञान विषय में अवधारणात्मक समझ, प्रयोगात्मक कौशल और कारण-परिणाम की पहचान के लिए निदानात्मक परीक्षण उपयोग किए जाते हैं। इससे यह जाना जा सकता है कि विद्यार्थी सिद्धांतों को समझ पा रहा है या नहीं।
2. उद्देश्य के आधार पर (On the Basis of Objective)
निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों के स्तर को पहचानना होता है।
मुख्य प्रकार:
- (क) ज्ञान आधारित परीक्षण (Knowledge-based Test):
यह परीक्षण विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और बुनियादी तथ्यों की समझ की जाँच करते हैं। उदाहरण के लिए, गणित में सूत्रों की पहचान या भाषा में व्याकरण के नियमों का ज्ञान। - (ख) समझ आधारित परीक्षण (Comprehension-based Test):
ये परीक्षण विद्यार्थियों की विषय की गहराई से समझने की क्षमता को मापते हैं। उदाहरण के लिए, कहानी के भावार्थ या वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग की समझ। - (ग) अनुप्रयोग आधारित परीक्षण (Application-based Test):
इस प्रकार के परीक्षण यह जाँचते हैं कि विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर सकता है या नहीं, जैसे गणितीय सूत्रों का प्रयोग वास्तविक समस्याओं में करना।
3. स्वरूप के आधार पर (On the Basis of Form of Test)
निदानात्मक परीक्षण प्रश्नों के स्वरूप के अनुसार भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं।
मुख्य प्रकार:
- (क) वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type):
इन परीक्षणों में बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य/असत्य, रिक्त स्थान भरना, मिलान करना आदि प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह समय की बचत करते हैं और मूल्यांकन में निष्पक्षता लाते हैं। - (ख) लघु उत्तरीय प्रकार (Short Answer Type):
इनमें छोटे उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जिनसे विद्यार्थियों की समझ का त्वरित मूल्यांकन किया जा सकता है। - (ग) निबंधात्मक प्रकार (Essay Type):
इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थी को विस्तारपूर्वक उत्तर देना होता है, जिससे उसकी तर्क शक्ति, विचार क्षमता और रचनात्मकता का पता चलता है।
4. उपयोग के आधार पर (On the Basis of Use)
शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में निदानात्मक परीक्षणों का उपयोग अलग-अलग उद्देश्य से किया जाता है।
मुख्य प्रकार:
- (क) प्रवेश निदानात्मक परीक्षण (Entry Diagnostic Test):
शिक्षण प्रारंभ होने से पहले विद्यार्थियों की पूर्वज्ञान स्थिति और तैयारी के स्तर को जानने के लिए यह परीक्षण किए जाते हैं। इससे शिक्षक को शिक्षण की दिशा तय करने में सहायता मिलती है। - (ख) मध्यावधि निदानात्मक परीक्षण (Mid-term Diagnostic Test):
शिक्षण के दौरान यह परीक्षण विद्यार्थियों की प्रगति और कठिनाइयों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं ताकि समय रहते सुधार किया जा सके। - (ग) अंतिम निदानात्मक परीक्षण (Terminal Diagnostic Test):
शिक्षण के अंत में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है और शेष कठिनाइयों का पता लगाकर उपचारात्मक सुझाव दिए जाते हैं।
5. व्यक्तिगत एवं समूह आधारित (Individual and Group Diagnostic Tests)
- (क) व्यक्तिगत निदानात्मक परीक्षण:
यह परीक्षण किसी एक विद्यार्थी की विशेष कठिनाइयों की पहचान करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः तब किया जाता है जब विद्यार्थी किसी विशेष विषय में अत्यधिक पिछड़ा हो। - (ख) समूह निदानात्मक परीक्षण:
इनका उद्देश्य किसी पूरी कक्षा या समूह की सामान्य कठिनाइयों का पता लगाना होता है ताकि शिक्षक सामूहिक रूप से सुधारात्मक उपाय कर सके।
निष्कर्ष (Conclusion)
निदानात्मक परीक्षण शिक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य उपकरण हैं। इनके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए उचित शिक्षण रणनीति तैयार कर सकता है। निदानात्मक परीक्षण केवल मूल्यांकन का साधन नहीं हैं, बल्कि यह शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने, विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने और उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुँचाने का माध्यम भी हैं। इस प्रकार, इन परीक्षणों के विविध प्रकार शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली, वैज्ञानिक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाते हैं।
Very Important notes for B.ed.: बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव(balak par vatavaran ka prabhav) II sarva shiksha abhiyan (सर्वशिक्षा अभियान) school chale hum abhiyan II शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक II जेंडर शिक्षा में संस्कृति की भूमिका (gender shiksha mein sanskriti ki bhumika) II मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, maslow hierarchy of needs theory in hindi II थार्नडाइक के अधिगम के नियम(thorndike lows of learning in hindi) II थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत(thorndike theory of learning in hindi ) II पावलव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत (pavlov theory of classical conditioning in hindi) II स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत skinner operant conditioning theory in hindi