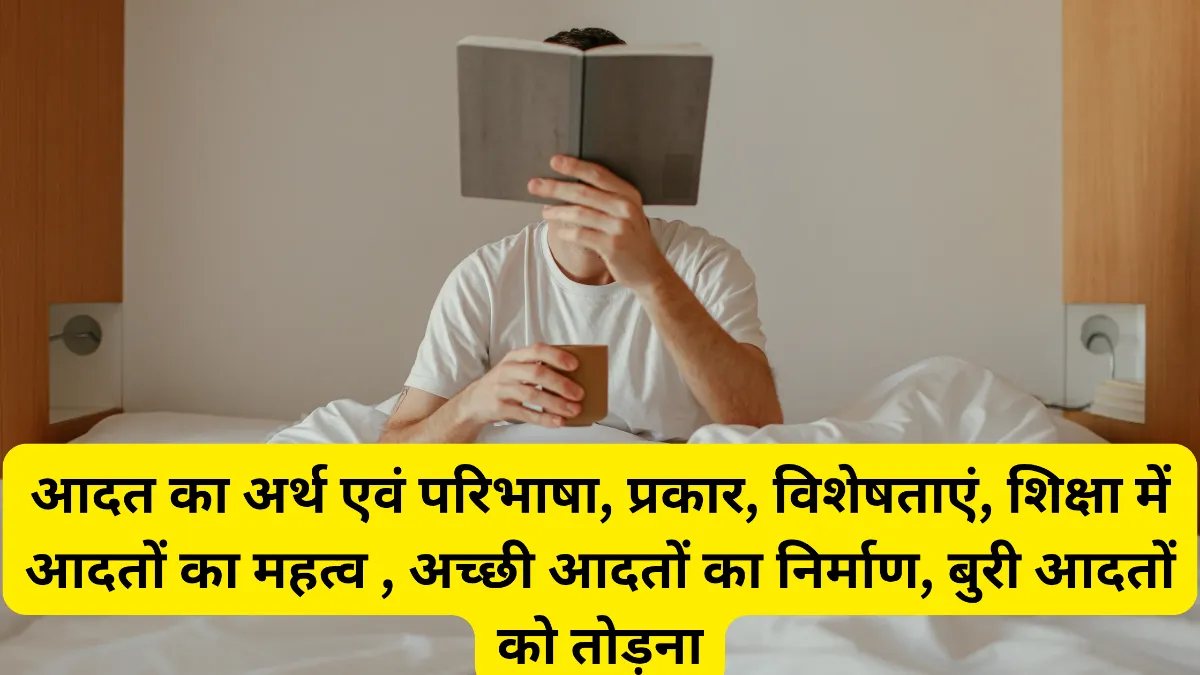आदत का अर्थ और परिभाषा, प्रकार, विशेषताएँ और शिक्षा में आदतों का महत्व। जानें अच्छी आदतें कैसे विकसित करें और बुरी आदतों को तोड़ने के प्रभावी तरीके।
आदत का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Habit)
आदत सामान्यतः उस क्रिया या व्यवहार को कहते हैं, जिसे व्यक्ति बार-बार करता है और जिसे करने का वह आदी हो जाता है। उदाहरण के लिए— चाय पीने की आदत, गुटका खाने की आदत आदि।
मनोविज्ञान की दृष्टि से आदत को सीखे हुए व्यवहार (Learned Behaviour) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बार-बार दोहराए जाने पर स्वचालित (Automatic) हो जाता है।
उदाहरण:
- प्रारंभ में जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हैंडल को संतुलित किया जाए और कैसे पैडल चलाएं।
- बार-बार अभ्यास करने के बाद वह बिना सोच-समझे साइकिल चला सकता है। हैंडल अपने आप घूमने लगता है और पैडलिंग सहज हो जाती है।
- इस स्थिति में कहा जा सकता है कि साइकिल चलाना उसकी आदत बन गई है।
इसी प्रकार— समय पर उठना, सही ढंग से खाना-पीना, बैठने-उठने की आदतें, सही ढंग से बोलना और चलना—ये सभी आदतें प्रारंभ में सीखी जाती हैं, लेकिन बार-बार दोहराने पर यह स्वचालित हो जाती हैं और व्यक्ति के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती।
आदत की परिभाषा
गैरेट (Garrett) के अनुसार—
“आदत उस व्यवहार का नाम है जो बार-बार दोहराए जाने के कारण स्वचालित रूप में होने लगता है।”
लैडेल (Laddell) के अनुसार—
“आदत कार्य का वह रूप है जो प्रारंभ में अपनी इच्छा से जान-बूझकर किया जाता है, परंतु बार-बार किए जाने के कारण वह स्वचालित हो जाता है।”
मरसेल के अनुसार –
“आदतें, व्यवहार करने की और परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियाँ होती हैं।”
मार्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार –
“व्यवहार द्वारा अर्जित समस्त परिवर्तन जो अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं आदत कहलाते हैं।”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आदत केवल बार-बार किए जाने वाले क्रियाओं का परिणाम होती है, जो व्यक्ति की स्वाभाविक सक्रियता और मानसिक संगठन का हिस्सा बन जाती है।
बिल्कुल! मैं आपके दिए हुए प्रारूप को और अधिक विस्तार, स्पष्टता और व्यवस्थित ढंग में बढ़ाकर प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आदतों के विशेषताएँ और शिक्षा में उनके महत्व भी जोड़ दूँगा। आप इसे इस तरह पेश कर सकते हैं:
आदतों के प्रकार (Kinds of Habits) –
मनुष्य के जीवन में आदतों का अत्यधिक महत्व है। आदतें न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचरण और व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बल्कि उसके सामाजिक जीवन और निर्णय लेने की क्षमता को भी आकार देती हैं। यही कारण है कि शिक्षा और व्यक्तित्व विकास में आदतों का अध्ययन आवश्यक माना गया है।
आमतौर पर आदतों को दो मुख्य वर्गों में बाँटा जाता है:
- अच्छी आदतें (Good Habits) – जो व्यक्ति के जीवन और समाज के लिए लाभकारी होती हैं।
उदाहरण: समय पर उठना, स्वच्छता रखना, दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना, संयमित रहना आदि। - बुरी आदतें (Bad Habits) – जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज में उसकी छवि को प्रभावित करती हैं।
उदाहरण: आलस्य करना, झूठ बोलना, गाली देना, चोरी करना, नशा करना आदि।
लेकिन मनोविज्ञान ने आदतों का विश्लेषण और भी गहराई से किया है। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग ढंग अपनाया।
1. बरनार्ड (Bernard) का वर्गीकरण
बरनार्ड ने आदतों को तीन प्रमुख प्रकारों में बाँटा है:
- शारीरिक आदतें (Physical Habits) – ये आदतें शरीर और उसके कार्यों से संबंधित होती हैं।
उदाहरण: नियमित व्यायाम, स्वच्छता बनाए रखना, सही आहार लेना। - मानसिक आदतें (Mental Habits) – ये आदतें व्यक्ति की सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।
उदाहरण: लगातार अध्ययन करना, ध्यान केंद्रित करना, तार्किक सोच अपनाना। - संवेगात्मक आदतें (Emotional Habits) – ये आदतें व्यक्ति की भावनाओं और उनकी अभिव्यक्ति से जुड़ी होती हैं।
उदाहरण: क्रोध को नियंत्रित करना, दूसरों की सहायता में उत्सुकता, सहानुभूति दिखाना।
2. वैलेंटाइन (Valentine) का विस्तृत वर्गीकरण
वैलेंटाइन ने आदतों को सात वर्गों में विभाजित किया है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं:
(1) यांत्रिक आदतें (Mechanical Habits)
यांत्रिक आदतें (Mechanical Habits) शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी आदतें होती हैं, जिन्हें व्यक्ति बार-बार अभ्यास करने से शरीर स्वचालित रूप से कर लेता है। ये आदतें सामान्यतः शारीरिक कौशल और मांसपेशियों के सही समन्वय पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना और लिखना ऐसी यांत्रिक आदतें हैं, जिन्हें लगातार अभ्यास से व्यक्ति बिना सोच-विचार के सहजता से कर सकता है।
(2) शारीरिक इच्छा से संबंधित आदतें (Habits of Physiological Desire)
शारीरिक इच्छा से संबंधित आदतें (Habits of Physiological Desire) उन आदतों को कहते हैं जो शारीरिक इच्छाओं या प्राकृतिक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती हैं और नियमित अभ्यास से स्थायी रूप ले लेती हैं। ये आदतें आमतौर पर व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवनशैली और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, चाय पीना, धूम्रपान करना, और भोजन के विशेष तरीके अपनाना ऐसी आदतों में शामिल हैं, जिन्हें व्यक्ति बार-बार करने से सहजता से निभाने लगता है।
(3) नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें (Nervous Habits)
नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें (Nervous Habits) वे आदतें होती हैं जो नाड़ी या तंत्रिका प्रणाली से जुड़ी होती हैं और आमतौर पर तनाव, चिंता या भावनात्मक असंतुलन के कारण विकसित होती हैं। ये आदतें व्यक्ति के मानसिक या भावनात्मक स्थिति का संकेत देती हैं और अक्सर अनियंत्रित रूप से दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, बार-बार आँखें झपकाना, नाखून चबाना, और पैर हिलाना ऐसी नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें हैं।
(4) भाषा संबंधी आदतें (Habits of Speech)
भाषा संबंधी आदतें (Habits of Speech) वे आदतें होती हैं जो व्यक्ति के बोलने की शैली से संबंधित होती हैं और समय के साथ नियमित अभ्यास या प्रवृत्ति से स्थायी हो जाती हैं। ये आदतें किसी व्यक्ति के संवाद कौशल, स्वर, और उच्चारण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, तेज़ बोलना, ठहर-ठहरकर बोलना, और उच्च स्वर में बोलना ऐसी भाषा संबंधी आदतों में शामिल हैं।
(5) विचार संबंधी आदतें (Habits of Thought)
विचार संबंधी आदतें (Habits of Thought) वे आदतें होती हैं जो सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं और व्यक्ति के मानसिक विकास तथा ज्ञानार्जन को प्रभावित करती हैं। ये आदतें व्यक्ति की तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता, और दृष्टिकोण को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, हर बात पर तर्क करना, समस्या को गहराई से समझना, और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ऐसी विचार संबंधी आदतों में शामिल हैं।
(6) भावना संबंधी आदतें (Habits of Feeling)
भावना संबंधी आदतें (Habits of Feeling) वे आदतें होती हैं जो व्यक्ति की भावनाओं और उन्हें व्यक्त करने की शैली से जुड़ी होती हैं। ये आदतें व्यक्ति के सहानुभूति, करुणा और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, दूसरों की मदद करना, सहानुभूति रखना, और परोपकार करना ऐसी भावना संबंधी आदतों में शामिल हैं।
(7) नैतिक आदतें (Moral Habits)
नैतिक आदतें (Moral Habits) वे आदतें होती हैं जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं और व्यक्ति के चरित्र को सशक्त और सम्माननीय बनाती हैं। ये आदतें व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय और सामाजिक संबंधों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, सत्य बोलना, ईमानदारी, अनुशासन का पालन, और बड़ों का सम्मान करना ऐसी नैतिक आदतों में शामिल हैं।
इस प्रकार, आदतें केवल शारीरिक क्रियाएँ नहीं हैं, बल्कि ये व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, नैतिक मूल्यों, मानसिक क्षमताओं और सामाजिक व्यवहार का निर्माण करती हैं। आदतों का सही चयन और नियमित अभ्यास जीवन को सफल और संतुलित बनाता है।
आदत की विशेषताएं (Characteristics of Habits)
मनुष्य का जीवन उसकी आदतों से निर्मित होता है। व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्तित्व, कार्यशैली और चरित्र उसकी आदतों के अनुरूप ही विकसित होता है। आदतें सामान्यतः अभ्यास और वातावरण के प्रभाव से निर्मित होती हैं। एक बार जब कोई आदत बन जाती है तो वह स्वचालित रूप से कार्य करती है और स्थायी रूप धारण कर लेती है। इन्हें बदलना या छुड़ाना प्रायः कठिन होता है। यही आदतों की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
(1) पर्यावरण की देन (Environment Product)
पर्यावरण की देन (Environment Product) आदतों के निर्माण में पर्यावरण की भूमिका वंशानुक्रम से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक अपने चारों ओर के लोगों का अनुकरण करता है। वह घर, विद्यालय और समाज में दूसरों के उठने-बैठने, चलने-फिरने, बोलने-चालने और व्यवहार करने की शैली को देखकर सीखता है। लगातार अनुकरण और अभ्यास करने से वही कार्य उसकी आदत का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, सच बोलना, ईमानदारी और सहायता करना जैसी अच्छी आदतें तथा बीड़ी-सिगरेट पीना और गुटखा खाना जैसी बुरी आदतें पर्यावरण से सीखी जाती हैं।
(2) स्वचालित (Automatic)
स्वचालित (Automatic) आदतों की विशेषता यह होती है कि एक बार बनने के बाद व्यक्ति को उन्हें करने के लिए अधिक विचार या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी कोई संबंधित परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो वह आदत स्वयं ही स्वचालित रूप से क्रियान्वित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को रोज़ सुबह व्यायाम करने की आदत है, तो वह बिना सोचे-समझे जागने के बाद सीधे व्यायाम करना शुरू कर देता है।
(3) कम थकान (Less Fatigue)
कम थकान (Less Fatigue) आदतों का एक प्रमुख लाभ यह है कि ये व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने में दक्ष और सहज बना देती हैं। जिस कार्य की आदत पड़ जाती है, उसे करते समय व्यक्ति को कम थकान और कम मानसिक प्रयास लगते हैं, क्योंकि वह कार्य स्वाभाविक रूप से संपन्न होने लगता है। उदाहरण के लिए, जो विद्यार्थी रोज़ लेखन का अभ्यास करता है, उसे परीक्षा में लिखते समय जल्दी थकान महसूस नहीं होती।
(4) एकरूपता (Uniformity)
एकरूपता (Uniformity) आदतों का यह गुण व्यक्ति के कार्यों और व्यवहार में समानता तथा स्थिरता बनाए रखता है। आदतन कार्य बार-बार एक ही ढंग से नियमित रूप से किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और निरंतरता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, समय पर उठना, रोज़ाना पढ़ाई करना, और हर बार नम्रता से बोलना आदतों से उत्पन्न एकरूपता के उदाहरण हैं।
(5) स्थायित्व (Stability)
स्थायित्व (Stability) आदतों का यह गुण है कि एक बार आदत पड़ जाने पर वह लंबे समय तक स्थायी बनी रहती है और आसानी से समाप्त नहीं होती। विशेषकर बुरी आदतों को छोड़ना काफी कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रयासों और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, धूम्रपान, गुटखा खाना और देर रात तक जागना ऐसी आदतें हैं जिन्हें छोड़ना आसान नहीं होता।
(6) चरित्र के अंग (Parts of Character)
चरित्र के अंग (Parts of Character) आदतें व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का आईना होती हैं। जिन व्यक्तियों की आदतें समाज-सम्मत और नैतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं, वे समाज में चरित्रवान कहे जाते हैं, जबकि समाज-विरोधी और अनैतिक आदतों वाले लोग चरित्रहीन समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए, अनुशासन, ईमानदारी और सत्यवादिता जैसी आदतें चरित्र को ऊँचा उठाती हैं, वहीं झूठ, चोरी और नशाखोरी जैसी आदतें चरित्र को गिरा देती हैं।
आदतें व्यक्ति के जीवन की आधारशिला हैं। ये न केवल उसके व्यवहार और कार्यशैली को प्रभावित करती हैं, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण करती हैं। इसलिए कहा जाता है—
“मनुष्य जैसा सोचता और करता है, वैसा ही बन जाता है, और यह सब उसकी आदतों का ही परिणाम होता है।”
आदतों का शिक्षा में महत्व, शिक्षा में आदतों का महत्व
(Importance of Habits in Education and Learning)
रायबर्न का कथन है—
“सीखना, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है।”
“Learning is the process of building up habits.” – Ryburn
यह कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि शिक्षा और अधिगम (Learning) का मूल आधार आदतों का निर्माण है। जब कोई ज्ञान, कौशल या व्यवहार निरंतर अभ्यास से व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाता है, तब वही उसकी आदत कहलाता है। आदतें न केवल अधिगम को सहज बनाती हैं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, चरित्र और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं।
शिक्षा और अधिगम में आदतों की उपयोगिता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है—
1. शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में सहयोग
अच्छी आदतें बालक के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। शारीरिक स्तर पर व्यायाम, स्वच्छता और समय पर भोजन जैसी आदतें स्वास्थ्य को सुदृढ़ और ऊर्जावान बनाती हैं। मानसिक स्तर पर अध्ययन, एकाग्रता और आत्म-अनुशासन की आदतें ज्ञानार्जन और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। वहीं संवेगात्मक स्तर पर सहयोग, सहानुभूति और परोपकार की आदतें बालक को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाती हैं और उसे एक सजग, संवेदनशील तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी नागरिक बनने में मदद करती हैं।
2. चरित्र निर्माण में योगदान
चरित्र निर्माण का आधार आदतें ही होती हैं। मनुष्य का स्वभाव और व्यक्तित्व उसकी आदतों से निर्मित होता है। यही आदतें उसे कर्मठ या अकर्मण्य, उदार या स्वार्थी, तथा दयालु या कठोर बनाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि—
“चरित्र आदतों का पुंज है।”
“Character is a bundle of habits.”
3. व्यक्तित्व निर्माण में सहायक
व्यक्तित्व का निर्माण केवल बाहरी रूप-रंग से नहीं, बल्कि आदतों से होता है। क्लेपर ने सही कहा है—
“आदतें व्यक्तित्व की आवरण हैं।”
“Personality is clothed in habits.” – Klapper (Quoted by Bhatia
यदि बालक में अनुशासन, समयनिष्ठा और ईमानदारी जैसी आदतें विकसित हैं, तो उसका व्यक्तित्व आकर्षक, प्रभावशाली और समाज में सम्मानजनक बन जाता है।
4. स्वभाव का अंग बन जाना
आदतें समय के साथ बालक के स्वभाव का अभिन्न अंग बन जाती हैं। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का विचार है—
“आदत दूसरा स्वभाव है। आदत, स्वभाव से दस गुना अधिक शक्तिशाली है।”
“Habit is second nature. Habit is ten times nature.” – Duke of Wellington (Quoted by James, p. 142)
यह स्पष्ट करता है कि आदतें मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
5. आचरण को नियंत्रित करना
अच्छी आदतें बालक को नैतिक सीमाओं के भीतर बनाए रखती हैं। इनके प्रभाव से वह अनैतिक, असामाजिक और अधार्मिक कार्यों से बचता है और अनुशासन तथा नैतिकता का पालन करने की प्रवृत्ति उसके भीतर स्वतः विकसित हो जाती है।
6. कठिन कार्यों को सरल बनाना
आदतें बालक में कठिन कार्यों को भी करने की शक्ति उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाता है, जैसे—अंधेरी खानों में मजदूरी करना, हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहना, या खतरनाक वातावरण में कार्य करना।
7. समाज में अनुकूलन (Social Adjustment)
आदतें व्यक्ति को समाज में अनुकूलन करने और समाज-विरोधी गतिविधियों से बचने में सहायक होती हैं। जेम्स का यह कथन अत्यंत सार्थक है—
“आदत, समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है।”
“Habit is the enormous fly-wheel of society, its most precious conservative agent.” – James
यह दर्शाता है कि आदतें समाज की स्थिरता और व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
8. थकान का अभाव
जब कोई कार्य आदत बन जाता है, तो उसे करने में थकान महसूस नहीं होती। उदाहरण के रूप में, यदि विद्यार्थी नियमित अभ्यास से पढ़ाई की आदत डाल लेता है, तो परीक्षा के समय उसे अतिरिक्त बोझ या तनाव का अनुभव नहीं होगा और वह सहजता से अपने कार्य को पूरा कर पाएगा।
9. स्मरण की सरलता
जो बातें बालक की आदत बन जाती हैं, उन्हें याद रखने में उसे कठिनाई नहीं होती। उदाहरण के लिए, गणित की सारणियाँ, प्रार्थना, श्लोक, या भाषा के शब्द यदि नियमित अभ्यास और आदत के रूप में सीखे जाएँ, तो बालक उन्हें सहजता और स्थायित्व के साथ याद रख सकता है।
10. कार्यकुशलता और समय की बचत
आदतें कार्य को शीघ्रता, कुशलता और सरलता से करने में सहायक होती हैं। रायबर्न का कथन इस बात को स्पष्ट करता है—
“आदत हममें जीवन के अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए समय और मानसिक शक्ति की बचत करने की क्षमता उत्पन्न करती है।”
“Habit enables us to save time and mental energy for more important tasks of life.” – Ryburn
इससे यह समझा जा सकता है कि आदतें व्यक्ति को संगठित, प्रभावी और उत्पादक बनाती हैं।
यद्यपि आदतें शिक्षा और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तथापि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ विद्वानों ने इसकी सीमाओं को भी रेखांकित किया है।
- मरसेल के अनुसार—
“आदत का निर्माण केवल संतोष का चिन्ह है और जब आदतों का निर्माण हो जाता है, तब अधिगम और उन्नति का कार्य अवरुद्ध हो जाता है।”
“The formation of habit is a symptom of satisfaction and when habits form, learning and improvement stop.” – Mursell
इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल आदतों का निर्माण करना नहीं, बल्कि रचनात्मकता, विवेकपूर्ण सोच और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करना भी होना चाहिए।
निष्कर्ष (Conclusion)
आदतें शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया का मूल आधार हैं। वे न केवल व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन को आकार देती हैं, बल्कि अधिगम को सरल, प्रभावी और स्थायी बनाती हैं। तथापि, शिक्षा का उद्देश्य केवल आदतों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, चिंतनशीलता और नवाचार की प्रवृत्ति भी विकसित करनी चाहिए।
छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण
आदतें हमारे जीवन में कार्यों को सरल, कुशल और नियमित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी नई आदत को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए कुछ नियम, उपाय और सिद्धान्त अपनाना आवश्यक है। प्रमुख दृष्टव्य निम्नलिखित हैं:
- संकल्प (Resolution)
आदत डालने के लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्प आवश्यक है। जिस कार्य को हम नियमित करना चाहते हैं, उसके प्रति हमें निश्चय करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि हम प्रातःकाल व्यायाम की आदत डालना चाहते हैं, तो यह प्रतिज्ञा करें कि चाहे कुछ भी हो, हम रोज़ व्यायाम करेंगे। जेम्स का कथन है-
“हमें नये कार्य को अधिक-से-अधिक सम्भव दृढ़ता और निश्चय से आरम्भ करना चाहिए।” (James, p. 145) - क्रियाशीलता (Activity)
केवल संकल्प पर्याप्त नहीं है, उसे कार्य-रूप में परिणत करना आवश्यक है। नए कार्य को तुरंत शुरू करना चाहिए और अवसर मिलने पर उसे तुरंत पूरा करना चाहिए। जेम्स कहते हैं-
“जो संकल्प आप करें, उसे पहले अवसर पर ही पूर्ण कीजिए।”
(Seize the very first opportunity to act on every resolution you make – James, p. 147) - निरन्तरता (Continuity)
आदत डालने के लिए उसे लगातार करना आवश्यक है। इसमें कोई विराम या शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जेम्स के अनुसार-
“जब तक नई आदत आपके जीवन में पूर्ण रूप से स्थायी न हो जाये, तब तक उसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं होने देना चाहिए।” (James, p. 145) - अभ्यास (Exercise)
किसी कार्य को नियमित करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास आवश्यक है। रोज़ाना थोड़े समय के लिए भी अभ्यास करना आदत को मजबूत बनाता है। जेम्स का मत है-
“प्रतिदिन थोड़े से ऐच्छिक अभ्यास द्वारा कार्य करने की शक्ति को जीवित रखिए।” (James, p. 149)
इसे सरल भाषा में कहा जाए तो—“करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान।” - अच्छे उदाहरण (Good Examples)
आदतों के निर्माण में अच्छे उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक या अभिभावक को बालकों को केवल उपदेश देने की बजाय स्वयं अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। जेम्स का परामर्श है-
“अपने छात्रों को बहुत अधिक उपदेश मत दीजिए।”
(Don’t preach too much to your pupils – James, Quoted by Jha, p. 393) - पुरस्कार (Reward)
अच्छी आदतें विकसित करने में पुरस्कार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को सही आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए पुरस्कार देना लाभकारी होता है। भाटिया के अनुसार-
“बालकों को अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए।” (Bhatia, p. 234)
इस प्रकार, संकल्प, क्रियाशीलता, निरन्तरता, अभ्यास, अच्छे उदाहरण और पुरस्कार—इन छह सिद्धान्तों का पालन करके किसी भी छात्र में अच्छी आदतें विकसित की जा सकती हैं।
बुरी आदतों को तोड़ना, छात्रों से बुरी आदतों को छुड़ाना (Break Bad Habits), बुरी आदतों को कैसे छोड़े
व्यक्ति कभी-कभी समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को भी आदत में बदल लेता है। ये बुरी आदतें न केवल उसके स्वयं के जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक होती हैं। इसलिए इन आदतों को तोड़ना आवश्यक है।
स्टर्ट और ओकडन का कथन है:
“शिक्षक का कार्य न केवल आदतों का निर्माण करना है, वरन् उसको तोड़ना भी है।”
(The task of the educator is not only to form habits, but also to break them – Sturt and Oakden, p. 238)
बुरी आदतों को तोड़ने के लिए शिक्षक और बालक निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं:
- संकल्प (Resolution)
बालक को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जेम्स के अनुसार, यह संकल्प अकेले न करके मित्रों, माता-पिता या सम्बंधियों के सामने करना अधिक प्रभावकारी होता है। उदाहरणतः, यदि सिगरेट छोड़नी है, तो इसका संकल्प सार्वजनिक रूप से करना चाहिए। - आत्म-सुझाव (Self-suggestion)
बालक स्वयं को बार-बार यह कह सकता है कि यह आदत हानिकारक है। उदाहरणः “सिगरेट पीने से कैंसर होता है, इसलिए मुझे इसे छोड़ देना चाहिए।” - ठीक अभ्यास (Correct Practice)
नाईट डनलप (Knight Dunlop) के अनुसार, यदि किसी बुरी आदत का अभ्यास गलत तरीके से किया गया है, तो उसे सही अभ्यास द्वारा सुधारना चाहिए। उदाहरणतः, गलत शब्द बोलने या लिखने की आदत को सही ढंग से बोलने या लिखने का अभ्यास कर सुधार सकते हैं। - नई आदत का निर्माण (Formation of New Habit)
किसी बुरी आदत को छोड़ने के स्थान पर एक अच्छी आदत अपनाना अधिक प्रभावकारी होता है। भाटिया के अनुसार,
“अच्छी आदत, बुरी आदत के प्रकटीकरण को अवसर नहीं देती है। अतः उसका स्वय ही अन्त हो जाता है।” - पुरानी आदत पर ध्यान (Focus on Old Habit)
तब तक बालक को अपनी पुरानी आदत पर ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए जब तक वह पूरी तरह उसे नहीं छोड़ देता। लापरवाही से आदत फिर लौट सकती है। - आदत का एकदम या धीरे-धीरे त्याग (Immediate or Gradual Abandonment)
जेम्स के अनुसार, कुछ आदतें एकदम छोड़ दी जा सकती हैं और कुछ को धीरे-धीरे। उदाहरणतः, नशीली वस्तुएँ एकदम छोड़ सकते हैं, जबकि चाय धीरे-धीरे कम करके पूरी तरह समाप्त की जा सकती है। - अप्रत्यक्ष आलोचना (Indirect Criticism)
कुछ आदतें संवेगात्मक असंतुलन से होती हैं, जैसे नाखून या कलम चबाना। शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से इसे आलोचना कर सकते हैं। उदाहरणः “नाखून चबाना हानिकारक है, क्योंकि गंदगी पेट में पहुँच सकती है।” - संगति में परिवर्तन (Change of Company)
बुरी आदतें अक्सर बुरी संगति के कारण पड़ती हैं। शिक्षक और माता-पिता को बालक को सही संगति में रखने का प्रयास करना चाहिए। - दण्ड (Punishment)
दण्ड का प्रयोग भी आदत तोड़ने में सहायक हो सकता है, परंतु यह तत्काल और उचित अवसर पर दिया जाना चाहिए। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार,
“कभी-कभी दण्ड, आदतों को तोड़ने में लाभप्रद होता है, पर दण्ड उचित अवसर पर ही दिया जाना चाहिए।” - पुरस्कार (Reward)
पुरस्कार बुरी आदतों को छोड़ने में दण्ड से अधिक प्रभावशाली होता है। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड का कथन है:
“Reward is better than punishment, praise is better than reproof.”
अर्थात, पुरस्कार और प्रशंसा दण्ड से उत्तम उपाय हैं।
शिक्षा द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार को वांछित दिशा में ढाल सकते हैं और उसमें स्थायित्व ला सकते हैं। इस प्रकार, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए संकल्प, आत्म-सुझाव, अभ्यास, नई आदत का निर्माण, संगति परिवर्तन, दण्ड और पुरस्कार—इन सभी विधियों का संयोजन आवश्यक है।
Very Important notes for B.ed.: बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव(balak par vatavaran ka prabhav) II sarva shiksha abhiyan (सर्वशिक्षा अभियान) school chale hum abhiyan II शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक II जेंडर शिक्षा में संस्कृति की भूमिका (gender shiksha mein sanskriti ki bhumika) II मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, maslow hierarchy of needs theory in hindi II थार्नडाइक के अधिगम के नियम(thorndike lows of learning in hindi) II थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत(thorndike theory of learning in hindi ) II पावलव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत (pavlov theory of classical conditioning in hindi) II स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत skinner operant conditioning theory in hindi