inclusive education in hindi समावेशी शिक्षा की अवधारणा । समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा की परिभाषा । समावेशी शिक्षा की विशेषताएं । समावेशी शिक्षा का क्षेत्र । समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत । समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है inclusive education introduction, inclusive education essay समावेशी शिक्षा का अर्थ – परिभाषा , अवधारणा, विशेषताएं , क्षेत्र ,आवश्यकता, सिद्धांत inclusive education in hindi
समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है (inclusive education concept)
समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक-बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है।
समावेशी शिक्षा का अर्थ (inclusive education meaning)
समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में inclusive education कहा जाता है जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना।
समावेशी शिक्षा की परिभाषा (inclusive education definition)
स्टीफन एवं ब्लैकहर्ट के अनुसार :-
“शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है।”
यरशेल के अनुसार :-
“समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर विकलांगता व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं।
शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार :-
” समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खुलती है।”
अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार : –
“समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती हैं जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।”
inclusive education in hindi
समावेशी शिक्षा की विशेषताएं(characteristics of inclusive education in hindi, features of inclusive education )
१. समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है।
Read More: जॉन डीवी के शैक्षिक विचार, जीवन परिचय, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक का स्थान, शिक्षण विधि
२. समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जा सकता है किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालयों में इनका प्रवेश कराया जाता है।
३. समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और वह समाज में सामान्य लोगों के तरह ही अपना जीवनयापन कर सके। इसीलिए ऐसे शिक्षण संस्थानों में नियमों में छूट दी जाती हैं और प्रभावशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि विशेषता लिए हुए बालक बहुत कम समय में ही अपने आपको सामान्य बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं।
४. समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती हैं। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है।
५. या एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।
६. समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हैं।
७. समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है।
८. समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता-पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है।
९. समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं दिए गए उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था है।
समावेशी शिक्षा के प्रकार (Types of Inclusive Education)
समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो सभी बच्चों, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक स्थिति में हों, को समान और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। यह शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से विकलांग बच्चों, वंचित वर्गों और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
समावेशी शिक्षा के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:
1. शैक्षणिक समावेश (Academic Inclusion)
शैक्षणिक समावेश (Academic Inclusion) एक ऐसा समावेशी शिक्षा का प्रकार है जिसमें विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक स्तर, सीखने की गति और विशेष जरूरतों के आधार पर समान अवसर प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी बच्चे, चाहे वे सामान्य हों या विशेष आवश्यकताओं वाले, एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ सकें और बराबरी से सीख सकें। इस प्रणाली में दृष्टिहीन छात्रों के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जाती है, वहीं धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए विशेष अध्यापक या सहायक उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे भी शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े रह सकें।
2. सामाजिक समावेश (Social Inclusion)
सामाजिक समावेश (Social Inclusion) का उद्देश्य सभी छात्रों को सामाजिक रूप से जोड़ना है ताकि वे भेदभाव से मुक्त, सहयोगात्मक और समावेशी वातावरण में मिल-जुलकर सीख सकें। यह प्रकार छात्रों को एक-दूसरे के साथ संवाद करने, सहयोग करने और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनमें सह-अस्तित्व, समानता और विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। उदाहरणस्वरूप, समूह कार्यों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी बच्चों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे वे एक-दूसरे को समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें।
3. भौतिक समावेश (Physical Inclusion)
भौतिक समावेश (Physical Inclusion) समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि स्कूल और कक्षा का भौतिक वातावरण सभी छात्रों, विशेषकर विकलांग बच्चों, के लिए अनुकूल और सुलभ हो। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि विद्यालय की संरचनाएं, सुविधाएं और संसाधन सभी छात्रों की भौतिक जरूरतों को पूरा करें, जिससे वे बिना किसी रुकावट के शिक्षा प्राप्त कर सकें। उदाहरणस्वरूप, व्हीलचेयर उपयोग करने वाले छात्रों के लिए रैंप की व्यवस्था, अलग-अलग प्रकार के टॉयलेट की उपलब्धता और सुनने में असमर्थ बच्चों के लिए श्रवण यंत्रों जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे वे भी आत्मनिर्भर होकर शिक्षा में भाग ले सकें।
4. भावनात्मक समावेश (Emotional Inclusion)
भावनात्मक समावेश (Emotional Inclusion) समावेशी शिक्षा का एक ऐसा पहलू है जिसमें बच्चों की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके तथा किसी भी प्रकार के तनाव, भय या असुरक्षा से मुक्त होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सके। यह प्रकार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने और उन्हें भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण प्रदान करने पर केंद्रित होता है। उदाहरणस्वरूप, विद्यालयों में परामर्शदाता (Counselor) की व्यवस्था की जाती है और कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण तथा सकारात्मक माहौल बनाया जाता है, जिससे बच्चे खुलकर अपनी बात कह सकें और भावनात्मक रूप से समर्थ बन सकें।
5. सांस्कृतिक और भाषायी समावेश (Cultural & Linguistic Inclusion)
सांस्कृतिक और भाषायी समावेश (Cultural & Linguistic Inclusion) का उद्देश्य ऐसे बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है जो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं या जिनकी मातृभाषा भिन्न होती है। यह समावेश सुनिश्चित करता है कि भाषा, धर्म, रीति-रिवाज या सांस्कृतिक पहचान के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। इसके अंतर्गत शिक्षण प्रणाली को इस प्रकार अनुकूल बनाया जाता है कि वह विविध भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करे और सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करे। उदाहरणस्वरूप, द्विभाषीय शिक्षा व्यवस्था की जाती है जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाएं भी सीख सकें, और स्कूलों में सांस्कृतिक विविधता का आदर व समावेश किया जाता है ताकि हर छात्र को अपनी पहचान के साथ सहज महसूस हो।
समावेशी शिक्षा का क्षेत्र (scope of inclusive education in hindi)
समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है। जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य है अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है।
१. शारीरिक रूप से बाधित बालक:
शारीरिक रूप से बाधित बालक वे होते हैं जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से ग्रसित होते हैं, जैसे—चलने-फिरने में असमर्थता, दृष्टिहीनता, श्रवण बाधित होना या वाणी विकार से पीड़ित होना। ऐसे बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखा जाए, इसके लिए समावेशी शिक्षा उन्हें सामान्य विद्यालयों में पढ़ाई का अवसर प्रदान करती है। उदाहरणस्वरूप, एक बच्चा जो व्हीलचेयर का उपयोग करता है, उसके लिए स्कूल परिसर में रैंप, विशेष बैठने की व्यवस्था, सहायक उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वह बिना किसी भेदभाव के अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हो सके।
२. मानसिक रूप से बाद बालक:
मानसिक रूप से बाधित बालक वे होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में कम होती है, जिससे उन्हें सीखने और समझने में अधिक समय लगता है। इस श्रेणी में मंदबुद्धि (Mental Retardation), आत्मविकास संबंधी समस्याएँ (जैसे ऑटिज़्म), और सीखने में कठिनाई (जैसे Dyslexia) से ग्रसित बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष रणनीतियों, धैर्य और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा इन बच्चों को भी समान अधिकार और अवसर देने की बात करती है, ताकि वे उपयुक्त सहायता और सहयोग के साथ शिक्षित होकर आत्मनिर्भर जीवन जी सकें और समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें।
३. सामाजिक रुप से बाधित/विचलित बालक:
सामाजिक रूप से बाधित या विचलित बालक वे होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक कारणों से शिक्षा की मुख्यधारा से कटे हुए होते हैं। इस श्रेणी में वे बच्चे शामिल होते हैं जो अत्यंत गरीबी में जीवन जीते हैं, बाल श्रम, बाल विवाह या बाल तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के शिकार होते हैं, अनाथ होते हैं या सड़कों पर जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अतिरिक्त दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग के वे बच्चे भी आते हैं जिन्हें समाज में भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। समावेशी शिक्षा इन सभी बच्चों को समान अवसर और संसाधन प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करती है, ताकि वे भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
४. शैक्षिक रूप से बाधित बालक:
शैक्षिक रूप से बाधित बालक वे होते हैं जो किसी न किसी कारणवश शैक्षिक प्रगति में पिछड़ जाते हैं। इनमें वे बच्चे शामिल होते हैं जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते, पढ़ाई में कमजोर होते हैं या भाषा, गणित जैसे विषयों में पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा, जिनके अभिभावकों की शिक्षा का स्तर कम होता है और जिन्हें घर से पढ़ाई में सहयोग नहीं मिल पाता, वे भी इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी क्षमताओं को निखारने के लिए समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षण विधियाँ, रेमेडियल क्लासेस और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की व्यवस्था करती है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें और शिक्षा से वंचित न रह जाएं।
समावेशी शिक्षा के लाभ (inclusive education benefits)
समावेशी शिक्षा वह शैक्षणिक व्यवस्था है जिसमें सामान्य, अक्षम, विशिष्ट आवश्यकता वाले और समस्यात्मक बच्चे सभी को एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से एकजुट बनाना है। समावेशी शिक्षा के अनेक लाभ हैं जो न केवल छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायक हैं, बल्कि पूरे समाज को भी सशक्त बनाते हैं।
समावेशी शिक्षा के प्रमुख लाभ:
सभी बच्चों के लिए समान अवसर
समावेशी शिक्षा में अक्षम, विशिष्ट आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग-थलग महसूस नहीं होता और वे भी समान अवसरों का लाभ उठाते हैं।वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान
यह शिक्षा प्रणाली विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ लाकर उनकी अलग-अलग आवश्यकताओं को पहचानती है और उनके अनुसार शिक्षण की योजना बनाती है। इससे भिन्नताओं को नकारने के बजाय उन्हें स्वीकारने और समझने की संस्कृति बनती है।भेदभाव और छुआछूत की भावना का अंत
जब सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक क्षमता जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने में सहायता मिलती है। इससे एक समरस और संवेदनशील समाज की नींव रखी जाती है।समाज का लघु रूप तैयार होता है
समावेशी कक्षा में विविध पृष्ठभूमियों वाले बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो वहाँ एक लघु समाज का निर्माण होता है। बच्चे एक-दूसरे से सहयोग करना, संघर्ष सुलझाना और सामंजस्य बनाना सीखते हैं।समायोजन (Adjustment) के कौशल का विकास
समावेशी शिक्षा बच्चों को विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व और क्षमताओं के साथ तालमेल बैठाने की कला सिखाती है। यह भविष्य में किसी भी कार्यक्षेत्र में समायोजन की समस्या को दूर करने में सहायक होती है।विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बेहतर समझ और सहयोग
समावेशी शिक्षा शिक्षकों और सहपाठियों को अक्षम या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में सहायता करती है। इससे इन बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।समस्यात्मक बच्चों के लिए उपयोगी
जिन बच्चों में व्यवहारिक या मानसिक समस्याएं होती हैं, समावेशी शिक्षा उनकी कमजोरियों की पहचान कर उन्हें सही मार्गदर्शन देती है। इससे वे सामान्य बच्चों की तरह विकास कर सकते हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े होने से बच सकते हैं।
- समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है।
- समावेशी शिक्षा के कारण वैयक्तिक विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण किया जाता है ।
- समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव,छूआ छूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि कि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है।
- समावेशी शिक्षा समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है।
- विशिष्ट बालक, अपंग बालक, या अक्षम बालक की विभिन्न समस्या को जानकर उनके उन समस्याओं की समाधान में समावेशी शिक्षा सहायक होती है।
- समावेशी शिक्षा उन बालकों के लिए भी लाभप्रद है जो समस्यात्मक बालक होते हैं समावेशी शिक्षा उनके उन कमजोरी को जानकर उनके समस्या को दूर करने का प्रयास करता है तथा उन्हें समस्यात्मक बालक बनने से रोकता है।
समावेशी शिक्षा की आवश्यकता(need of inclusive education in hindi, inclusive education needs)
समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास करता है भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके।
नीचे हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में बिंदु बद रूप से पढ़ेंगे –
- समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
- समावेशी शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है।
- जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसमें सामान्य तथा अपंग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं जिससे उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है जिससे बालकों में एकता, भाईचारा और समानता का भावना उत्पन्न होता है।
- जहां सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहां शिक्षा में भी कम खर्च होता है क्योंकि जहां अलग-अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है वह केवल समावेशी शिक्षा कम खर्च या लागत में कर लेता है।
- समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां लघु समाज का निर्माण होता है क्योंकि यहां हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसके कारण उनमें नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है।
- समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा जैसे भावनाओं का भी विकास किया जाता है।
- आज के युग में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि यह शिक्षा ही आज के समाज में बदलाव ला सकता है इसलिए समावेशी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए।
- विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे एक सीमित और अलग वातावरण में ढल जाते हैं। जब वे समाज में वापस लौटते हैं, तो उन्हें सामान्य परिस्थितियों और लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर, सामान्य बच्चे भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे वे उनके साथ संवेदनशीलता और सहयोग का व्यवहार नहीं सीख पाते।
- सामान्य विद्यालय प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, जबकि विशेष विद्यालय केवल कुछ ही बड़े शहरों में स्थित होते हैं। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- जब विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो कक्षा का वातावरण अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण बनता है। यह विविधता सभी विद्यार्थियों को एक-दूसरे से सीखने, सहिष्णु बनने और सहयोग की भावना विकसित करने में मदद करती है।
- यह धारणा गलत है कि केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ही सीखते हैं। दरअसल, सामान्य बच्चे भी दिव्यांग बच्चों से कई जीवनोपयोगी गुण जैसे सहनशीलता, संघर्षशीलता, और करुणा सीखते हैं। हर बच्चा किसी-न-किसी विशेषता का धनी होता है, जो कक्षा के समग्र विकास में योगदान देता है।
inclusive education in hindi
समावेशी शिक्षा का महत्व (importance of inclusive education in hindi)
समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं, और सभी को समान अवसर एवं संसाधन प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समानता, न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देना है। समावेशी शिक्षा न केवल बच्चों को अकादमिक रूप से सक्षम बनाती है, बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी उन्हें परिपक्व बनाती है।
समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित हैं-
समानता और एकता का विकास
जब सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो उनके बीच सहयोग, सहानुभूति और समानता की भावना विकसित होती है। इससे समाज में भेदभाव की भावना कम होती है और सभी के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है।कम खर्चीली शिक्षा व्यवस्था
समावेशी शिक्षा में एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत सभी बच्चों को एक ही संस्थान और संसाधनों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है, जिससे अलग-अलग विशेष स्कूलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह शिक्षा प्रणाली अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव बनाती है।मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास
विविधताओं से भरे इस वातावरण में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सहयोग, सहिष्णुता और नेतृत्व की भावना का विकास होता है। वे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं।प्राकृतिक एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण
जब सभी बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं, तो एक स्वाभाविक और अनौपचारिक वातावरण का निर्माण होता है जिसमें हर बच्चा स्वतंत्रता, समानता और आत्मीयता महसूस करता है। यह वातावरण बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है।समायोजन की समस्या का समाधान
समावेशी शिक्षा बच्चों को विविध सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में अनुकूल बनाने में सहायक होती है। वे विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ रहना, सीखना और सहयोग करना सीखते हैं, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के सामाजिक या कार्यस्थलीय समायोजन में कठिनाई नहीं आती।समाज में समावेशी दृष्टिकोण का विकास
जब प्रारंभिक अवस्था से ही समावेशिता की भावना बच्चों में विकसित होती है, तो बड़े होकर वे समाज में सभी वर्गों और समुदायों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। इससे सामाजिक एकता और समरसता को बल मिलता है।
- समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है
- जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं इसलिए या शिक्षा कम खर्चीली भी होती है।
- समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास उनके अंदर नैतिक विकास सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जाता है।
- जहां सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता हो वहां प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है।
- यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।
समावेशी शिक्षा के सिद्धांत (Theory of inclusive education, theory of inclusive special education)
समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत है-
१. वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना
समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसके कारण उन में विभिन्न तरह के वातावरण उत्पन्न होता है वातावरण को एक ही वातावरण में डालने का काम समावेशी शिक्षा करता है।
२. विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा
समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है बालक विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेकर या उन्हें देखकर उनके अंदर अधिगम की शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है।
३. भेदभाव रहित शिक्षा
समावेशी शिक्षा जहां बिना किसी भेदभाव के सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती हैं जिससे उनके अंदर भेदभाव की भावना को मिटाया जाता है समावेशी शिक्षा भेदभाव को दूर करने छुआछूत ओं को दूर करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है।
४. माता-पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना
समावेशी शिक्षा में ना केवल बच्चों की शिक्षा में शिक्षक ही सहायक होते हैं बल्कि उन बच्चों के माता-पिता भी उनके शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं उनकी सहायता करते हैं। जिससे उनके अंदर अधिगम की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है बच्चे अपने माता-पिता के सहयोग पाकर और अच्छी तरह से अधिगम कर पाते हैं।
५. व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता
जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें सामान्य बालकों के सामान बनाया जा सके।
६. लघु समाज का निर्माण
समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक जैसे सामान्य बालक प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक अपंग बालक एक ही विद्यालय में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं जिससे उनमें एक लघु समाज का निर्माण होता है।
समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है (What are the teaching competencies a teacher should have in inclusive education)
समावेशी शिक्षा में शिक्षक में इन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है:-
- अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण आधार होती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंध होती है। अतः शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान ना करें, जिससे कि वे डर जाए। जैसे कक्षा में अपमान निंदा करना, दंड देना क्योंकि कभी-कभी नकारात्मक अभिप्रेरणा से बालक की हानि भी हो जाती है। समावेशी शिक्षा में विभिन्न तरह के विद्यार्थी होते हैं अतः इस बात का ध्यान शिक्षक को हमेशा होना चाहिए और समावेशी शिक्षा में हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा ही देना चाहिए। एक शिक्षक को बच्चों को अभिप्रेरित करने की पूरी दक्षता होनी चाहिए।
- समावेशी शिक्षा में एक अध्यापक में यह दक्षता भी होना चाहिए कि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले छात्रों को यह बता देना चाहिए कि वह कार्य उनकी किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी क्योंकि उनकी आवश्यकताएं उन्हीं के अधिगम में उद्दीपन के रूप में कार्य करती है और समावेशी शिक्षा में यह बहुत अहम भूमिका निभाती है।
- समावेशी शिक्षा में शिक्षकों का कार्यभार सबसे अधिक होता है जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वह अत्यंत तनावग्रस्त और निराश हो जाते हैं इसका प्रभाव कक्षा में भी दिखाई देता है अतः शिक्षक में समायोजन करने की दक्षता भी होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो जिससे वह प्रसन्नचित रहकर शिक्षण का कार्य पूर्ण रुचि के साथ कर सकें।
- शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए आदर्श व्यक्तित्व होता है। अतः उसे उच्च चरित्र एवं नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनमें ईमानदारी, नियमबध्दता, जैसे गुणों का परिचय मिलता हो। एक अध्यापक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को नैतिक एवं चारित्रिक रूप से उत्कृष्ट करने का प्रयास करें जिसके लिए उसे स्वयं में इन गुणों का विकास करना पड़ेगा। शिक्षक के निपुणता का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी दिखाई पड़ता है।
- एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं प्रज्वलित नहीं होगा इसलिए शिक्षक में अपने विषय में निपुणता या ज्ञाता या विद्वान होना अत्यंत आवश्यक है। विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर शिक्षक कक्षा में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ शिक्षण का कार्य कर पाता है।
- एक शिक्षक में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि समावेशी शिक्षा के दौरान वे किस कक्षा में किस प्रकार के सहायक शिक्षण सामग्री(TLM) का उपयोग करें। समावेशी शिक्षा में TLM का विशेष प्रभाव होता है क्योंकि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती हैं जिसमें हर प्रकार के विद्यार्थी मौजूद होते हैं तो शिक्षक उनके जरूरतों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करें।
- शिक्षक में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होना अनिवार्य है। शिक्षक को अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाना होता है अतः उसमें अपने भावों को प्रकट करने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो विद्यार्थियों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त अच्छी भावाभिव्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट, प्रभावपूर्ण आवाज, भाषा सरल एवं प्रासंगिक उदाहरण युक्त तथा धारा प्रवाह कथन के रूप में हो।
- समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के विद्यार्थी मौजूद होते हैं जिससे एक लघु समाज का निर्माण होता है अत: शिक्षक में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि वह इस लघु समाज को व्यापक समाज में कैसे बदल सकता है। इसके लिए वे विभिन्न प्रकार की उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं।
- कोई भी विद्यार्थी शिक्षा क्यों ग्रहण करता है ताकि उनके जो लक्ष्य हैं उसे वे पा सके। समावेशी शिक्षा में भी बच्चों के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उन्हें उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। एक शिक्षक में इन दक्षताओं का होना भी आवश्यक है।
समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए या समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं
समावेशी शिक्षा के दौरान अनेक समस्याओं या बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें से कुछ प्रमुख समस्या या बाधा इस प्रकार हैं-
१. शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी:
समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं सामान्य बालक अक्षम बालक सभी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और यही कारण है कि एक शिक्षक को उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए उन्हें कक्षा के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना आना चाहिए साथ ही एक शिक्षक में इतनी शिक्षण कौशलों का विकास होना चाहिए कि वह विशिष्ट एवं सामान्य बालकों की समस्या को समझ कर उनकी समस्या का समाधान कर सके पर ये क्षमता सभी शिक्षक पर नहीं पाया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या शिक्षक में शिक्षण कौशलों का विकास में कमी होना है।
२. सामाजिक मनोवृत्ति:
हम जिस देश या समाज में रहते हैं यहां के लोगों की सामाजिक मनोवृत्ति ही ऐसी है कि अक्षम बालक या विशिष्ट बालको को नकारात्मक भाव से देखते हैं उनके मन में उस बालक के प्रति पहले से ही नकारात्मक भावना बैठ चुका है कि यह बालक आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा साथ ही उनके परिवार या माता-पिता उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। उन्हें समाज से दूर रखते हैं। उन्हें शिक्षा देना भी नहीं चाहते और जो बालक आगे भी बढ़ना चाहते हैं उनके मन में यह बातें बैठा दी जाती हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ये सामाजिक मनोवृत्ति समावेशी शिक्षा की समस्याओं का एक अहम हिस्सा ही है जो हर एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में घर कर बैठा है।
३. शारीरिक बाधाएं:
समावेशी शिक्षा की और एक बड़ी समस्या यह भी है कि जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम है बाधिर है ऐसे बालकों को अधिगम में समस्या होती ही है और वह किसी भी चीज को धीरे धीरे सीखते हैं उन्हें सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है पर उनके इन समस्याओं को नजरअंदाज कर उनके साथ सामान्य बालक जैसे ही व्यवहार, शिक्षण विधियां, प्रवृत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। जिससे उनमें समस्या उत्पन्न होने लगती हैं।
४. पाठ्यक्रम :
पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम लाचीला, उपयोगी एवं सामान्य एवं विशिष्ट बालक या अक्षम बालक सभी के अनुरूप हो।
५. भाषा और संवाद में समस्या:
जैसे की हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं जिसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो श्रावण वाचन लेखन पठन में बहुत ही पीछे होते हैं। जिसके कारण भाषा को समझने और संवाद करने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि समावेशी शिक्षा इतनी आसान नहीं है। इन समस्याओं का सामना सभी शिक्षक नहीं कर पाते है।
६. भारतीय शिक्षा नीतियां से बाधाएं:
भारत में बहुत से ऐसे शिक्षा नीतियां हैं जो समावेशी शिक्षा के बीच रुकावट या बाधा उत्पन्न करती है शिक्षक या स्कूल उन नीतियों के दायरे में रहते हैं जो समावेशी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करती है।
आज के इस लेख में हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा । समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा की परिभाषा । समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र । समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत ।समावेशी शिक्षा का महत्व । समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है के बारे में पढ़ा उम्मीद है आप सभी को इस लेख की मदद से काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
समावेश शिक्षा के मुख्य उद्देश्य
समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे देश का विकास बालको को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संस्थानो का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यवसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना। इन उदेश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है-
1. सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करना
समावेशी शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। समाज में बहुत से बच्चे—विशेषकर विकलांग, निर्धन, अल्पसंख्यक या आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले—अक्सर मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर रह जाते हैं। समावेशी शिक्षा उनके लिए एक समान अवसर प्रदान करती है, जिससे वे भी समान रूप से सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें।
2. विविधता को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना
हर बच्चा अलग होता है। उसकी सीखने की गति, रुचियाँ, सामाजिक परिवेश और ज़रूरतें भिन्न होती हैं। समावेशी शिक्षा इन भिन्नताओं को बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य यह है कि स्कूलों में ऐसी व्यवस्था हो जहां हर प्रकार के बच्चे को समझा जाए और उसे अनुकूल शिक्षा दी जाए।
3. भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली विकसित करना
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव न किया जाए। यह एक ऐसा वातावरण तैयार करने पर बल देती है जहां हर छात्र को समान मान्यता और सम्मान मिले।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना
ऐसे बच्चे जो दृष्टिहीन, श्रवण बाधित, मानसिक रूप से कमजोर या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा उन्हें अलग-थलग करने की जगह उन्हें बाकी छात्रों के साथ मिलाकर शिक्षित करती है ताकि उनमें आत्मविश्वास, सामाजिकता और आत्मनिर्भरता विकसित हो।
5. सामाजिक समरसता और एकजुटता को बढ़ावा देना
समावेशी शिक्षा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को एक साथ पढ़ने का अवसर देती है, जिससे वे एक-दूसरे की संस्कृतियों, जीवनशैली और समस्याओं को समझते हैं। इससे समाज में आपसी समझ, सहिष्णुता और सद्भाव का विकास होता है।
6. शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए सक्षम बनाना
इसका एक उद्देश्य यह भी है कि शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों के साथ सहज रूप से व्यवहार कर सकें। शिक्षक यदि समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं, तो वे हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से समझ पाएंगे और उसकी मदद कर पाएंगे।
7. सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना
समावेशी शिक्षा सामाजिक असमानता को मिटाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। जब सभी वर्गों के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो सामाजिक वर्गों में बंटवारा कम होता है और समानता की भावना का निर्माण होता है।
8. हर बच्चे की प्रतिभा को पहचानना और निखारना
समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेष होता है। यह प्रणाली सभी को समान पाठ्यक्रम के ढांचे में नहीं बाँधती बल्कि यह प्रयास करती है कि हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उसे शिक्षा दी जाए।
- शारिरिक अक्षमता वाले बालकों के माता-पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना।
- शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना।
- शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय करना तथा बालको के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना।
- शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना चाहिए ।
समावेशी शिक्षा आज के युग में कितनी जरूरी है और क्यों?
अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचे तो यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। अर्थात कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना तथा कुछ बच्चें जिनकी आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हैं उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा इसमें जरूरी है-
१. क्योंकि सभी बच्चे चाहे वह कैसे भी आवश्यकता वाले हो, एक ही समाज में रहना है अतः शुरू से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी।
२. क्योंकि सामान्य विद्यालय सभी जगह है जबकि विशेष विद्यालय दूर शहरों में होते हैं अतः एक ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय जाने के लिए दूर तक सफर करना पड़े तो या उस बच्चे के मूल अधिकार का हनन है।
प्रत्येक राष्ट्र अपने यहां के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास करता है ताकि राष्ट्रीय की उन्नति हो सके। यह बात तो सिध्द है कि जिस राष्ट्रीय के ज्यादातर लोग शिक्षित है वह राष्ट्र ज्यादा उन्नति कर रहा है तथा जिस राष्ट्र के कम लोग पढ़े लिखे हैं वह राष्ट्र गरीब हैं।
अतः समावेशी शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे अपने पास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले विशेष स्कूल दूर होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे वे अब समावेशी शिक्षा के आने से पास के स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं सभी प्रकार के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने पर राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में वह राष्ट्र अवश्य ही विकसित राष्ट्र बनेगा।
समावेशी शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि जब एक ही स्कूल में विकलांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियां एवं क्षमताएं जानने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा दूर होगी वही विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं।
कक्षा-कक्ष में समावेशी शिक्षा कैसे लागू करें? (How to Implement Inclusive Education in a Classroom)
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि हर बच्चे को उसकी सामाजिक, भौतिक, बौद्धिक या भाषाई विविधता के बावजूद समान अवसर मिले। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है:
1. अधिगमकर्ता का समावेशन (Inclusiveness of Learner)
- RTE Act 2009 (अनुच्छेद 3 और 4): इस अधिनियम के अनुसार, सभी प्रकार के बच्चे — चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, धर्म, भाषा, शारीरिक या मानसिक स्थिति के हों — उन्हें एक समान विद्यालय में एक ही कक्षा में साथ-साथ पढ़ने का अधिकार है।
- NEP 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020): समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2025 तक सभी स्कूलों को समावेशी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- लिंग, जाति, नृजातीयता, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव रहित प्रवेश: किसी भी प्रकार का भेदभाव विद्यालयों में प्रवेश या शिक्षा के दौरान नहीं किया जाएगा।
- आयु आधारित प्रवेश (Age-Based Admission): सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के अनुसार, जिस बच्चे की उम्र 31 मार्च को 5 वर्ष पूरी हो रही हो, उसे 6 वर्ष की उम्र में पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। अन्य कक्षाओं का निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाएगा।
- आयु समरूप कक्षा (Age-Homogeneous Class): कक्षा में शामिल सभी बच्चे लगभग समान उम्र वर्ग के होने चाहिए ताकि सामाजिक एवं मानसिक संतुलन बना रहे।
- ब्रिज कोर्स और विद्या प्रवेश कार्यक्रम: जिन बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा नहीं मिली है या जो सीधे उच्च कक्षा में दाखिला लेते हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स संचालित किए जाएंगे। NEP 2020 ने ‘विद्या प्रवेश’ नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है।
2. अधिगम प्रक्रिया में समावेशन (Inclusiveness in Learning Process)
वैयक्तिक विभिन्नताएं और शिक्षण रणनीति: हर बच्चा अलग होता है—उसकी समझने की क्षमता, रुचियाँ और ज़रूरतें भिन्न होती हैं। एक नवाचारी और संवेदनशील शिक्षक ही ऐसी विविधता को समझते हुए शिक्षण प्रक्रिया को सफल बना सकता है। अधिगम की प्रक्रिया को लचीला और विद्यार्थी-केंद्रित बनाना समावेशी शिक्षा की कुंजी है।
3. कक्षा-कक्ष का वातावरण (Inclusive Classroom Environment)
मैत्रीपूर्ण और भयमुक्त वातावरण: समावेशी कक्षा में बच्चों को सीखने का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ वे बिना डर और झिझक के खुलकर अपनी बात कह सकें। शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका निभाते हुए लोकतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक माहौल तैयार करना चाहिए।
शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता: कक्षा में विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, जो सभी बच्चों की पहुँच में हो, विशेषकर दिव्यांग छात्रों के लिए। दृश्य, श्रव्य और स्पर्श आधारित संसाधन समान रूप से सुलभ होने चाहिए।
4. सहकारी शिक्षण (Cooperative / Collaborative Learning)
- समूह आधारित गतिविधियाँ: शिक्षक को सहपाठी शिक्षण (peer learning) और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे विद्यार्थी एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, सहयोग की भावना विकसित करते हैं और एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हैं।
- साझा जिम्मेदारी: समूह गतिविधियाँ केवल दिव्यांग छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होती हैं। इससे सहिष्णुता, सहयोग और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं।
5. समावेशी पाठ्यक्रम (Inclusive Curriculum)
- लचीला और विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सामान्य और दिव्यांग दोनों प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल, श्रवण बाधित छात्रों के लिए संकेत भाषा, मानसिक मंद बच्चों के लिए सरल भाषा और गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रम में अनुकूलन: कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव आवश्यक हो सकता है, जबकि कुछ के लिए केवल प्रस्तुतिकरण का तरीका बदलना पर्याप्त होता है।
6. मूल्यांकन में समावेशन (Inclusive Assessment)
- व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित आकलन: हर छात्र की प्रगति को एक ही मापदंड से नहीं आँका जा सकता। समावेशी मूल्यांकन में विविध तकनीकों—जैसे मौखिक उत्तर, परियोजनाएँ, गतिविधियाँ और पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाना चाहिए।
- पारंपरिक आकलन से आगे: केवल लिखित परीक्षा के बजाय आकलन में विविधता लाना आवश्यक है, ताकि सभी बच्चों की वास्तविक क्षमताओं को समझा जा सके।
7. क्षमताओं पर ध्यान दें, अक्षमताओं पर नहीं (Focus on Abilities, Not Disabilities)
सकारात्मक दृष्टिकोण: शिक्षक, अभिभावक और समाज को बच्चों की अक्षमताओं के बजाय उनकी संभावनाओं और क्षमताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक बच्चा जो किसी एक क्षेत्र में सीमित है, वह किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट हो सकता है।
निष्कर्ष:
समावेशी शिक्षा कोई एकल पद्धति नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण है जो समानता, गरिमा और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। यदि शिक्षक, स्कूल, पाठ्यक्रम और समाज मिलकर कार्य करें, तो समावेशी शिक्षा के सपने को वास्तविकता में बदला जा सकता है।
Very Important notes for B.ed.: बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव(balak par vatavaran ka prabhav) II sarva shiksha abhiyan (सर्वशिक्षा अभियान) school chale hum abhiyan II शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक II किशोरावस्था को तनाव तूफान तथा संघर्ष का काल क्यों कहा जाता है II जेंडर शिक्षा में संस्कृति की भूमिका (gender shiksha mein sanskriti ki bhumika) II मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, maslow hierarchy of needs theory in hindi II थार्नडाइक के अधिगम के नियम(thorndike lows of learning in hindi) II थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत(thorndike theory of learning in hindi ) II स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार , जीवन दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, आधारभूत सिद्धांत II महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शैक्षिक चिंतान एवं सिद्धांत II
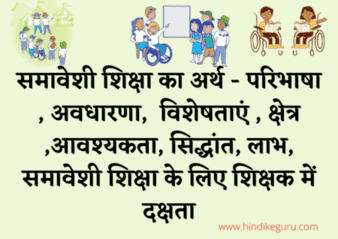
समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन शिक्षण दक्षता ओं का होना आवश्यक है इसके बारे में भी लिखिए
आपका लेख अत्यंत सुंदर एवं बहुत लाभकारी है