स्वच्छन्दतावाद : परिभाषा, विशेषताएँ और हिन्दी साहित्य में प्रभाव
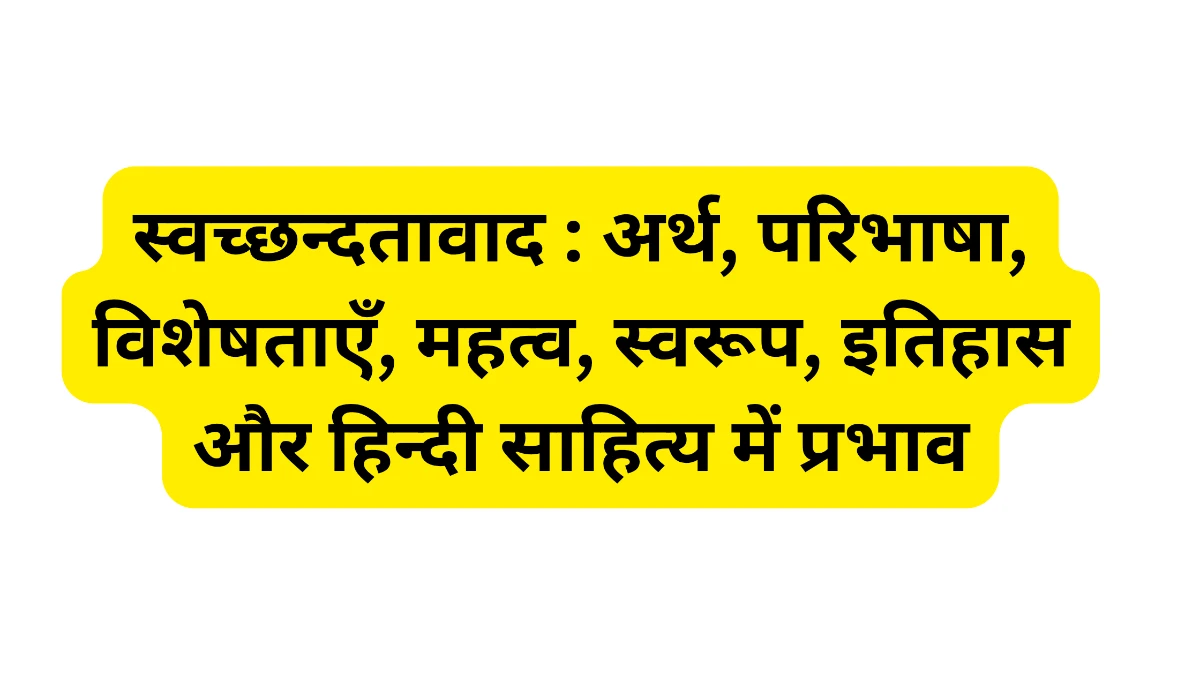
स्वच्छन्दतावाद (अंग्रेज़ी: Romanticism) कला, साहित्य और बौद्धिक चेतना का एक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन था, जिसका उदय अठारहवीं शताब्दी के अन्त में यूरोप में हुआ। 1800 से 1850 के बीच यह आन्दोलन अपने चरम पर पहुँचा और साहित्य को नई दिशा प्रदान की।
स्वच्छन्दतावाद का अर्थ और परिभाषा
स्वच्छन्दतावाद का शाब्दिक अर्थ है ‘स्वतंत्रता’ या ‘मुक्ति’। जिस प्रकार फ्रांसीसी क्रान्ति ने राजनीति में स्वतंत्रता का बिगुल बजाया, उसी प्रकार स्वच्छन्दतावाद ने साहित्य को परम्परागत बंधनों से मुक्त कर एक नई चेतना प्रदान की।
हिन्दी साहित्य में यह धारा 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में विशेष रूप से उभरकर सामने आई, जब छायावादी काव्य के रूप में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियाँ दिखाई दीं।
डॉ॰ अमरनाथ के अनुसार हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने ग्रन्थ हिन्दी साहित्य का इतिहास में किया। उन्होंने श्रीधर पाठक को इस धारा का प्रवर्तक माना। डॉ॰ अमरनाथ का मत है कि छायावाद और स्वच्छन्दतावाद में गहरा साम्य है। दोनों में प्रकृति-प्रेम, मानवीय दृष्टिकोण, आत्माभिव्यक्ति, रहस्यभावना, प्राचीन संस्कृति के प्रति अनुराग, प्रतीक-योजना, निराशा, पलायन और अहं के उदात्तीकरण जैसे तत्व विद्यमान हैं।
पाश्चात्य साहित्य में स्वच्छन्दतावाद
पश्चिमी साहित्य में इस आन्दोलन की जड़ें रूसो के विचारों से जुड़ी हुई थीं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने इसे साहित्यिक आन्दोलन का रूप प्रदान किया, जिसे अंग्रेज़ी आलोचना में Romanticism कहा गया।
आचार्य शुक्ल ने इस शब्द का हिन्दी अनुवाद ‘स्वच्छन्दतावाद’ किया। उनके मतानुसार द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक के नेतृत्व में जिस काव्यधारा का विकास हुआ, उसे प्रवृत्तियों के आधार पर स्वच्छन्दतावाद कहा जा सकता है।
स्वच्छन्दतावाद के प्रवर्तक
स्वच्छन्दतावाद का उद्भव किसी एक व्यक्ति अथवा देश की देन नहीं था, बल्कि यह यूरोप के सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में धीरे-धीरे विकसित हुआ। फिर भी इसके प्रवर्तकों के रूप में कुछ प्रमुख नाम वैश्विक स्तर पर, अंग्रेजी साहित्य में और हिन्दी साहित्य में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं।
1. विश्व स्तर पर – ज्याँ-ज़ाक रूसो (Jean-Jacques Rousseau)
स्वच्छन्दतावादी चिन्तन की बौद्धिक नींव रखने का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक ज्याँ-ज़ाक रूसो को दिया जाता है। उन्होंने मनुष्य की स्वाभाविक स्वतंत्रता, भावनाओं और प्रकृति के प्रति प्रेम को अपने दर्शन का आधार बनाया। रूसो की रचनाओं और विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी गहन प्रेरणा दी। इस प्रकार वे न केवल राजनीतिक और सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत बने, बल्कि स्वच्छन्दतावाद की वैचारिक भूमि तैयार करने वाले प्रमुख चिन्तक भी सिद्ध हुए।
2. अंग्रेजी साहित्य में – विलियम वर्ड्सवर्थ (William Wordsworth)
अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद का वास्तविक सूत्रपात विलियम वर्ड्सवर्थ से माना जाता है। 1798 ई. में उन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर ‘लिरिकल बैलेड्स’ (Lyrical Ballads) का प्रकाशन किया, जिसने अंग्रेजी काव्य में नयी दिशा प्रदान की। वर्ड्सवर्थ ने कविता को “भावनाओं का सहज उच्छलन” कहा और साधारण जन-जीवन तथा प्रकृति को अपनी काव्य-दृष्टि का केन्द्र बनाया। यही कारण है कि उन्हें अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद का प्रवर्तक माना जाता है।
3. हिन्दी साहित्य में – पंडित श्रीधर पाठक
हिन्दी साहित्य में पंडित श्रीधर पाठक को स्वच्छन्दतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उन्हें खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छन्दतावादी कवि कहा है। पाठक जी ने परम्परागत काव्य-धारा से हटकर वैयक्तिक भावनाओं, प्रकृति-सौन्दर्य और नवीन कल्पनाओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। इस प्रकार उन्होंने हिन्दी काव्य में स्वच्छन्दतावाद की नींव रखी और बाद के छायावादी कवियों को मार्ग प्रशस्त किया।
अतः स्पष्ट है कि—
- ज्याँ-ज़ाक रूसो ने स्वच्छन्दतावादी चिन्तन की दार्शनिक नींव रखी,
- विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे अंग्रेजी साहित्य में सशक्त काव्य-धारा के रूप में प्रतिष्ठित किया,
- और पंडित श्रीधर पाठक ने हिन्दी साहित्य में इसके प्रवर्तक का कार्य किया।
स्वच्छंदतावाद का इतिहास और विकास
स्वच्छंदतावाद की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जहां विलियम वर्ड्सवर्थ के ‘Lyrical Ballads’ ने इस काव्यधारा का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद कॉलरिज़, शेली, बायरन, कीट्स और सर वाल्टर स्कॉट जैसे कवि इस आंदोलन को विकसित करने में अग्रणी रहे। यह आंदोलन फ्रांस, जर्मनी, इटली सहित कई यूरोपीय देशों में फैला, लेकिन भारत में इसका स्वर विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक गुलामी विरोधी था। हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रभाव बीसवीं सदी के दूसरे दशक में छायावाद के रूप में देखने को मिला, जिसमें मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामनरेश त्रिपाठी जैसे प्रसिद्ध कवि हुए।
स्वच्छंदतावाद का साहित्य पर प्रभाव
यह आंदोलन केवल कविता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उपन्यास, निबंध, कला, दर्शन और संगीत सहित अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य में इसे छायावाद के माध्यम से समझा जाता है, जिसमें आत्माभिव्यंजन, रहस्यभावना, प्रेमालाप, निराशा और व्यक्तिगत भावनाओं का प्रबल प्रदर्शन होता है। स्वच्छंदतावाद ने हिंदी साहित्य को नए विषय, नए शिल्प और नए प्रकार की अभिव्यक्ति दी, जिसने परंपरागत सीमाओं को तोड़ा और स्वतंत्रता के नए आयाम स्थापित किए।
प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि
– मैथिलीशरण गुप्त
– माखनलाल चतुर्वेदी
– सुभद्रा कुमारी चौहान
– रामनरेश त्रिपाठी
– जयशंकर प्रसाद
– महादेवी वर्मा
– सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
ये कवि अपनी काव्य रचनाओं में स्वतंत्रता, भावना, प्रकृति प्रेम और व्यक्तिवाद को प्रमुखता देते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध किया।
इस प्रकार, स्वच्छंदतावाद हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी विचारधारा है जिसने साहित्य को आत्मिक, मुक्त और कल्पनाशील बनाया। यह रूढ़िवादी काव्यशास्त्र को चुनौती देते हुए नई अभिव्यक्तियों और नई सोच को जन्म देता है।
स्वच्छन्दतावाद का उद्भव
स्वच्छन्दतावाद का उद्भव किसी एक देश या क्षण विशेष का परिणाम नहीं था, बल्कि यह यूरोप में घटित व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तनों की संयुक्त देन था।
राजनीतिक कारण
1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने “स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व” का उद्घोष कर पूरे यूरोप में नई चेतना का संचार किया। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को साहित्यिक चिन्तन का केन्द्र बनाया गया। कवियों और लेखकों ने राजनीतिक बन्धनों के विरोध तथा मानवाधिकारों की उद्घोषणा को अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया।
सामाजिक कारण
औद्योगिक क्रान्ति ने कृषि-प्रधान और सामन्ती समाज व्यवस्था को झकझोरकर पूँजीवाद को जन्म दिया। यद्यपि इस व्यवस्था ने शोषण को बढ़ावा दिया, परन्तु इसी ने व्यक्ति की आकांक्षाओं और स्वतंत्रता की चेतना को भी बल दिया। इस नई सामाजिक परिस्थिति ने साहित्यकारों को पुराने ढाँचे से बाहर निकलकर नवीन दृष्टिकोण अपनाने और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया।
धार्मिक कारण
इस काल में चर्च और परम्परागत आडम्बरों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। लोग ईश्वर को केवल कठोर दैवी सत्ता के रूप में न देखकर उसे मानवीय भावनाओं और करुणा से जोड़ने लगे। धर्म की इस मानवीय व्याख्या ने साहित्य को गहन भावनात्मकता, संवेदनशीलता और करुणा से ओत-प्रोत किया।
दार्शनिक कारण
दार्शनिक स्तर पर ज्यां जाक रूसो ने उद्घोष किया – “मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, परन्तु हर जगह बन्धनों में जकड़ा है।” उन्होंने ‘प्रकृति की ओर लौट चलो’ का आह्वान किया, जिससे साहित्यकारों को कृत्रिमता और रूढ़िवाद से मुक्त होकर प्रकृति, भावनाओं और व्यक्तित्व की खोज की प्रेरणा मिली।
स्वच्छन्दतावाद की विशेषताएँ
स्वच्छन्दतावाद (Romanticism) साहित्य का वह प्रवाह है जिसमें मानवीय आत्मा की स्वतंत्रता, प्रकृति के साथ गहन तादात्म्य और भावनाओं की उन्मुक्त अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से विद्यमान है। यह केवल साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने परम्परागत रूढ़ियों को तोड़कर भावनाओं, कल्पना और सौन्दर्य की नई व्याख्या प्रस्तुत की। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित रूप में देखी जा सकती हैं—
1. भाव-प्रवणता
स्वच्छन्दतावादी साहित्यकारों ने भावनाओं और अनुभूतियों को सर्वोपरि स्थान दिया। वर्ड्सवर्थ ने कविता को “भावों का सहज उच्छलन” कहा और शेली ने भी अपनी रचनाओं में भावोद्गारों की प्रचुरता दिखाई। हिन्दी में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की रचनाओं में भाव-प्रवणता के कोमल एवं गहन स्वर सहज ही मिलते हैं।
2. व्यक्तिवाद और आत्मनिष्ठा
इस आंदोलन ने व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना और उसकी आत्मानुभूतियों को केंद्र में रखा। निराशा, विषाद और भावुकता की गहन अभिव्यक्ति व्यक्तिवाद के रूप में सामने आई। निराला की अनामिका और प्रसाद की आँसू इस प्रवृत्ति की सशक्त मिसाल हैं।
3. कल्पना की प्रधानता
स्वच्छन्दतावादी रचनाकारों ने कल्पना को काव्य का प्राण माना। कल्पना के माध्यम से उन्होंने भावों को ऐश्वर्य और सौन्दर्य प्रदान किया। परिणामस्वरूप रचनाओं में रहस्य और दुरूहता का भी समावेश हुआ। विलियम ब्लेक कल्पना को चिरंतन सत्य मानते थे, और हिन्दी छायावादी कवियों ने भी इसी प्रवृत्ति को अपनाया।
4. अतीत के प्रति अनुराग
स्वच्छन्दतावादियों के लिए वास्तविक जगत से अधिक आकर्षक अतीत और अज्ञात लोक रहा। वे स्वर्णिम अतीत और सुमधुर भविष्य की कल्पना में रमकर काव्य रचते थे। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली और कीट्स की रचनाओं में यह प्रवृत्ति स्पष्ट है। हिन्दी में प्रसाद के साहित्य में अतीत की स्मृतियों और गौरव का गहरा अनुराग दृष्टिगोचर होता है।
5. सौन्दर्य-दृष्टि
स्वच्छन्दतावाद का मूल स्वभाव सौन्दर्य की खोज है। शेली सम्पूर्ण प्रकृति को सौन्दर्य से आलोकित मानते हैं, जबकि कीट्स ने सौन्दर्य को “सत्य” का रूप माना। हिन्दी छायावादी कवियों—प्रसाद और पन्त—की रचनाएँ सौन्दर्य-बोध की गहन अभिव्यक्ति से परिपूर्ण हैं।
6. प्रकृति-प्रेम
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकृति को केवल दृश्य-पटभूमि न मानकर सचेतन सत्ता के रूप में चित्रित किया। उनके लिए प्रकृति ही विश्वात्मा है। वर्ड्सवर्थ और शेली ने प्रकृति के प्रति अद्वितीय अनुराग दिखाया, जबकि हिन्दी में पन्त को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा ने भी प्रकृति का बहुविध और बहुरंगी चित्रण किया।
7. निराशावादी प्रवृत्ति
स्वच्छन्दतावादियों की रचनाओं में अक्सर जीवन और युग की विषमताओं से उपजा विषाद झलकता है। शेली और कीट्स के काव्य में यह भाव प्रमुख है। हिन्दी में प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्ति “ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे-धीरे” इस प्रवृत्ति का उत्तम उदाहरण है।
8. मानवतावादी दृष्टिकोण और राष्ट्रप्रेम
स्वच्छन्दतावाद केवल आत्माभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने मानवता और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी पोषित किया। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना इस विचारधारा में अन्तर्निहित है। वर्ड्सवर्थ और प्रसाद की रचनाओं में यह दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
9. नवीन अभिव्यंजना
स्वच्छन्दतावादियों ने शास्त्रीय रूढ़ियों और प्राचीन परम्पराओं को अस्वीकार कर अभिव्यक्ति में नवीनता और स्वच्छन्दता को अपनाया। काव्य की भाषा, विषय-वस्तु और शिल्प—तीनों में उन्होंने नये दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।
10. विराट् और रहस्य की ओर आकर्षण
स्वच्छन्दतावादी कवि प्रकृति और जीवन के विराट पक्ष को उद्घाटित करते हैं। उनकी रचनाओं में रहस्यवाद, आध्यात्मिकता और अनन्त की खोज प्रमुख रूप से उपस्थित है। प्रसाद की कामायनी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।
निष्कर्ष
स्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावाद केवल साहित्यिक आंदोलन नहीं, बल्कि भावनाओं और विचारों की क्रान्तिकारी धारा थी। इसने रूढ़िबद्ध शास्त्रीयता को अस्वीकार कर स्वतंत्रता, कल्पना और सौन्दर्य को नई ऊँचाइयाँ दीं। हिन्दी का सम्पूर्ण छायावादी साहित्य इस धारा से प्रभावित है। स्वच्छन्दतावाद ने कला, संगीत, दर्शन और राजनीति तक को प्रभावित किया और आज भी यह स्वतंत्र सृजन और कल्पना की प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
स्वच्छन्दतावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
1. आत्मकेन्द्रिकता और व्यक्तिपरकता
स्वच्छन्दतावाद का मूल आधार व्यक्ति की आंतरिक चेतना और आत्मानुभूतियों पर टिका है। इस धारा के कवि और साहित्यकार बाह्य जगत से अधिक अपनी अंतरात्मा की ओर उन्मुख रहते हैं। वे अपने सुख-दुःख, आशा-निराशा और अनुभूतियों को ही काव्य का केन्द्र बनाते हैं।
2. साहित्यिक रूढ़ियों का विरोध
स्वच्छन्दतावाद का जन्म परम्परागत शास्त्रीयता और बंधनकारी साहित्यिक रूढ़ियों के विरुद्ध हुआ। इस प्रवृत्ति ने पूर्व निर्धारित नियमों, अलंकारों और परम्परागत विषयों को अस्वीकार कर स्वतंत्र अभिव्यक्ति और नवीन प्रयोगों को बढ़ावा दिया।
3. व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा
इस आंदोलन में व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी स्वतंत्र सत्ता को सर्वोपरि माना गया। प्रत्येक कवि अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता को उद्घाटित करता है। इसीलिए स्वच्छन्दतावादी साहित्य में आत्मनिष्ठ भावनाएँ, वैयक्तिक अनुभूतियाँ और गहन व्यक्तित्व-चेतना प्रबल दिखाई देती हैं।
4. प्रकृति और रहस्य के प्रति गहन आकर्षण
स्वच्छन्दतावादियों के लिए प्रकृति केवल सौन्दर्य का साधन नहीं, बल्कि जीवंत सत्ता और रहस्यमयी शक्ति है। वे प्रकृति में आत्मा का स्पन्दन खोजते हैं और रहस्यमय जगत की ओर आकर्षित होते हैं। इस दृष्टि से उनके साहित्य में आध्यात्मिकता और रहस्य-बोध गहराई से उपस्थित है।
5. वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति
स्वच्छन्दतावादी साहित्य में कवि अपनी निजी अनुभूतियों और हृदय की गहराइयों को अत्यन्त सहज और भावपूर्ण रूप से व्यक्त करता है। यही कारण है कि इस धारा के काव्य में गहन भावुकता, आत्मनिष्ठता और वैयक्तिक संवेदनाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है।
हिन्दी साहित्य में महत्व
स्वच्छन्दतावाद ने हिन्दी साहित्य को नई चेतना प्रदान की। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह प्रवृत्ति द्विवेदी युग से प्रारम्भ होकर छायावाद में विकसित हुई। इस धारा ने साहित्य में वैयक्तिकता, भावुकता और आत्मानुभूति को स्थान दिया।
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने पहली बार जगत की सच्चाई और व्यक्तिगत जीवन के मूल्यों को प्रतिष्ठा दी। यही कारण है कि स्वच्छन्दतावाद ने न केवल हिन्दी काव्यधारा को नवीन दृष्टिकोण दिया, बल्कि साहित्य को मानवीय संवेदनाओं से भी अधिक निकट बना दिया।
स्वच्छन्दतावाद के स्वरूप
- भावना और व्यक्तिवाद पर जोर
ज्ञानोदय के तर्कप्रधान दृष्टिकोण के विपरीत स्वच्छन्दतावाद ने भावनाओं, अंतर्ज्ञान और वैयक्तिक अनुभवों को महत्व दिया। इस धारा के कवियों ने व्यक्ति के निजी जीवन, उसकी आशाओं, आकांक्षाओं और विषाद को ही काव्य का केन्द्र बनाया। - कल्पना की प्रधानता
स्वच्छन्दतावादी रचनाकारों ने कल्पना को सृजन का आधार माना। कल्पना के सहारे वे वास्तविकता से परे जाकर आदर्श, रहस्य और सौन्दर्य से सम्पन्न लोक का निर्माण करते हैं। - प्रकृति का महिमामंडन
प्रकृति को उन्होंने केवल दृश्य-पटभूमि न मानकर एक जीवंत सत्ता के रूप में चित्रित किया। उसकी उदात्तता, सौन्दर्य और रहस्य के प्रति उन्होंने गहन आकर्षण प्रकट किया। वर्ड्सवर्थ ने तो प्रकृति को शिक्षक और मार्गदर्शक तक मान लिया। - अतीत के प्रति अनुराग
स्वच्छन्दतावादियों ने मध्यकालीन जीवन, संस्कृति और गौरवपूर्ण अतीत की ओर आकर्षण प्रकट किया। इतिहास और मिथक उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। - रचनात्मक स्वतंत्रता
स्वच्छन्दतावाद ने शास्त्रीय रूढ़ियों और निर्धारित नियमों को अस्वीकार कर दिया। कवियों और कलाकारों ने अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त किया, जिससे साहित्य और कला में नवीनता आई। - मानवीय अनुभव की गहराई
इस आंदोलन ने प्रेम, करुणा, वीरता, विषाद और आशा जैसे गहन मानवीय अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इसमें मानव और प्रकृति के बीच आत्मीय सम्बन्ध को भी रेखांकित किया गया। - जन-साधारण से जुड़ाव
स्वच्छन्दतावादी साहित्यकारों ने साहित्य को केवल उच्च वर्ग की बपौती न मानकर सामान्य जन-जीवन की भावनाओं और संवेदनाओं से जोड़ा। इस प्रकार साहित्य अधिक मानवीय और सार्वभौमिक बना।
निष्कर्ष
संक्षेप में, स्वच्छन्दतावाद वह आंदोलन था जिसने कठोर तर्कवाद के स्थान पर भावनाओं को महत्व दिया, शास्त्रीय रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित किया, और प्रकृति व मानवीय अनुभवों के सौन्दर्य को नये आयाम प्रदान किए। इस आंदोलन ने न केवल 18वीं–19वीं शताब्दी के साहित्य और कला को प्रभावित किया, बल्कि आज भी यह कलाकारों, कवियों और चिन्तकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
इसे भी पढ़ें :
- लेखन कौशल (Writing Skill in Hindi): अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषताएं, विधियां, उद्देश्य, उपयोगिता, प्रकार
- स्तंभ लेखन क्या है पत्रकारिता में स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य है (Stambh yojna kya hai)
- फीचर लेखन के कितने प्रकार है(feature lekhan ke prakar)- परिभाषा,स्वरूप, तत्व, उद्देश्य
- समाचार लेखन के तत्व और समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं
- अनुच्छेद लेखन
- प्रयोगवाद की विशेषताएं: परिचय, अर्थ, पृष्ठभूमि, उदय और कारण, नामकरण, स्वरूप, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, समय सीमा
- छायावाद की विशेषताएं लिखिए: अर्थ, उद्भव और विकास, समय सीमा, महत्व,प्रमुख विशेषताएँ, पृष्ठभूमि, चार स्तंभ
- प्रगतिवाद की विशेषताएं, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ