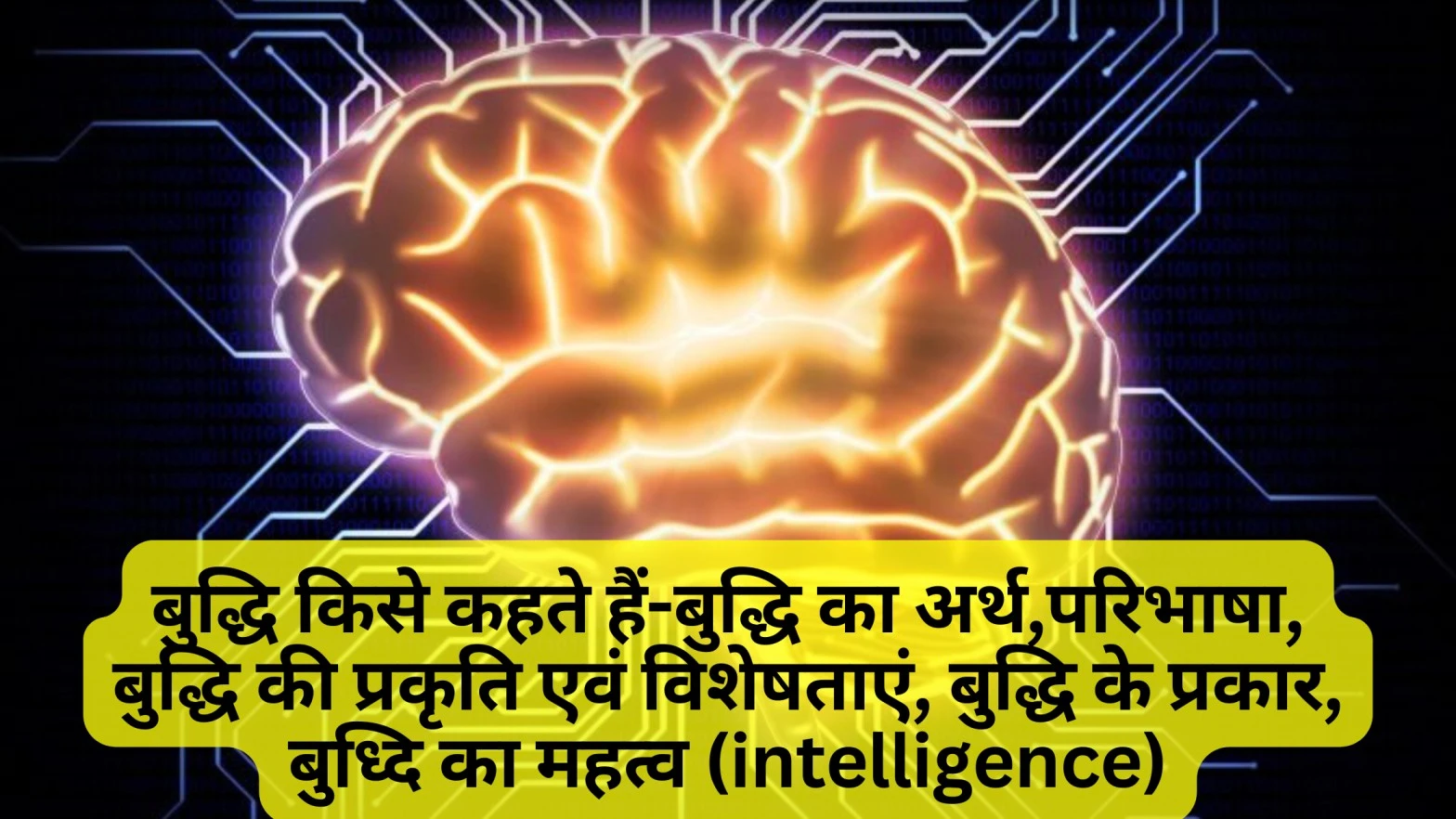बुद्धि किसे कहते हैं-बुद्धि का अर्थ,परिभाषा, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार (intelligence)
बुद्धि किसे कहते हैं(buddhi kise kahate hain)
बुद्धि व्यक्ति की वह सर्वभौम शक्ति है जो उसे ध्येय युक्ति कार्य करने तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता देती है।
जो व्यक्ति जितना अधिक चतुराई से समस्या का समाधान निकाल लेता है और संकट में नहीं पड़ता वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि मिली है। यह जन्मजात क्षमता है इसका विकास वातावरण में होता है।
अतः बुद्धि व्यक्ति की क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है। वह वातावरण तथा परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता। वह स्वयं को समायोजित करता है या स्वयं वातावरण के अनुकूल बन जाता है।
बुद्धि का अर्थ(meaning of intelligence in hindi)
बुद्धि का अंग्रेजी रूपांतरण है intelligence। Intelligence शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों पहला Inter और दूसरा Legere ।
बुद्धि सामान्य शब्द है। जिसका अर्थ गगन है। बुद्धि का अर्थ इतना व्यापक है कि इसका अर्थ प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक संदर्भ में इसका अर्थ बदल जाता है।
कुछ लोग बुद्धि को समायोजन की क्षमता मानते हैं। समायोजन करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो समायोजन के व्यवहार का निर्धारण करती है।
सीखने की क्षमता तथा अमूर्त चिंतन को भी बुद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। जितनी शीघ्रता से, शुद्धता से बालक सिखता है वह उतना ही बुद्धिमान कहलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जितना अमूर्त चिंतन करता है उसे उन उपलब्धियों के कारण बुद्धिमानों की श्रेणी में रखा जाता है।
समस्या समाधान की दिशा में त्वरित निर्णय लेने वाला भी बुद्धिमान कहलाता है। जैसे तेनालीराम और बीरबल जैसे लोग विकट समस्याओं के सरल समाधान के कारण ही बुद्धिमानओं की श्रेणी में आते हैं।
📖 Read: बुद्धि के सिद्धांत
बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषा (definition of intelligence)
विभिन्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा अपने-अपने ढंग से की है उनका मूल विचार भी उसी प्रकार से हैं-
टर्मन (terman) के अनुसार:
एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है, जिस अनुपात में वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है।(an individual is intelligent in proprotion as he is able to carry on abstract thinking.)
स्पीयरमैन के अनुसार:
बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है।(intelligence is relational thinking.)
थार्नडाइक के अनुसार:
वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है।
एच.ई. गैरिट के अनुसार:
ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे अंक शब्द रेखा चित्र समीकरण और सूत्र ही बुद्धि है।
बिने तथा साइमन के अनुसार:
निर्णय सद्भावना उपकरण समझने की योग्यता उक्ति युक्त तर्क और वातावरण में अपनी को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है।
बुद्धि की प्रकृति बताइए, बुद्धि की विशेषताएं बताइए, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं(nature of intelligence in hindi)
उपर्युक्त परिभाषा ओं से स्पष्ट होता है कि बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषता निम्नलिखित है-
१. बुद्धि समायोजन की विशेषता है
२. बुद्धि अधिगम की योग्यता है
३. बुद्धि अमूर्त चिंतन है
४. बुद्धि समस्या समाधान है
५. मानसिक आयु पर बुद्धि
१. बुद्धि समायोजन की विशेषता है
अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वातावरण में अपने आप को समायोजित करना चाहता है लेकिन व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है अतः बुद्धि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को उस रूप में ढलने का प्रयास करता है या उस परिस्थिति से समायोजित होने का प्रयास करता है। समायोजन की क्षमता ही व्यक्ति की बुद्धि की विशेषता होती है। जिस व्यक्ति का दिमाग या बुद्धि उस परिस्थिति को जिस तरह से हल करने में यह समाधान करने में सक्षम होता है उस व्यक्ति का बुद्धि भी उसी प्रकार से कार्य करता है।
२. बुद्धि अधिगम की योग्यता है
बुद्धि का यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्ति किसी कार्य कौशल को किस सीमा तक तथा कितने समय में सीखता है या उसे पूरा कर पाता है। सीखने की मात्रा की अधिकता तथा सीखने में लगने वाला समय की बुद्धि की विशेषता होती है जो व्यक्ति किसी भी कार्य को जितनी तेजी से करता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेजी से काम करता है तथा जो व्यक्ति किसी भी कार्य को सीखने या करने में बहुत अधिक समय लगाता है तो वह व्यक्ति एक तो मन बुद्धि होगा या विशिष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति होगा जिस कारण से उसके सीखने की गति में प्रभाव पड़ती है।
३. बुद्धि अमूर्त चिंतन है
हर मनुष्य किसी भी काम को सोच विचार कर या चिंतन मनन करके ही करता है यह मनुष्य की एक विशेषता है जो अन्य प्राणी में नहीं पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले उसे अमूर्त रूप से या गहराई से सोच विचार या चिंतन मनन करके ही करता है। चिंतन स्वयं में अमूर्त है परंतु या अमूर्त चिंतन कालांतर में अन्य कार्यों को संपन्न करने में योग देता है। उसी प्रकार बुद्धि भी एक अमूर्त चिंतन ही है।
४. बुद्धि समस्या समाधान है।
हर व्यक्ति के सामने हर प्रकार की समस्या है किसी ना किसी वक्त खड़ी हो ही जाती है जिसका समाधान मनुष्य ढूंढने लगता है। बुद्धि की एक विशेषता है समस्याओं का समाधान ढूंढना। समस्या जितनी जटिल होगी या कठिन होगी समाधान में उतना ही अधिक समय लगेगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जितना अधिक होगा वह उसी तेजी से उस समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। समस्या का समाधान मिल जाने पर व्यक्ति को अपार संतुष्टि मिलती है।
५. मानसिक आयु पर बुद्धि
बुद्धि की और एक विशेषता है कि बुद्धि मानसिक आयु पर भी निर्भर होती है। एक छोटा सा बालक किसी भी समस्या को अपने उम्र या अपनी मानसिकता के दायरे में रहकर ही सोच सकता है तथा उसका समाधान कर सकता है जैसे-जैसे बड़ा होता है उनकी मानसिक आयु बड़ी होती जाती है तथा उनके सोचने समझने तथा कार्य करने और समस्या समाधान करने की गति में तीव्रता देखी जाती हैं अतः बुद्धि मानसिक आयु पर भी निर्भर होती है।
बुद्धि के प्रकार का वर्णन कीजिए, बुद्धि के प्रकार बताइए, buddhi ke prakar kitne hain,intelligence ke prakar, इंटेलिजेंस के प्रकार (types of intelligence)
थार्नडाइक ने बुद्धि को तीन भागों में बांटा है-
१. अमूर्त बुद्धि (Abstract intelligence)
२. मूर्त बुद्धि (Concrete intelligence)
३. सामाजिक बुद्धि (Social intelligence)
१. अमूर्त बुद्धि (Abstract intelligence)
अमूर्त बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों को चिंतन तथा मनन के माध्यम से हल करना है। समस्याओं तथा अनुभव की प्रतिमाओं को अधिकाधिक स्पष्ट करने के लिए अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। कवि साहित्यकार चित्रकार आदि अपनी भावनाओं को अमूर्त बुद्धि के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। अमूर्त बुद्धि में शब्द अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया जाता है या पठन की सीखने की प्रक्रिया है, उन समस्याओं को हल करने की भी प्रक्रिया है जिनमें शब्द या प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए शब्द एवं प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कला अमूर्त या मौखिक बुद्धि की देन है। विद्यालय में पठन गणित भूगोल इतिहास एवं ऐसी ही विषयों में सफलता केले अमूर्त बुद्धि का विकास करना आवश्यक हो जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने अमूर्त बुद्धि के क्षमता के अनुसार ही किसी भी वस्तु को पहचानता व उसे समझता है यह व्यक्ति की बुद्धिमानी का निशानी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को किस प्रकार से ग्रहण करता है या उसे सीखता है।
अमूर्त बुद्धि का परीक्षण तीन प्रकार से किया जा सकता है
i. आकांक्षा का स्तर: व्यक्ति की आकांक्षा के स्तर का मापन करने से हमें उस व्यक्ति की अमूर्त बुद्धि का पता चलता है। जिस व्यक्ति को आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा उसकी अमूर्त बुद्धि भी उतनी ही तीव्र होगी।
ii. विभिन्न प्रकार के कार्य करने से: जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करता है या अनेकों प्रकार के कार्यकर्ता है उनके कार्य करने की क्षमता से अमूर्त बुद्धि का पता लगाया जा सकता है।
iii. कार्य करने की गति से: जो व्यक्ति अमूर्त कार्यों को जितना अधिक गति से करता है उसकी अमूर्त बुद्धि उसी के अनुसार कम या अधिक होगी।
२. मूर्त बुद्धि (Concrete intelligence)
मूर्त का अर्थ होता है समक्ष या सामने। किसी भी वस्तु को देखकर उसे समझने और उनके अनुरूप क्रिया करने में मूर्त बुद्धि का उपयोग किया जाता है। इसको यांत्रिक (mechanical) या गत्यात्मक (motor) भी कहा जाता है। इस प्रकार की बुद्धि उन परिस्थितियों में कार्य करते हैं जिम्मी वस्तु या उद्देश्य निहित हो होता है जैसे कारपेंटर का काम, मिस्त्रीगिरी का काम, मशीनों का काम, आदि यंत्रों से संबंधित काम इसी प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति ऑन समस्याओं को शीघ्र हल कर लेता है जिसमें मूर्त वस्तुओं को पहचानने की शक्ति हो।
मूर्त बुद्धि का दूसरा स्वरूप शिक्षा में भी देखा जा सकता है। इसमें गत्यात्मक योग्यता (motor ability) निहित रहते हैं। नृत्य, खेल तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों में यह बुद्धि निहित होती है।
३. सामाजिक बुद्धि (Social intelligence)
सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य है कि जो जिस व्यक्ति में यह शक्ति होती है कि किस प्रकार से समाज में समायोजन करने की क्षमता उत्पन्न कर सकती हैं? सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति को समाज में संबंध बनाने में यह बुद्धि योग्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत व्यवहार कौशल आता है। व्यवहार कौशल के साथ व्यक्तित्व एवं चरित्र के गुण निहित होते हैं स्वभाव मन स्थिति मनोवृति ईमानदारी निर्णय हास्य स्वभाव आधिकारिक समाजिक बुद्धि की ओर संकेत करते हैं।
बहुत से व्यक्ति असामाजिक या सामाजिक बुद्धि ना होने के कारण अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। सामान्यता अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि साथ साथ चलती है। नेतागण इसी बुद्धि के उपयोग से जन जीवन में लोकप्रिय होकर प्रतिनिधि बन जाते हैं।
तो दोस्तों आज आपने इस लेख में पढ़ा कि बुद्धि किसे कहते हैं,बुद्धि का अर्थ,बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषा (definition of intelligence),बुद्धि की प्रकृति बताइए, बुद्धि की विशेषताएं बताइए, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं(nature of intelligence in hindi),बुद्धि के प्रकार बताइए, buddhi ke prakar kitne hain,intelligence ke prakar, इंटेलिजेंस के प्रकार (types of intelligence) यह लेख आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए तथा इससे संबंधित और भी जानकारी देना चाहते हैं तो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइए।
Also Read: बुद्धि के सिद्धांत का वर्णन करें buddhi ke siddhant ka varnan karen
बुद्धि को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक (Factors Determining Intelligence in Hindi)
बुद्धि एक जटिल मानसिक गुण है, जो किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और नई जानकारियों को आत्मसात करने की क्षमता को दर्शाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या बुद्धि जन्मजात होती है या यह अर्जित की जाती है? यह प्रश्न लंबे समय से मनोवैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय रहा है।
मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह विवाद “प्रकृति बनाम पोषण” (Nature vs. Nurture Controversy) के नाम से जाना जाता है। एक पक्ष का मानना है कि बुद्धि मुख्यतः वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, जबकि दूसरा पक्ष इसे वातावरण से प्रभावित मानता है। आधुनिक अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि बुद्धि का निर्धारण केवल किसी एक तत्व से नहीं, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर क्रिया से होता है।
1. वंशानुक्रम (Heredity) और बुद्धि
वंशानुक्रम का अर्थ है माता-पिता से संतानों को मिलने वाले आनुवंशिक गुण। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने के लिए गहन अध्ययन किए हैं कि बुद्धि का एक बड़ा भाग अनुवांशिक रूप से नियंत्रित होता है।
महत्वपूर्ण शोध और निष्कर्ष:
- सर फ्रांसिस गाल्टन (Sir Francis Galton) ने पाया कि उच्च बुद्धि कुछ खास कुलों तक सीमित रहती है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है।
- टरमैन (Terman) और गोडार्ड (Goddard) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने जुड़वाँ बच्चों और परिवारों पर अध्ययन कर इस सिद्धांत को समर्थन दिया।
- आर्थर जेनसेन (Arthur Jensen) ने 1966 में कहा कि व्यक्ति की बुद्धिलब्धि (IQ) का 75% से 80% तक भाग आनुवंशिक कारणों से निर्धारित होता है, और केवल 20-25% ही पर्यावरण पर निर्भर करता है।
प्रमुख तथ्य:
- आनुवंशिक रूप से मेधा से युक्त माता-पिता के संतान में बुद्धि का स्तर प्रायः उच्च होता है।
- जैविक संरचना और मस्तिष्क की बनावट भी बुद्धि पर असर डालती है।
2. वातावरण (Environment) और बुद्धि
वातावरण का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति किस सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और पारिवारिक परिवेश में पलता-बढ़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बुद्धि केवल जन्मजात नहीं होती, बल्कि प्रभावी वातावरण द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण शोध:
- विलियम्स, ब्लूम (Benjamin Bloom), कार्ल ब्राइटर, और क्लार्क एंड क्लार्क जैसे शोधकर्ताओं ने कहा कि अनुकूल वातावरण में बच्चों की मानसिक क्षमताएँ अत्यधिक विकसित होती हैं।
- शोधों से यह भी सिद्ध हुआ कि जन्म से लेकर चार वर्ष की आयु तक का समय बुद्धि विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है।
प्रमुख तथ्य:
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, सामाजिक संपर्क और प्रेरणा भरे वातावरण से बुद्धि में वृद्धि होती है।
- विपरीत रूप से, गरीबी, उपेक्षा, तनाव और सामाजिक अव्यवस्था जैसे नकारात्मक कारक बुद्धि के विकास को बाधित करते हैं।
3. वंशानुक्रम और वातावरण की अन्तर्क्रिया (Heredity-Environment Interaction)
अनेक मनोवैज्ञानिक अब इस बात पर सहमत हैं कि बुद्धि का विकास एकमात्र वंशानुक्रम या वातावरण से नहीं, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया से होता है।
मूल अवधारणा:
वंशानुगत तत्व व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता का बीज बोते हैं।
वातावरण उस बीज को सिंचित करता है और उसकी वृद्धि में सहायक बनता है।
उदाहरण:
यदि कोई बालक जन्म से ही उच्च बौद्धिक क्षमता लेकर आया है लेकिन उसे पोषणहीन, हिंसात्मक या अशिक्षित वातावरण में पाला गया, तो उसकी क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगी।
वहीं, एक सामान्य बौद्धिक स्तर वाला बालक यदि प्रोत्साहित करने वाले वातावरण में पले, तो उसमें असाधारण बुद्धि विकसित हो सकती है।
निष्कर्ष:
“बुद्धि का विकास एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें वंशानुक्रम में हैं और शाखाएँ वातावरण से सिंचित होती हैं।”
बुद्धि का महत्त्व
बुद्धि का महत्त्व हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह केवल पढ़ाई-लिखाई या तर्क-वितर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे निर्णय लेने, व्यवहार, समस्या समाधान और जीवन को सही दिशा देने में भी बुद्धि की अहम भूमिका होती है। नीचे बुद्धि के महत्त्व को विस्तार से बताया गया है:
1. निर्णय लेने में सहायक (Helpful in Decision-Making)
बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग तब होता है जब व्यक्ति को किसी जटिल या चुनौतीपूर्ण स्थिति में सही निर्णय लेना होता है।
बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को जल्दबाज़ी या भावनाओं में बहकर नहीं देखता, बल्कि उस स्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है।
वह प्रत्येक पक्ष और परिणाम को सोचता है, तथ्यों पर विचार करता है और फिर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेता है।
ऐसा निर्णय न केवल तत्काल समस्या का समाधान करता है, बल्कि भविष्य में भी लाभदायक सिद्ध होता है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कौन-सी बात कब और कैसे कहनी है, किस अवसर पर कौन-सा कार्य करना चाहिए और कब चुप रहना ज़्यादा हितकर होता है।
2. समस्याओं का समाधान (Solving Problems Effectively)
जीवन में समस्याएँ आना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धि हमें इन समस्याओं का समाधान खोजने की शक्ति देती है।
जब जीवन में कोई संकट या चुनौती आती है, तो बुद्धिमत्ता ही हमें घबराने से रोकती है और समाधान की दिशा में सोचने को प्रेरित करती है।
बुद्धिमान व्यक्ति विकल्पों का विश्लेषण करता है, संभावनाओं पर विचार करता है और किसी भी कठिन परिस्थिति को सरलता से सुलझा लेता है।
वह नकारात्मक सोच के स्थान पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे जीवन में नई राहें खुलती हैं।
3. संबंधों को सुधारने में मददगार (Strengthens Relationships)
आज के समय में सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है।
बुद्धि से सम्पन्न व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने, उनके दृष्टिकोण को अपनाने और अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता रखता है।
ऐसा व्यक्ति संवाद करते समय मर्यादा और संयम का पालन करता है, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता।
वह जानता है कि कब समझाना है और कब समझना है। इसी कारणवश उसके संबंध मधुर और स्थायी बने रहते हैं।
बुद्धिमत्ता से ही हम सहानुभूति, सहयोग और सामंजस्य जैसे गुणों को अपनाते हैं।
4. समाज में सम्मान (Social Recognition and Respect)
जिस व्यक्ति में सही निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहारिक सोच, संतुलन और विवेक होता है, वह समाज में एक आदर्श बन जाता है।
बुद्धिमान व्यक्ति की बातें लोग ध्यान से सुनते हैं, उसकी सलाह को महत्व देते हैं और उसकी उपस्थिति को सम्मानित करते हैं।
वह अपने ज्ञान और अनुभव से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
ऐसे व्यक्ति को नेता, मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में देखा जाता है।
इस तरह बुद्धि केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आधार बनती है।
5. जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति (Guiding Force in Life)
बुद्धि व्यक्ति को यह समझने की क्षमता देती है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं।
कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है।
ऐसे में बुद्धिमत्ता ही हमें भटकने से रोकती है और उचित मार्ग पर ले जाती है।
बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्तियों और सीमाओं को पहचानता है। वह अपने सपनों की पूर्ति के लिए योजना बनाता है, और बिना विचलित हुए उस पर कार्य करता है।
बुद्धि हमें लक्ष्य की ओर ले जाने वाली दिशा सूचक शक्ति की तरह कार्य करती है।
6. नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक (Essential for Moral and Spiritual Growth)
बुद्धि का उपयोग केवल भौतिक प्रगति के लिए नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाती है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि जीवन केवल पैसा कमाने या ऐशोआराम के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, सेवा, और धर्म का पालन करना भी जरूरी है।
बुद्धि व्यक्ति को लोभ, क्रोध, मोह जैसे दोषों से बचाती है और उसे संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है।
वह धर्म, सत्य, करुणा और परोपकार जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाता है, जिससे उसका आत्मविकास होता है और उसे आंतरिक शांति प्राप्त होती है।
बुद्धिमत्ता ही हमें मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करती है – यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में बुद्धि को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया है।
Very Important notes for B.ed.: बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव(balak par vatavaran ka prabhav) II sarva shiksha abhiyan (सर्वशिक्षा अभियान) school chale hum abhiyan II शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक II किशोरावस्था को तनाव तूफान तथा संघर्ष का काल क्यों कहा जाता है II जेंडर शिक्षा में संस्कृति की भूमिका (gender shiksha mein sanskriti ki bhumika) II मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, maslow hierarchy of needs theory in hindi II थार्नडाइक के अधिगम के नियम(thorndike lows of learning in hindi) II थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत(thorndike theory of learning in hindi ) II स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार , जीवन दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, आधारभूत सिद्धांत II महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शैक्षिक चिंतान एवं सिद्धांत II