कबीरदास का जीवन परिचय ॥ Kabir Das Ka Jivan Parichay
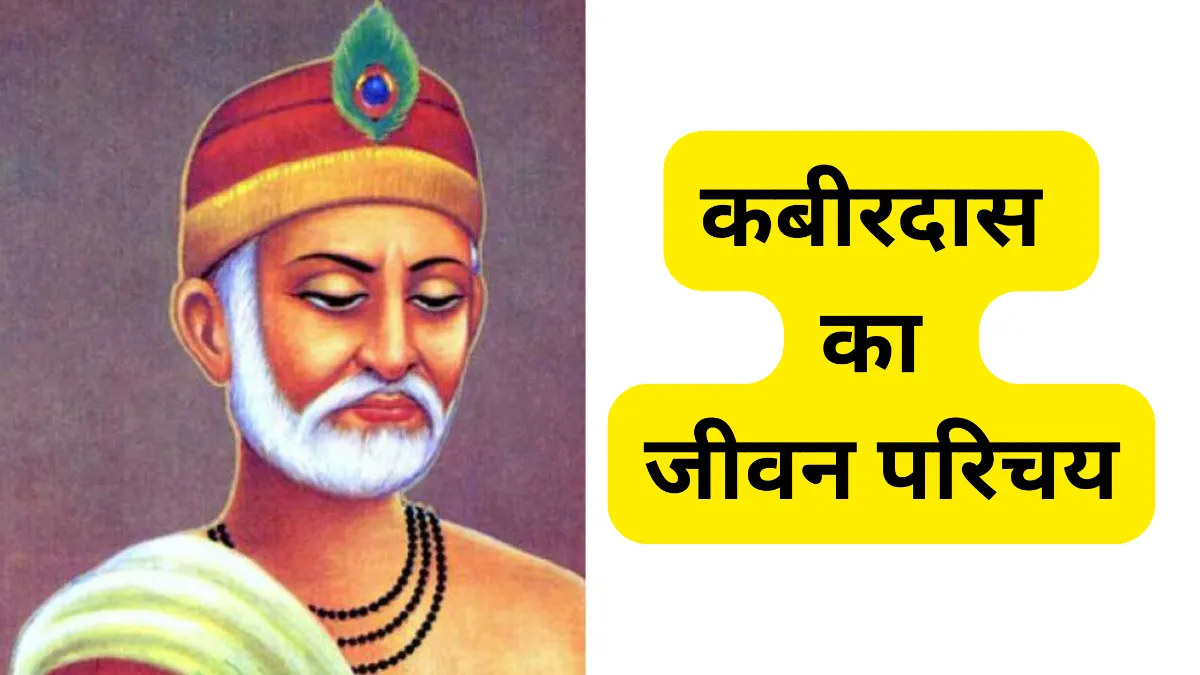
कबीरदास का जीवन प्रेरणा, साधना और समाज सुधार की मिसाल है, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को नया दृष्टिकोण दिया और निर्गुण भक्ति के माध्यम से लोकमानस को जागृत किया।
जन्म एवं परिवेश
कबीरदास का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी (वाराणसी) के निकट लहरतारा तालाब के पास हुआ था। उनके जन्म और माता-पिता के विषय में मतभेद हैं, किंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि उनका पालन-पोषण मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरु और नीमा ने किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे जन्म से ब्राह्मण विधवा की संतान थे, जिन्हें लोक-लाज के कारण छोड़ दिया गया और बाद में नीरु-नीमा ने उन्हें आश्रय दिया। उनका बचपन अत्यंत सादगी में बीता। वे जुलाहे का काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके दो संतानें—पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थीं। कबीरदास ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, किंतु साधु-संतों की संगति, सत्संग और तपस्या से जीवन का गहरा ज्ञान अर्जित किया। वे स्वयं कहते हैं—”मसि कागद छुओ नहीं, कमल गहि नहिं हाथ, पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय”।
शिक्षा एवं गुरु
कबीरदास ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किंतु साधु-संतों, फकीरों और सत्संग की संगति से उन्होंने गहन अध्ययन, अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। वे स्वयं कहते हैं—”मसि कागद छुओ नहीं, कमल गहि नहिं हाथ, पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय”। कबीरदास के गुरु रामानंद जी माने जाते हैं, जिनके सान्निध्य में उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और भक्ति की एक नई दृष्टि मिली। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब रामानंद जी घाट पर स्नान करने आए, तब बालक कबीर सीढ़ियों पर लेट गए; उनके स्पर्श से कबीर को ‘राम-नाम’ की दीक्षा मिली और रामानंद उनके गुरु बन गए। कबीर ने योग, साधना और सन्यास के क्षेत्र में गहरी खोज की और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बिना गुरु के जीवन अंधकारमय है—”गुरु बिना घोर अंधेरा, सब खोजन हार”। वेदांत, उपनिषद, योग और इस्लाम के सिद्धांतों की गहरी समझ रखते हुए भी उन्होंने कर्म, गृहस्थ जीवन और सत्य के मार्ग को सर्वोपरि माना।
समाज सुधारक और विचारक
कबीरदास अपने समय के श्रेष्ठ समाज सुधारक और विचारक थे जिन्होंने जातिप्रथा, छुआछूत, धर्मांधता, अंधविश्वास, मूर्तिपूजा और बाहरी आडंबर जैसी कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। वे स्पष्ट कहते हैं—”जाति-पाँति पूछे न कोई, हरि को भजै सो हरि का होई”। कबीर का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति कर्मकांड, पाखंड या संप्रदाय से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और सत्संग से होती है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों की सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार किया और सच्चे धर्म का मार्ग बताया। कबीरदास ने मानवता, सरलता, सत्य-बोध और करुणा को अपने उपदेशों का आधार बनाया। वे कर्मप्रधान समाज, व्यावहारिकता और पारिवारिक जीवन को सर्वोत्तम मानते थे। सन्यास और बाहरी दिखावे से दूर रहकर उन्होंने गृहस्थ जीवन की प्रतिष्ठा की और लोगों को प्रेम, एकता और मानव धर्म की ओर प्रेरित किया।
साहित्यिक योगदान
कबीरदास हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति काव्यधारा के महान कवि और संत माने जाते हैं। उन्होंने भक्तिकाल को नई दिशा दी और अपनी रचनाओं से समाज, धर्म, दर्शन, नीति, योग, आत्मज्ञान, प्रेम और मानवता जैसे विषयों को सरल ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख रचनाएँ साखी, सबद और रमैनी हैं। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी आदि लोकभाषाओं का मिश्रण थी, जिससे उनकी वाणी जनसामान्य के हृदय तक पहुँची। उनके दोहे जीवन-दर्शन, नीति और भक्ति का सार लिए हुए हैं और आज भी समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। उदाहरणस्वरूप—
- “बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर” - “पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय”
कबीरदास की वाणी केवल हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे गुरुग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला। उनकी शिक्षाओं के आधार पर कबीरपंथ नामक संप्रदाय की स्थापना हुई। उनके काव्य में गरीबी, योग, आत्मसंयम, प्रेम, कृपा, गुरु महिमा, धर्म, प्रकृति और समाज सुधार जैसे विविध विषयों की झलक मिलती है, जिससे उनका साहित्यिक योगदान अमर और सार्वकालिक हो गया।
धार्मिक सुधार और भक्ति
कबीरदास ने धार्मिक सुधार और भक्ति के क्षेत्र में महान कार्य किया। उन्होंने हिंदू-मुसलमान दोनों समुदायों की बाहरी पूजा-पद्धतियों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों और पाखंड का तीखा विरोध किया। कबीर का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति कर्मकांडों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और निर्मल हृदय से संभव है। वे स्पष्ट कहते हैं—”पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय; ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय”। इसी प्रकार वे दिखावे वाले भजन-पूजन की आलोचना करते हुए कहते हैं—”माला फेरै कर में, जीभ फेरै माउ, मनवा तो चहुं दिसि फेरै, यह तो सुमिरन नाउ”। कबीर निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाया। उनके उपदेशों का मुख्य उद्देश्य था—मानवता को जोड़ना, प्रेम, करुणा और समानता का संदेश फैलाना। उनकी शिक्षाओं के आधार पर कबीरपंथ नामक संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसने भक्ति और धार्मिक जागरण को भारत के विशाल समाज में फैलाया।
मृत्यु और काशी-मगहर विवाद
कबीरदास ने 1518 ईस्वी में मगहर (उत्तर प्रदेश) में देह त्याग किया। उस समय प्रचलित मान्यता थी कि काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है और मगहर में प्राण त्यागने पर नरक की प्राप्ति होती है। कबीरदास ने इस अंधविश्वास को तोड़ने और समाज को सत्य का संदेश देने के लिए काशी छोड़कर मगहर में मृत्यु स्वीकार की। उनके देहावसान के बाद हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच अंतिम संस्कार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। किंवदंती है कि जब उनके शव पर से चादर हटाई गई तो वहाँ फूलों का ढेर पाया गया। उन फूलों को दोनों समुदायों ने अपनी-अपनी परंपरा के अनुसार दफनाया और समाधि बनाई। इस प्रकार कबीरदास की मृत्यु ने न केवल धार्मिक आडंबरों को चुनौती दी, बल्कि उनकी विरासत को और भी अमर बना दिया।
मुख्य शिक्षाएँ और कहानियाँ
कबीरदास ने जीवनभर समाज को सत्य, अहिंसा, अनुशासन, गुरु की महिमा, व्यभिचार और छुआछूत का निषेध, कर्मप्रधानता तथा पारिवारिक जीवन की श्रेष्ठता जैसी शिक्षाएँ दीं। उनका स्पष्ट कहना था—”गुरु बिन जो दान करे, सो अंधा बकरी”, अर्थात् गुरु के बिना ज्ञान और कर्म अंधेरे में भटकने जैसा है। कबीरदास बुरे संस्कारों, लोभ-लालच और अवगुणों के प्रबल विरोधी थे। उनके जीवन की कई प्रेरक घटनाएँ आज भी लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। उदाहरणस्वरूप, जलेबी की कथा प्रसिद्ध है—एक बार उन्हें जलेबी खाने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु मन पर नियंत्रण का अभ्यास करते हुए उन्होंने उन्हें स्वयं न खाकर एक कुत्ते को दे दीं। इससे उन्होंने मन-विजय और इंद्रिय-नियंत्रण का संदेश दिया।
कबीरपंथ आज भी उनके विचारों और शिक्षाओं का अनुकरण करता है और यह सम्प्रदाय देश-विदेश में व्यापक रूप से फैला है। कबीरदास के अनुयायी उन्हें “पूर्ण ब्रह्म” और “सर्वसृष्टि रचनहार” मानते हैं। उनकी वाणी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और कई अन्य भाषाओं में प्रचलित होकर समाज को निरंतर प्रेरित कर रही है। इस प्रकार, कबीरदास की शिक्षाएँ और प्रेरक प्रसंग आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं।
निष्कर्ष
कबीरदास केवल एक संत या कवि ही नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक, युगद्रष्टा, निर्गुण भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक और मानवता के सच्चे मार्गदर्शक थे। उनके जीवन में साधना, भक्ति, प्रेम, समानता और सत्य की स्थायी प्रेरणा है। कबीर की वाणी, विचार और रचनाएँ आज भी समाज को दिशा, सत्य और प्रेम की राह दिखाती हैं। उनका जीवन संदेश स्पष्ट करता है—”जहाँ प्रेम है, वहाँ ईश्वर है”। हिंदी भक्तिकाल में उनके योगदान, समाज सुधार, धार्मिक जागरण और साहित्यिक सृजन ने उन्हें अमर कर दिया। कबीरदास का जीवन भारतीय समाज, साधना और साहित्य के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा, और उनके उपदेश, दोहे तथा जीवन-दृष्टि युग-युगान्तर तक स्मरणीय रहेंगे।
प्रमुख रचनाएँ और संक्षिप्त विवरण
कबीरदास की रचनाएँ भारतीय भक्ति आंदोलन और समाज सुधार में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएँ बीजक, साखी, सबद, रमैनी और उनके प्रसिद्ध दोहे हैं, जिनमें मानवता, प्रेम, भक्ति, नीति और जीवन-दर्शन की शिक्षाएँ निहित हैं।
प्रमुख रचनाएँ और संक्षिप्त विवरण
- बीजक: कबीर की सम्पूर्ण वाणी का प्रामाणिक संग्रह, जिसमें साखी, सबद और रमैनी तीनों भाग सम्मिलित हैं। इसमें लगभग 84 रमैनियाँ, 227 साखियाँ और 238 सबद हैं।
- साखी: दोहा शैली में लिखित, नैतिकता, जीवन-दर्शन, गुरु महिमा और आत्मशुद्धि पर आधारित शिक्षाप्रद रचनाएँ। उदाहरण:
“गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागूं पाँय।
बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाय।” - सबद: गीतात्मक पद, जिनमें प्रेम, भक्ति, साधना और आध्यात्मिक भावनाएँ प्रकट होती हैं; गेय स्वरूप में इनका अनुभव अधिक प्रभावशाली होता है।
- रमैनी: चौपाई छंद में रचित दार्शनिक, रहस्यवादी और समाज सुधारक रचनाएँ। इसमें जीवन, माया, ज्ञान, मुक्ति आदि विषयों का गहन विवेचन मिलता है।
- कबीर के दोहे और अन्य पद: नीति, धर्म, समाज, प्रेम, गुरु और जीवन-दर्शन पर आधारित छोटे-छोटे पद और दोहे। उदाहरण:
“बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर”
“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय” - अन्य रचनाएँ: “घूंघट के पट”, “हमन है इश्क मस्ताना”, “झीनी झीनी बीनी चदरिया”, “माया महा ठगिनी”, “मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में”, “मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे” आदि पद और अंग व साखियाँ।
कबीरदास की ये रचनाएँ आज भी भक्ति, समाज सुधार, जीवन-दर्शन और आत्मिक जागरण के प्रेरणास्रोत हैं। उनकी भाषा जन-भाषा, सधुक्कड़ी, अवधी, पंजाबी और भोजपुरी का मिश्रण है, जिससे उनकी वाणी आम जन तक सरलता से पहुँची और समाज में गहरा प्रभाव डाला।
इसे भी पढ़िए:
- डॉ. रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय ॥ Dr Ramkumar Verma Ka Jivan Parichay
- चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय ॥ Chandradhar Sharma Guleri Jivan Parichay
- गुणाकर मुले का जीवन परिचय ॥ Gunakar Muley Ka Jeevan Parichay
- यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय ॥ Yatindra Mishra Jeevan Parichay
- बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय (Balkrishna Bhatt ka jeevan parichay)
- राजा लक्ष्मण सिंह का जीवन परिचय (Raja lakshman singh ka jeevan parichay)
- राजा शिवप्रसाद ‘सितारेहिंद’ का जीवन परिचय (Raja shivprasad sitarehind ka jeevan parichay)
- तुलसीदास का जीवन परिचय tulsidas ka jivan parichay
- हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय harishankar parsai ka jivan parichay