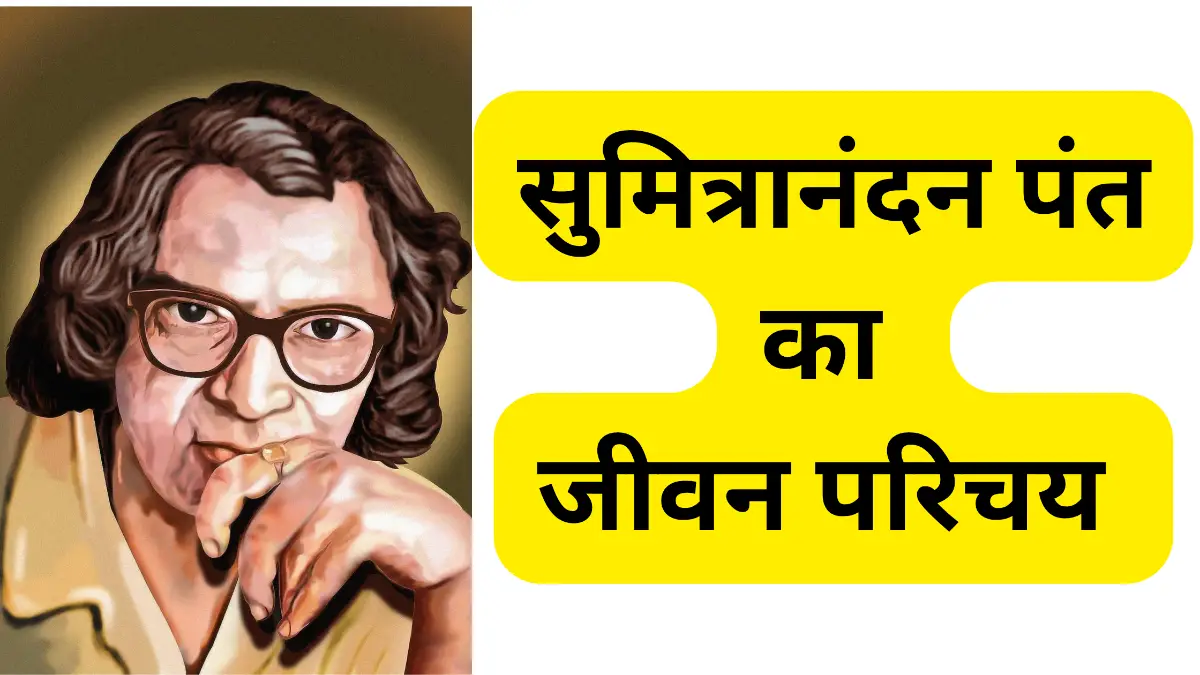सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय : जीवन और साहित्यिक योगदान ॥ Sumitranandan Pant Ka Jivan Parichay
जन्म और प्रारंभिक जीवन
हिन्दी साहित्य के छायावाद युग के महत्त्वपूर्ण स्तंभों में से एक सुमित्रानन्दन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी (संवत् 1957 वि०) को उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक सुरम्य ग्राम में हुआ। कौसानी की प्राकृतिक छटा ने उनके जीवन और काव्य पर गहरा प्रभाव डाला। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। दुर्भाग्यवश, जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माँ का निधन हो गया। परिणामस्वरूप, उनका पालन-पोषण उनकी दादी ने किया।
सुमित्रानन्दन पंत का वास्तविक नाम गुसाई दत्त पंत था। किंतु उन्हें यह नाम अधिक प्रिय नहीं था, इसलिए बाद में उन्होंने स्वयं को नया नाम दिया — सुमित्रानन्दन पंत। यह नाम साहित्य-जगत में उनकी पहचान बन गया। वे चार भाइयों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही प्रकृति-प्रेमी तथा संवेदनशील प्रवृत्ति के धनी थे।
शिक्षा और अध्ययन
पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। इसके बाद वे काशी (वाराणसी) पहुँचे और वहाँ क्वींस कॉलेज तथा जयनारायण स्कूल में अध्ययन किया। बाद में वे प्रयाग (इलाहाबाद) चले गए और म्योर कॉलेज में एफ.ए. की पढ़ाई शुरू की। हालांकि प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी और स्वाध्याय को ही अपनी साधना बना लिया।
वे संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेज़ी और बंगला भाषा का अध्ययन करने लगे। विशेष रूप से रवीन्द्रनाथ ठाकुर (रविबाबू) से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके साथ ही वे पाश्चात्य साहित्यकारों — शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और टेनिसन — से भी गहराई से प्रभावित हुए। संस्कृत साहित्य में कालिदास उनके प्रिय कवि रहे। साथ ही स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, कार्ल मार्क्स और श्री अरविन्द के विचारों ने भी उनके जीवन और काव्य-दर्शन को प्रभावित किया।
व्यक्तित्व और रुचियाँ
सुमित्रानन्दन पंत अत्यंत सुसंस्कृत और आधुनिक विचारों वाले कवि थे। उन्हें कपड़ों और केश-सज्जा का विशेष शौक था। वे संगीत के भी प्रेमी थे और अनेक बार स्वयं गुनगुनाकर रचनाएँ रचा करते थे। प्रयाग रेडियो स्टेशन में उच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी साहित्यिक पहचान बनाए रखी। उनका व्यक्तित्व कोमल, संवेदनशील और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर था।
साहित्यिक योगदान
सुमित्रानन्दन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मात्र सात वर्ष की आयु से उन्होंने काव्य-रचना आरम्भ कर दी थी। उनकी प्रथम प्रकाशित रचना ‘गिरजे का घण्टा’ (1916) थी, जिसने उनके साहित्यिक जीवन की दिशा निर्धारित की। इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी साहित्यिक अभिरुचि और प्रखर हुई। सन् 1920 में उनकी प्रारम्भिक कृतियाँ ‘उच्छ्वास’ और ‘ग्रन्थि’ प्रकाशित हुईं, जबकि 1927 में उनके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह ‘वीणा’ और ‘पल्लव’ ने उन्हें छायावाद का सशक्त प्रतिनिधि सिद्ध किया।
काव्य-सृजन के साथ पंत जी ने ‘रूपाभ’ नामक पत्र का सम्पादन भी किया, जिसमें उनके प्रगतिशील विचार झलकते हैं। सन् 1942 में महर्षि अरविन्द के संपर्क में आने से उनकी काव्य-दृष्टि और अधिक दार्शनिक और गहन हो गई।
उनके साहित्यिक योगदान को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ‘कला और बूढ़ा चाँद’ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ‘लोकायतन’ पर सोवियत भूमि पुरस्कार तथा ‘चिदम्बरा’ पर भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से भी अलंकृत किया।
साहित्य, दर्शन और सौंदर्य-बोध का अद्भुत समन्वय पंत जी की काव्यधारा को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बनाता है। उन्होंने काव्य के साथ-साथ कहानी, निबन्ध और नाटक आदि विधाओं में भी रचनाएँ कीं।
उनकी काव्य-यात्रा को मोटे तौर पर चार चरणों में बाँटा जाता है—
- प्रकृति काव्य चरण – उनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति की छटा और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण मिलता है।
- मानवीय एवं सामाजिक चेतना का चरण – इसमें वे सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े।
- दर्शनपरक और विचारपरक चरण – विवेकानन्द, गाँधी, मार्क्स और श्री अरविन्द के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने दार्शनिक कविताएँ लिखीं।
- परिपक्व काव्य चरण – इसमें वे जीवन, समाज और ब्रह्मांडीय चेतना की ओर उन्मुख हुए।
प्रमुख काव्य-ग्रंथ
उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की सूची इस प्रकार है—
- वीणा
- गुंजन
- पल्लव
- उच्छ्वास
- ग्राम्या
- युगान्त
- युगवाणी
- उत्तरा
- स्वर्ण किरण
- स्वर्ण धूलि
- युगपथ
- अणिमा
- मानसी
- वाणी
- कला और बूढ़ा चाँद
- खादी के फूल
- लोकायतन
- चिदम्बरा
उनकी रचनाओं में जहाँ एक ओर प्रकृति का रमणीय चित्रण है, वहीं दूसरी ओर मानवीय संवेदना, दार्शनिक गहराई और राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत संगम मिलता है।
काव्य-विशेषताएँ
- प्रकृति-प्रेम – कौसानी की प्राकृतिक छटा ने पंत जी के हृदय को बचपन से ही आकर्षित किया। उनकी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता और कोमलता का जीवंत चित्रण है।
- छायावादी प्रवृत्ति – वे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के साथ हिन्दी के छायावाद के चार स्तंभों में गिने जाते हैं।
- मानवीय चेतना – उनकी कविताओं में स्त्री-पुरुष समानता, समाज में न्याय और शांति की आकांक्षा बार-बार प्रकट होती है।
- दार्शनिक दृष्टि – विवेकानन्द और अरविन्द के प्रभाव से उनके काव्य में आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण विकसित हुआ।
- भाषा और शैली – उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, कोमल और मधुर है। वे छायावादी अलंकार, प्रतीक और कल्पना के लिए प्रसिद्ध हैं।
पुरस्कार और सम्मान
सुमित्रानन्दन पंत को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए—
- साहित्य अकादमी पुरस्कार – कला और बूढ़ा चाँद के लिए
- सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार – लोकायतन के लिए
- भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार – चिदम्बरा के लिए
- पद्मभूषण अलंकरण – हिन्दी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए
ये सम्मान उनके साहित्यिक कद और हिन्दी जगत में उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं।
भाषा-शैली
सुमित्रानन्दन पंत की भाषा-शैली अत्यन्त सरस, मधुर और काव्यात्मक है। उनकी कृतियों में कोमल भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिलती है। बांग्ला और अंग्रेज़ी साहित्य से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी काव्य में एक विशिष्ट गीतात्मक शैली का विकास किया। पंत जी का विशेष योगदान यह रहा कि उन्होंने खड़ी बोली को ब्रजभाषा जैसा माधुर्य, लय और कोमलता प्रदान की। उनके काव्य में ध्वनियों की संगीतात्मकता, शब्दों की मधुरता और भावनाओं की सजीवता पाठक को सहज ही आकृष्ट कर लेती है।
पंत जी केवल प्रकृति-चित्रण के कवि ही नहीं, बल्कि गहन विचारक और मानवता के सहज आस्थावान शिल्पी भी थे। उन्होंने काव्य के माध्यम से नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की और आदर्श मानव जीवन की ओर संकेत किया। उनकी भाषा में जहाँ एक ओर भावुकता और कोमलता है, वहीं दूसरी ओर गहन दार्शनिकता और जीवन-मूल्यों की गहरी छाप भी दिखाई देती है।
इस प्रकार पंत जी की भाषा-शैली में छायावादी सौंदर्य, संगीतात्मक माधुर्य और दार्शनिक गाम्भीर्य का अद्भुत संगम मिलता है, जो उन्हें हिंदी साहित्य का अप्रतिम कवि सिद्ध करता है।
स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध
1919 में महात्मा गाँधी के असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह से प्रभावित होकर सुमित्रानन्दन पंत ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। वे स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े और राष्ट्र की सेवा को सर्वोपरि माना। यही कारण है कि उनकी कई रचनाओं में स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की गूंज सुनाई देती है।
हिंदी साहित्य में स्थान
सुमित्रानन्दन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि होने के साथ-साथ सौन्दर्य के अद्वितीय उपासक माने जाते हैं। उनकी सौन्दर्यानुभूति के तीन प्रमुख केन्द्र रहे—प्रकृति, नारी और कला। उनके काव्य-जीवन का आरम्भ प्रकृति-चित्रण से हुआ, जिसमें वे प्रकृति के विविध रूपों, रंगों और लयों को सजीव कर देते हैं। उनकी काव्य-दृष्टि में न केवल प्रकृति की छटा का मोहक वर्णन है, बल्कि मानवीय भावनाओं और कल्पना की कोमलता का अनूठा संगम भी है।
पंत जी के काव्य में प्रकृति की सुकुमारता और मानवीय संवेदनाओं की कोमलता इस प्रकार घुल-मिल जाती है कि उन्हें ‘प्रकृति का सुकुमार कवि’ कहा जाता है। उनकी कविताएँ केवल सौन्दर्य-चित्रण तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनमें जीवन के गहरे सत्य, मानवीय करुणा और आध्यात्मिक चेतना की झलक भी दिखाई देती है।
उनका सम्पूर्ण काव्य आधुनिक साहित्यिक चेतना का सशक्त प्रतीक है। इसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता और आध्यात्मिकता—सभी का अद्भुत समन्वय मिलता है। इसी बहुआयामी स्वरूप ने पंत जी को हिंदी साहित्य के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया और उन्हें आधुनिक हिंदी काव्य का अमर कवि बना दिया।
अंतिम जीवन और निधन
सुमित्रानन्दन पंत का संपूर्ण जीवन साहित्य और समाज सेवा को समर्पित रहा। वे निरंतर लिखते रहे और हिन्दी साहित्य को नई दिशा देते रहे। 28 दिसम्बर 1977 ईस्वी (संवत् 2034 वि०) को उनका निधन हो गया।
उनका जीवन और साहित्य हिन्दी काव्य परम्परा में अमर है। वे न केवल छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, बल्कि उन्होंने आधुनिक हिन्दी कविता को एक नई दिशा दी।
निष्कर्ष
सुमित्रानन्दन पंत हिन्दी साहित्य के उन महान कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने प्रकृति की सुंदरता, मानवीय संवेदनाओं और दार्शनिक गहराई को अपनी कविताओं के माध्यम से अमर कर दिया। उनका जीवन अनेक संघर्षों, अनुभवों और साधनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई।
आज भी उनकी कविताएँ हिन्दी साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।
इसे भी पढ़िए:
- कबीरदास का जीवन परिचय ॥ Kabir Das Ka Jivan Parichay
- फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय ॥ Phanishwar Nath Renu Ka Jivan Parichay
- डॉ. रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय ॥ Dr Ramkumar Verma Ka Jivan Parichay
- चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय ॥ Chandradhar Sharma Guleri Jivan Parichay
- गुणाकर मुले का जीवन परिचय ॥ Gunakar Muley Ka Jeevan Parichay
- यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय ॥ Yatindra Mishra Jeevan Parichay
- बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय (Balkrishna Bhatt ka jeevan parichay)
- राजा लक्ष्मण सिंह का जीवन परिचय (Raja lakshman singh ka jeevan parichay)
- राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद; का जीवन परिचय (Raja shivprasad sitarehind ka jeevan parichay)
- तुलसीदास का जीवन परिचय tulsidas ka jivan parichay
- हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय harishankar parsai ka jivan parichay